 आज जिन जातियों को जो नाम हैं, क्या वह वह नाम उन्हें जाति व्यवस्था के जन्म के बाद ही मिला है, ऐसा नहीं है, इस बारे में एक जरूरी भ्रम जरूर दूर कर लेना चाहिए-संदर्भ बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता की जाति क्या थी?
आज जिन जातियों को जो नाम हैं, क्या वह वह नाम उन्हें जाति व्यवस्था के जन्म के बाद ही मिला है, ऐसा नहीं है, इस बारे में एक जरूरी भ्रम जरूर दूर कर लेना चाहिए-संदर्भ बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता की जाति क्या थी?कुछ एक दिनों पहले मैं बोध गया महाबोधि बिहार और बुद्ध को खीर खिलाने वाली सुजाता के गांव गया था। मैंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सुजाता ग्वालन थीं। इसके बाद तो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। एक तो यह की जब बुद्ध के समय में जाति व्यवस्था पैदा ही नहीं हुई थी, तो वह कहां से यादव हो गईं। दूसरा यह कि वह यादव ही थीं, आज के यादव लोग उन्हें अपनी जाति की नहीं मानते हैं। मैं सुजाता को यादव नहीं कहा था, ग्वालन कहा था।
यह सही है कि बुद्ध के समय में जाति व्यवस्था पैदा नहीं हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अलग-अलग पेशे करने वाले समूह नहीं पैदा हुए और उनका कोई नाम नहीं था। बुद्ध के समय में (करीब आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व) समय श्रम विभाजन एक हद तक उच्चत्तर अवस्था में था। एक काम करने वाले समूहों सामने आ गए थे, कुछ आ रहे थे। दस्तकारों, कारीगरों और अन्य कौशल विशेष से संपन्न समूह पैदा हो चुके थे या हो रहे थे। जैसे मिट्टी के बर्तना बनाने वाले, लोहे की चीजें बनाने वाले, धातुओं से आभूषण बनाने वाले, पशु-पालन और दूध-दही का कारोबार करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, कपड़ा बनाने, सिलने वाले, लकड़ी की चीजें बनाने वाले, व्यापार-कारोबार करने वाले, ज्ञान-विज्ञान और दर्शन की दुनिया में काम करने वाले, गीत-संगीत और संस्कृति के अन्य विधाओं का पेशा करने वाले और यौद्धाओं आदि समूह पैदा हो गए थे। इसके अलावा श्रमिकों के समूह भी अस्तित्व में आ गए थे।

अलग-अलग काम करने वाले समूहों के नाम भी थे। चूंकि ज्ञान-विज्ञान और कौशल, दस्ताकारी और कारीगरी आदि दूसरी पीढ़ी को स्थानंतारण अनुभव संगत ज्ञान के आधार पर ही हो रहा था, इसलिए एक समूह को अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी को सौंपना सहज था। मतलब माता-पिता अपने बेटे-बेटियों को आसानी से सौंप सकते थे। सारी बातों का लब्बोलुआब यह है कि जाति व्यवस्था के पैदा होने और उसे लौह सांचे में ढाल देने से पहले भी अलग-अलग पेशा करने वालों समूहों का अलग-अलग नाम था। जैसे लोहार तब भी था, बढ़ई तब भी था,मछुवारा (मल्लाह) तब भी थे, कुम्हार तब भी थे, सोनार तब भी थे, ग्वाला तब भी थे, कसाई तब भी थे यहां तक ब्राह्मण संज्ञा भी बुद्ध के काल में मिलती है। बहुत सारे पेशे और उनसे जुड़े बहुत सारे नाम।
उनमें से बहुत सारे नाम वैसे के वैसे, या कुछ बदले हुए रूप में या पूरी तरह बदले हुए रूप में आज भी मौजूद हैं। पेशेगत समूहों के नामों में दो तरह से परिवर्तन आया पहला भाषा के बदलने से परिवर्तन। जैसे पालि में वह नाम कुछ अलग तरह से उच्चारित होता है, तो प्राकृत में थोड़ा अलग, अपभ्रंश में अलग और संस्कृत के जन्म के बाद भी कुछ बदलाव। तमिल में कुछ अलग, इसके साथ हिंदी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तेलगू, कन्नड़, संथाल, गोंंडी आदि में अलग। लेकिन सबका संबंध पेशे से जुड़ा हुआ था। अभी हाल तक जातियों के नामों में परिवर्तन होता रहा है, अभी भी हो रहा है,जबकि मूल चीज वैसे-की-वैसे है। जैसे ग्वाला,अहीर,यादव, सिंह यादव की एक यात्रा है। धोबी-कन्नौजिया, अनेकों अनेक।
जाति व्यवस्था के जन्म और उसके लौह सांचे में ढल जाने के बाद निम्न तरह के बुनियादी परिवर्तन आए-
1- जाति व्यवस्था के जन्म और लौह सांचे में ढलने से पहले एक पेशे के लोग दूसरा पेशा अपना सकते थे, दूसरे पेश में जाने के बाद उनकी पहचान उस पेशे से जुड़ जाती। जैसे कुम्हार, लोहार का पेशा अपना सकता था, फिर उसे कुम्हार नहीं लोहार कहा जाता। इसी तरह धोबी, लोहार का पेशा अपना सकता था, उसे उसकी पहचान धोबी की नहीं,लोहार की होती। यहां तक कि ज्ञान-विज्ञान की दुनिया में काम करने वालों में लोहार, धोबी और बढ़ई का पेशा करने वाला शामिल हो सकता था। तब उसकी पहचान वही हो जाती। लेकिन वर्ण-जाति व्यवस्था के लौह सांचे में ढाल देने के बाद एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे में जाना नामुमकिन बन गया या बना दिया गया। ऐसा करना दंड का भागी होना था। मतलब जन्म आधारित बना दिया।
2- बुद्ध के काल में किसी पेशे को हेय समझना, नीचा काम समझना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन उसका मुख्य आधार किसी पेशे से होने वाली आय और उससे वाला मान-सम्मान ही था। जैसे बुद्ध काल में भी ज्ञान-विज्ञान के पेशे में, धर्म-दर्शन के पेशे में या योद्धा के पेशे में लगे हुए लोगों का ज्यादा सम्मान था और चूंकि एक पेशे से दूसरे में जाने की संभावना थी, इस वजह से किसी समूह के व्यक्ति को हमेशा-हमेशा के लिए नीच और ऊंच नहीं ठहराया जा सकता था।
जाति व्यवस्था के लौह सांचे ने जातियों के ऊंच-नीच का श्रेणीक्रम पूरी तरह पक्का कर दिया। हालांकि उसका आधार पेशे से जुड़ा रहा। बुद्ध काल में दास प्रथा किसी न किसी रूप में थी, दासों को हेय और नीचा समझा जाता था।
3- जाति व्यवस्था के जन्म और उसके लौह सांचे ने एक जाति की लड़की-लड़के के दूसरी जाति के लड़के-लड़की से शादी को प्रतिबंधित कर दिया, उसे भी जातियों के लोह साचें में कस दिया।
निष्कर्ष रूप में यह कहना है कि यदि बुद्ध काल में किसी किसी समूह को मल्लाह-केवट कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उस समय जाति व्यवस्था पैदा हो गई थी। इसी तरह यदि किसी समूह को ग्वाला कहा जा रहा है, तो भी उसका मतलब जाति व्यवस्था उस समय थी, यह नहीं कहा जा रहा है। आज की तारीख में भी जो कुछ ऐसी जातियां हैं,उनके जो पेशे हैं, वे पेशे बुद्ध काल में पैदा हो चुके थे, उस पेशे को करने वाले समूह की पहचान उसके पेशे से होती थी। हां यहां यह भी स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि अलग-अलग पेशा करने वाले समूह ही थी, उन्नत पूंजीवादी समाज की तरह अलग-अलग व्यक्ति नहीं। पेशे समूहगत ही थे।
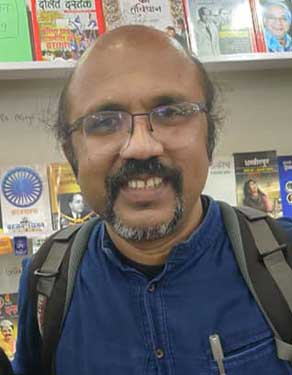
लेखक स्वतंत्र पत्रकार और बहुजन विचारक हैं। हिन्दी साहित्य में पीएचडी हैं। तात्कालिक मुद्दों पर धारदार और तथ्यपरक लेखनी करते हैं। दास पब्लिकेशन से प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक सामाजिक क्रांति की योद्धाः सावित्री बाई फुले के लेखक हैं।

