 दशकों से आरक्षण भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर समय-समय पर देश का माहौल उतप्त हो जाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ यह कुछ दशकों से हो रहा है: आधुनिक भारत में ऐसे हालात की सृष्टि भारत के स्वाधीनता संग्राम से ही शुरू होती है. स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भावुक होने वाले अधिकांश लोगों को शायद पता नहीं कि भारत में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत आरक्षण को लेकर होती है. 1885 में अंग्रेज अक्टोवियन ह्युम के नेतृत्व में जिस कांग्रेस की शुरुआत होती है, दरअसल वह भारतीय एलिट वर्ग के लिए छोटी-छोटी सुविधाओं की मांग के लिए थी,जो धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग में बदल गयी. भारतीय एलिट क्लास की मांग पर अंग्रेजों ने 1892 में पब्लिक सर्विस कमीशन की द्वितीय श्रेणी के 941 पदों में 158 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किये. एक बार आरक्षण का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस ने भारतीयों के लिए पीडब्ल्यूडी,रेलवे, चुंगी आदि विभागों के उच्च पदों पर आरक्षण की मांग उठाना शुरू किया. अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों में आरक्षण की मांग ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस ने 1900 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कड़ी निंदा प्रस्ताव लाया. बहुतों को लग सकता है कि दलितों द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए उठाई जा रही मांग, नई परिघटना है. नहीं! तब भारतीयों के लिए रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी आरक्षण की मांग उठाया था. हिंदुस्तान मिलों के घोषणा पत्रक में उल्लेख किया गया था कि ऑडिटर , वकील, खरीदने-बेचने वाले दलाल आदि भारतीय ही रखे जांय . तब योग्यता का आधार केवल हिन्दुस्तानी होना था, परीक्षा में कम ज्यादा नंबर लाना नहीं . कहा जा सकता कि शासन-प्रशासन , उद्योग-व्यापार में संभ्रांत भारतीयों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस का ‘आरक्षण बढाओ आन्दोलन’ परवर्तीकाल में स्वाधीनता आन्दोलन का रूप ले लिया .
दशकों से आरक्षण भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसे लेकर समय-समय पर देश का माहौल उतप्त हो जाता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ यह कुछ दशकों से हो रहा है: आधुनिक भारत में ऐसे हालात की सृष्टि भारत के स्वाधीनता संग्राम से ही शुरू होती है. स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भावुक होने वाले अधिकांश लोगों को शायद पता नहीं कि भारत में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत आरक्षण को लेकर होती है. 1885 में अंग्रेज अक्टोवियन ह्युम के नेतृत्व में जिस कांग्रेस की शुरुआत होती है, दरअसल वह भारतीय एलिट वर्ग के लिए छोटी-छोटी सुविधाओं की मांग के लिए थी,जो धीरे-धीरे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग में बदल गयी. भारतीय एलिट क्लास की मांग पर अंग्रेजों ने 1892 में पब्लिक सर्विस कमीशन की द्वितीय श्रेणी के 941 पदों में 158 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किये. एक बार आरक्षण का स्वाद चखने के बाद कांग्रेस ने भारतीयों के लिए पीडब्ल्यूडी,रेलवे, चुंगी आदि विभागों के उच्च पदों पर आरक्षण की मांग उठाना शुरू किया. अंग्रेजों द्वारा इन क्षेत्रों में आरक्षण की मांग ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस ने 1900 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कड़ी निंदा प्रस्ताव लाया. बहुतों को लग सकता है कि दलितों द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए उठाई जा रही मांग, नई परिघटना है. नहीं! तब भारतीयों के लिए रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी आरक्षण की मांग उठाया था. हिंदुस्तान मिलों के घोषणा पत्रक में उल्लेख किया गया था कि ऑडिटर , वकील, खरीदने-बेचने वाले दलाल आदि भारतीय ही रखे जांय . तब योग्यता का आधार केवल हिन्दुस्तानी होना था, परीक्षा में कम ज्यादा नंबर लाना नहीं . कहा जा सकता कि शासन-प्रशासन , उद्योग-व्यापार में संभ्रांत भारतीयों को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर शुरू हुआ कांग्रेस का ‘आरक्षण बढाओ आन्दोलन’ परवर्तीकाल में स्वाधीनता आन्दोलन का रूप ले लिया .
बहरहाल उच्च वर्ण हिन्दुओं के लिए आरक्षण की शुरुआत अगर 1892 में हुई तो हिन्दुओं की दबी-कुचली जाति शुद्रातिशुद्रों के आरक्षण की शुरुआत 26जुलाई,1902 से कोल्हापुर रियासत से होती है , जिसे देने का श्रेय कुर्मी जाति में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशधर छत्रपति शाहूजी महाराज को जाता है. लेकिन दस्तावेजों में 1892 को भारत में आरक्षण की शुरुआत का वर्ष भले ही चिन्हित किया गया है, वास्तव में इसकी शुरुआत हिंदुत्व के दर्शन के विकास के साथ-साथ वैदिक भारत अर्थात आज से साढ़े तीन हजार पूर्व तब होती है, जब वर्ण-व्यवस्था ने आकार लेना शुरू किया .
यह सच्चाई है कि ईश्वर विश्वासी तमाम संगठित धर्मों का चरम लक्ष्य ,अपने-अपने धर्म के अनुसरणकारियों को मरणोपरांत सुख सुलभ कराना रहा है. सभी धर्मों के प्रवर्तकों ने यह बताने में एक दूसरे से होड़ लगाया है कि परलोक सुख में ही मानव जीवन कि सार्थकता है. मरणोपरांत यह सुख सुलभ हो ,इसके लिए मार्ग सुझाने के लिए ही तमाम धर्म-ग्रंथों की सृष्टि हुई है. इन धर्म ग्रंथों में उन कायदे-कानूनों का ही उल्लेख है, जिनका अनुसरण कर लोग पैराडाइज ,जन्नत ,स्वर्ग का सुख एन्जॉय कर सकते थे . इसके लिए सभी धर्मों ने स्वधर्म पालन का कठोर निर्देश अपने धर्मशास्त्रों में दिया है. जहां तक भारत का सवाल है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य का उच्च उद्घोष करने वाले हिन्दू धर्म में स्व-धर्म पालन को दृष्टिगत रखते हुए हुए भूरि –भूरि धर्म शास्त्रों का सृजन एवं ‘राज्य’ की उत्पत्ति का सिद्धांत विकसित किया गया . इस विषय में धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता मनु का मानना रहा है कि ‘प्राणीमात्र का कल्याण ही स्व-धर्म पालन में है, पर मनुष्य समाज ऐसे प्राणियों से बना है , जिसमें स्वधर्म परायणता दुर्लभ है. इसलिए इन अशुचि, अधर्मपरायण प्राणियों को स्वधर्म-पालन निमित्त बाध्य करने के लिए उन्हें दण्डित करना परमाआवश्यक है.’ इसी उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु उन्होंने दंडविधान की व्यवस्था की. मनु के अनुसार दण्ड का सर्जन ईश्वर ने स्वयं किया. इस प्रकार मनु के मतानुसार धर्म और दण्ड दोनों की उत्पत्ति साथ-साथ हुई है और दण्ड का उद्देश्य धर्म संस्थान एवं धर्मरक्षा है. मनु ने धर्म रक्षा हेतु जो दण्डनीति बनाई,वही राजशास्त्र अर्थात राजधर्म के रूप में मान्य हुई.
प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र उद्देश्य धर्म-संस्थापन बतलाया गया है. इस धरा पर प्रत्येक प्राणी स्वधर्म पालन सम्यक प्रकार करता रहे, जगत में धर्म-संकरता उत्पन्न न होने पाए : बस यही राज्य का एकमात्र कर्तव्य बतलाया गया है. बहरहाल जिसे हिन्दू धर्म शास्त्रों द्वारा स्वधर्म पालन कहा गया है, वह सम्पूर्ण मानव जाति का धर्म न होकर सिर्फ हिन्दू ईश्वर(विराट-पुरुष) के विभिन्न अंगों से जन्मे चार वर्ण के लोगों का धर्म है. स्वधर्म पालन के नाम पर चार वर्णों (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य और शुद्रतिशूद्र) में बंटे सामाजिक समूहों के लिए भिन्न-भिन्न कर्म/पेशे (वृत्तियां) धर्म शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट किये गए. इन पेशे/ कार्यों से विचलन पूरी तरह निषिद्ध रहा. पेशों के विचलन से धर्म-संकरता की सृष्टि होती है इसलिए जिस वर्ण के लिए जो कार्य निर्दिष्ट किये गए , उसे छोड़कर दूसरे वर्णों का पेशा/कर्म अपनाना दंडनीय अपराध रहा. इनमें ब्राह्मण वर्ण के मानव समूहों का धर्म अध्ययन-अध्यापन, पौरोहित्य, राज्य सञ्चालन में मंत्रणादान;क्षत्रियों का धर्म भूस्वामित्व,शासन-प्रशासन और सैन्य संचालन तो वैश्यों का धर्म पशुपालन,व्यवसाय-वाणिज्य का कार्य सम्पादित करना तय किया गया. स्वधर्म पालन में हिन्दू ईश्वर के जघन्य अंग (पैर) से जन्मे लोगों का धर्म रहा ऊपर के तीन वर्णों की सेवा, वह भी नि:शुल्क!
बहरहाल स्वधर्म पालन के लिए वर्ण-व्यवस्थाधारित राजधर्म लागू होने के फलस्वरूप जिस वर्ण के लिए धर्म-पालन के नाम पर जो कार्य निदिष्ट किये गए , वे पेशे/कर्म उस वर्ण के लिए चिरकाल के लिए आरक्षित होकर रह गए . ऐसे में स्वधर्म पालन करवाने के उद्देश्य से प्रवर्तित वर्ण व्यवस्था मूलतः एक आरक्षण व्यवस्था, जिसे हिन्दू आरक्षण-व्यवस्था कहा जा सकता है, के रूप में क्रियाशील रहने के लिए अभिशप्त हुई. इस हिन्दू आरक्षण में स्वधर्म पालन के नाम पर चौथे वर्ण के अंतर्गत आने वाले शुद्रातिशूद्रों के लिए ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्यों के लिए आरक्षित पेशे अपनाने का कोई अवसर नहीं रहा. इसलिए साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व शुरू हुई आरक्षणवादी वर्ण-व्यवस्था के चलते दलित , आदिवासी और पिछड़े शक्ति के समस्त स्रोतों (आर्थिक-राजनीति-शैक्षिक- धार्मिक इत्यादि) से हमेशा-हमेशा के लिए बहिष्कृत होने के लिए अभिशप्त हुए. अवश्य ही 6 अक्तूबर,1860 को लागू लार्ड मैकाले की आईपीसी के वजूद में आने से हिन्दू आरक्षण की बंदिशें टूटीं .किन्तु हिन्दू आरक्षण के चलते वे शिक्षा और धन-बल से इतना कमजोर बना दिए गए थे कि आईपीसी द्वारा सुलभ कराये गए अवसरों का सद्व्यहार न कर सके. अवसरों के सद्व्यवहार का अवसर उन्हें डॉ. आंबेडकर के प्रयत्नों से मिला.
बहरहाल वर्ण-व्यवस्था का एक आरक्षण-व्यवस्था में तब्दील होना महज संयोग नहीं रहा. इसे बहुत ही सुपरिकल्पित रूप से आरक्षण व्यवस्था का रूप दिया गया, जिसका सुराग आर्य-पुत्र पंडित नेहरु द्वारा वर्ण व्यवस्था के निर्माण के पीछे चिन्हित कारणों से मिलता है. पंडित नेहरु ने भारत की खोज में निकलते हुए बताया है-‘वर्ण-भेद, जिसका मकसद आर्यों को अनार्यों से जुदा करना था , अब खुद आर्यों पर अपना यह असर लाया कि ज्यों-ज्यों धंधे बढे और इनका आपस में बंटवारा हुआ, त्यों-त्यों नए वर्गों ने वर्ण या जाति की शक्ल अख्तियार कर ली. इस तरह , एक ऐसे जमाने में , जब फतह करने वालों का यह कायदा रहा कि हारे हुए लोगों को या तो गुलाम बना लेते या बिलकुल मिटा देते थे, वर्ण-व्यवस्था ने एक शान्ति वाला हल पेश किया. और धंधों के बंटवारे की जरुरत से इसमें वैश्य बनें , जिनमें किसान ,कारीगर और व्यापारी लोग थे; क्षत्रिय हुए जो हुकूमत करते या युद्ध करते थे; ब्राह्मण बनें जो पुरोहिती करते करते थे, विचारक थे, जिनके हाथ में नीति की बागडोर थी और जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वे जाति के आदर्शों की रक्षा करेंगे. इन तीनों वर्णों से नीचे शूद्र थे , जो मजदूरी करते और ऐसे धंधे करते , जिनमें खास जानकारी की जरुरत नहीं होती और जो किसानों से अलग थे. कदीम वाशिंदों से भी बहुत से इन समाजों में मिला लिए गए और उन्हें शूद्रों के साथ इस समाज में सबसे नीचे का दर्जा दिया गया. ‘
वास्तव में आर्यों ने वर्ण-व्यवस्था को जो आरक्षण का रूप दिया, उसे विजेता का धर्म भी कहा जा सकता है. इतिहास के हर काल में साम्राज्यवादी विदेशागतों ने पराधीन बनाये गए मूलनिवासियों के देश की संपदा – संसाधनों को अपने कब्जे में करने और उनको दास/सेवक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तरह-तरह के नियम कानून बनाये. भारत से बाहर के साम्राज्यवादियों ने मुख्यतः शस्त्र आधारित नियम-कायदे बनाकर मूलनिवासियों का शोषण किया. मसलन जिस भारत से दक्षिण अफ्रीका की सर्वाधिक साम्यता है, वहां के विदेशागत गोरों ने बन्दूक की नाल पर पुष्ट कानून के जरिये वहां के मूलनिवासियों को शक्ति के समस्त स्रोतों से बहिष्कृत कर उन्हें शक्तिशून्य दास के रूप में परिणत किया. किन्तु पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश रहा, जहाँ हजारों वर्ष भारत आये विदेशागातों ने धर्म-शास्त्रों के जरिये दलित, आदिवासी,पिछड़ों और आधी आबादी को दैविक-गुलाम बनाकर शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार स्थापित किया.
बहरहाल अगर महानतम समाज विज्ञानी कार्ल मार्क्स ने दुनिया के इतिहास को परिभाषित करते हुए यह कहा कि दुनिया का इतिहास संपदा और संसाधनों के बटवारे पर केन्द्रित वर्ग संघर्ष का इतिहास है तो भारत के सम्बन्ध में फुले, कांशीराम इत्यादि ने जातीय संघर्ष का इतिहास बताया. फुले-कांशीराम को भारत का इतिहास जातीय संघर्ष का इतिहास इसलिए बताना पड़ा क्योंकि जिस संपदा-संसाधनों के बंटवारे के कारण मानव सभ्यता के विकास के साथ वर्ग-संघर्ष संगठित होता रहा , सपदा-संसाधनों के बंटवारे का वह सिद्धांत वर्ण-व्यवस्था में निहित रहा. इस वर्ण-व्यवस्था ने दो वर्गों- शक्ति संपन्न विशेषाधिकारयुक्त सुविधाभोगी वर्ग और बंचित बहुजन समाज – का निर्माण किया. ये दोनों वर्ग देवासुर -संग्राम काल से ही संपदा-संसाधनों पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए संघर्षरत रहे. अवश्य ही इसमें विशेषाधिकारयुक्त वर्ग हमेशा से विजयी रहा और आज तो वे 90 प्रतिशत से ज्यादा संपदा-संसाधनों पर कब्ज़ा जमाकर वंचित मूल निवासी वर्ग के समक्ष और कड़ी चुनौती पेश कर दिया है. ऐसे में सवाल पैदा होता कि क्या कभी भारत के बहुजन दक्षिण अफ्रीका के मूलनिवासियों की भांति संपदा-संसाधनों पर अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो पाएंगे ?
(लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.)
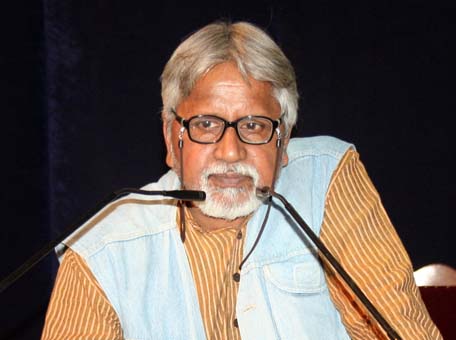
डायवर्सिटी मैन के नाम से विख्यात एच.एल. दुसाध जाने माने स्तंभकार और लेखक हैं। हर विषय पर देश के विभिन्न अखबारों में नियमित लेखन करते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और दुसाध प्रकाशन के नाम से इनका अपना प्रकाशन भी है।

