 जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.
मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.
लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी.
जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.
मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.
लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी. जब लड़ने को खड़े हुए, तब ही पीएम मोदी का बयान क्यों आया?
 जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.
मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.
लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी.
जब तक दलित पिट रहे थे तब तक मोदी का बयान नही आया. जब वो लड़ने उठ खड़े हुये तब मोदी क्यो बोले? क्यों? लड़ने वालो को इस बयान की क्या जरूरत है? अपने बयान से वो दलितो की मदद कर रहे हैं या उन्हे भ्रमित कर भाजपा की मदद कर रहे हैं? मोदी का बयान लड़ने उठ खड़े दलितों को भ्रमित करने का मनिवैज्ञानिक हमला मात्र है. गौरक्षको के हमले का प्लान भी.
मुस्लिम तो मारे तक गये, उनके लिये तो अब भी नही बोले. गौर से देखिये मुसलमान लड़ने को नही खड़े हुये तो उनके लिये मोदी ने कुछ नहीं बोला. क्या मोदी जी अपने गौरक्षको को ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिमो पर हमला करो? जाहिर है वो एक रणनीति के तहत फिर से बेईमानी कर रहे हैं जिसकी उनके चरित्र को देखते हुये उनसे उम्मीद की जाती है. लड़ते दलितों को आपके बयान की जरूरत नहीं है मोदी जी. बतौर प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करिए और कोई एक्शन लेना हो तो लीजिये, उसके लिये एहसान मत दिखाइये. पिटने वाला दलित अब लड़ेगा और बहुजन बनेगा.
लड़ाई लड़ने के लिये उठे बहुजनों अपना सशक्तीकरण और देश के दुश्मनो की अपनी समझ को बनाये रखो, आपके शोषण करने वाले इन नफरत से भरे अमानुष देशद्रोही संघियो को आपका अपना बताने कि कोशिश कर भ्रमित करने वाले मक्कारो के बयान आयेंगे. मोदी सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बहुजनो को खुद लड़ने की जरूरत नही हैं मैं हूँ. ये झूठ है आपकी लड़ाई की प्रेरणा को तोडने के लिये. अपनी समझ बनाये रखो, और उद्देश्य भी. गुजरात दलित मार्च को मिला विदेशों से समर्थन, अमेरिका और कनाडा में भी होगा विरोध प्रदर्शन
 कैलिफोर्निया। बाबासाहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे अमेरिका और कनाडा में “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करेंगें और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगें, 12 अगस्त से इसकी शुरूआत कोपले स्क्वेयर और हारवर्ड स्क्वेयर सहित पूरे विश्व में होगी. सभी अम्बेडकराइट लोग 12 अगस्त से 15 अगस्त तक विश्व की अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगें और इसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से पब्लिश करेंगें. मुख्यधारा की मीडिया गटर बन गई जो कि सिर्फ ज्योतिष, बॉलीवुड, क्रिकेट, फर्जी बाबाओं के प्रचार और हिंदूत्वादी सीरियल को प्रोमोट करती है.
भारत में दलितों पर अत्याचार और मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ रही हैं. ये लोग जानवरों की सुरक्षा के नाम पर स्वयं जानवर बन रहें हैं. इन्होंने देश को हिंदू तालिबान बना दिया है. अम्बेडकरवादी विचारों को मानने वाले लोग “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे संगठनों से सहमत है. अम्बेडकरवादी भारत के सभी राज्यों और शहरों में 15 अगस्त तक एकजुट होकर दलित मार्च का समर्थन करेंगें. अम्बेडकरवादियों का कहना है कि यह समय करो या मरो का है, अपने बच्चों और पोतों के लिए, भविष्य में हमें बिना जाति के जीना है. अब बर्दाश्त नहीं होगा.
अम्बेडकर एशोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, बोस्टन स्टडी ग्रुप, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया और अन्य प्रगतिशील समूह “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करता है और 13 अगस्त को सेन फ्रांसिस्को के बाजार में भी प्रोटेस्ट करेंगे. ये संगठन विदेशों में रहने के बाद भी भारत से अधिक एक्टिव है और भारतीय प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखता है.
कैलिफोर्निया। बाबासाहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग पूरे अमेरिका और कनाडा में “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करेंगें और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगें, 12 अगस्त से इसकी शुरूआत कोपले स्क्वेयर और हारवर्ड स्क्वेयर सहित पूरे विश्व में होगी. सभी अम्बेडकराइट लोग 12 अगस्त से 15 अगस्त तक विश्व की अलग-अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगें और इसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों से पब्लिश करेंगें. मुख्यधारा की मीडिया गटर बन गई जो कि सिर्फ ज्योतिष, बॉलीवुड, क्रिकेट, फर्जी बाबाओं के प्रचार और हिंदूत्वादी सीरियल को प्रोमोट करती है.
भारत में दलितों पर अत्याचार और मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ रही हैं. ये लोग जानवरों की सुरक्षा के नाम पर स्वयं जानवर बन रहें हैं. इन्होंने देश को हिंदू तालिबान बना दिया है. अम्बेडकरवादी विचारों को मानने वाले लोग “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करने के लिए एक-दूसरे संगठनों से सहमत है. अम्बेडकरवादी भारत के सभी राज्यों और शहरों में 15 अगस्त तक एकजुट होकर दलित मार्च का समर्थन करेंगें. अम्बेडकरवादियों का कहना है कि यह समय करो या मरो का है, अपने बच्चों और पोतों के लिए, भविष्य में हमें बिना जाति के जीना है. अब बर्दाश्त नहीं होगा.
अम्बेडकर एशोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन, बोस्टन स्टडी ग्रुप, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ कैलिफोर्निया और अन्य प्रगतिशील समूह “आजादी के लिए गुजरात दलित मार्च” का समर्थन करता है और 13 अगस्त को सेन फ्रांसिस्को के बाजार में भी प्रोटेस्ट करेंगे. ये संगठन विदेशों में रहने के बाद भी भारत से अधिक एक्टिव है और भारतीय प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखता है. बिहारः 38 सीटों पर होगा सामान्य वर्ग का कब्जा
 पटना। जातिगत भेदभाव बिहार के शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले ही पटना में दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था. अब मामला शैक्षणिक संस्था में आरक्षण की नीति में परिवर्तन करने को लेकर उठा है. बिहार के शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी निर्देश कॉलेजों को दिया है. उन्होंने आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों के दाखिला करने के आदेश दे दिए है. इस चौधरी के इस आदेश की छात्रों ने निंदा की हैं.
राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में सभी खाली सीटें भरी जाएंगी. इसके लिए सरकार आरक्षण नियम में बदलाव करेगी. इन कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पांच टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रह गई हैं. इन सीटों को भरने के लिए सरकार ने आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए खाली रह गई सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का एडमिशन लेने पर सहमति दे दी है. सरकार की इस सहमति से दलित वर्ग के छात्र ने इस नीति का विरोध किया है. छात्रों ने मांग की है कि आरक्षित सीटों पर सिर्फ आरक्षण वाले विद्यार्थी ही दाखिला लेंगें.
पटना। जातिगत भेदभाव बिहार के शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ रहा है. कुछ दिन पहले ही पटना में दलित छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था. अब मामला शैक्षणिक संस्था में आरक्षण की नीति में परिवर्तन करने को लेकर उठा है. बिहार के शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी निर्देश कॉलेजों को दिया है. उन्होंने आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों के दाखिला करने के आदेश दे दिए है. इस चौधरी के इस आदेश की छात्रों ने निंदा की हैं.
राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में सभी खाली सीटें भरी जाएंगी. इसके लिए सरकार आरक्षण नियम में बदलाव करेगी. इन कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पांच टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में आरक्षित कोटे की कुछ सीटें खाली रह गई हैं. इन सीटों को भरने के लिए सरकार ने आरक्षण नियमों में संशोधन करते हुए खाली रह गई सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का एडमिशन लेने पर सहमति दे दी है. सरकार की इस सहमति से दलित वर्ग के छात्र ने इस नीति का विरोध किया है. छात्रों ने मांग की है कि आरक्षित सीटों पर सिर्फ आरक्षण वाले विद्यार्थी ही दाखिला लेंगें. कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले इस ओलंपियन से मिलिए
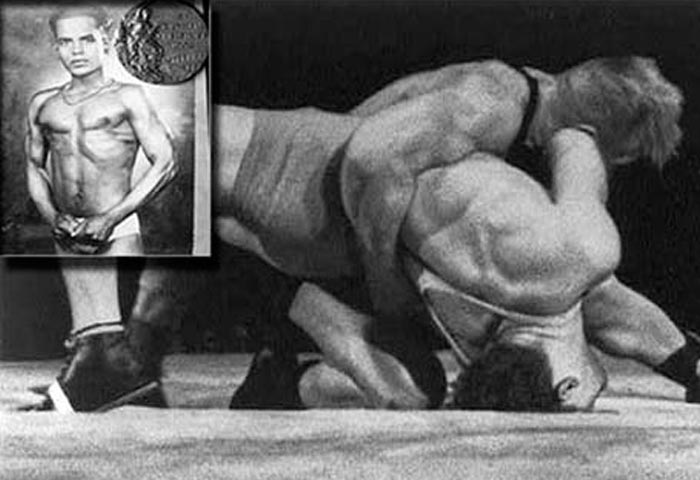 आज ओलंपिक में जब मूलनिवासी समाज की दीपा कर्माकर ने भारत के लिए एक उम्मीद जगा दी है, तो ऐसे में महान ओलंपिक खिलाड़ी ‘खाशाबा दादासाहेब जाधव उर्फ के.डी.जाधव’ का जिक्र करना भी जरूरी है. इस महान ओलंपिनय ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के बैंटमवेट वर्ग कुश्ती में कांस्य जीत कर विश्व फलक पर भारत को इज्जत दिलाई थी. भारत के लिये ओलंपिक की व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में यह पहला पदक था. लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि ओलंपिक जैसे मंच पर भारत की नाक ऊंची करने वाले इस खिलाड़ी को भारत का पद्म सम्मान भी नसीब नहीं हुआ.
महाराष्ट्र में जन्में के. डी. जाधव को हेलसिंकी ओलंपिक के लिए टीम चयन के दौरान साजिश का सामना करना पड़ा था. हालांकि तमाम मशक्कत के बाद आखिरकार अपनी प्रतिभा साबित कर उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह बना ली थी. तब जाधव के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे. उन्होंने सरकार से सहायता मांगी, लेकिन जाधव की आर्थिक मदद की मांग को तात्कालीन सरकारों ने अनसुना कर दिया था. तब उन्होंने गांव में चंदा मांगकर, अपनी सम्पति और घर गिरवी रखकर ओलंपिक जाने के लिये धन जुटाया था. वापस आने पर के. डी ने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीतकर लोगों का पैसा वापस कर एहसान चुकाया था. गरीबी एवं संघर्ष के बावजूद खुद्दारी में जीवन जीते हुये के. डी. जाधव की मौत 1984 में सड़क दुर्घटना में हो गई. महज आश्चर्य ही नहीं बल्कि शर्म की बात है कि ओलंपिक पदक के 50वें साल और उनकी मृत्यु के 15वें साल में 2001 में जाकर उन्हें अर्जुन सम्मान मिल सका. इस बीच एक तथ्य यह भी है कि जाधव अकेले ऐसे ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनको कोई पद्म सम्मान नहीं दिया गया.
एक गरीब परिवार औऱ तमाम संघर्ष से निकलकर दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाले एक गैरद्विज खिलाड़ी की उपेक्षा का यह मामला साधारण नहीं है, बल्कि गंभीर पक्षपात एवं सामाजिक पूर्वाग्रह का मामला भी दिखता है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ओलंपिक में ज्यादातर बार मूलनिवासी (दलित-आदिवासी-पिछड़े) समाज के प्रतिभाओं ने ही देश का मान रखा है. चाहे वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हों, मुक्केबाज मैरीकॉम हो, निशानेबाज दीपीका कुमारी हो या फिर अब दीपा कर्माकर. ‘ध्यानचंद’ के साथ ‘के.डी. जाधव’ को भारत रत्न से सम्मानित कर भारत के माथे पर लगे इस पक्षपात और पूर्वाग्रह के कलंक को धोने का काम वर्तमान या भविष्य की कोई भारत सरकार कब करती है इसका इंतजार रहेगा. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही 14 अगस्त को के.डी. जाधव की पुण्यतिथि होती है. इस महान ओलंपियन और देश का मान बढ़ाने वाले प्रेरणा पुरुष को नमन.
(जन्म: 15 जनवरी, 1926- मृत्यु: 14 अगस्त, 1984)
आज ओलंपिक में जब मूलनिवासी समाज की दीपा कर्माकर ने भारत के लिए एक उम्मीद जगा दी है, तो ऐसे में महान ओलंपिक खिलाड़ी ‘खाशाबा दादासाहेब जाधव उर्फ के.डी.जाधव’ का जिक्र करना भी जरूरी है. इस महान ओलंपिनय ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के बैंटमवेट वर्ग कुश्ती में कांस्य जीत कर विश्व फलक पर भारत को इज्जत दिलाई थी. भारत के लिये ओलंपिक की व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में यह पहला पदक था. लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि ओलंपिक जैसे मंच पर भारत की नाक ऊंची करने वाले इस खिलाड़ी को भारत का पद्म सम्मान भी नसीब नहीं हुआ.
महाराष्ट्र में जन्में के. डी. जाधव को हेलसिंकी ओलंपिक के लिए टीम चयन के दौरान साजिश का सामना करना पड़ा था. हालांकि तमाम मशक्कत के बाद आखिरकार अपनी प्रतिभा साबित कर उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह बना ली थी. तब जाधव के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे. उन्होंने सरकार से सहायता मांगी, लेकिन जाधव की आर्थिक मदद की मांग को तात्कालीन सरकारों ने अनसुना कर दिया था. तब उन्होंने गांव में चंदा मांगकर, अपनी सम्पति और घर गिरवी रखकर ओलंपिक जाने के लिये धन जुटाया था. वापस आने पर के. डी ने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीतकर लोगों का पैसा वापस कर एहसान चुकाया था. गरीबी एवं संघर्ष के बावजूद खुद्दारी में जीवन जीते हुये के. डी. जाधव की मौत 1984 में सड़क दुर्घटना में हो गई. महज आश्चर्य ही नहीं बल्कि शर्म की बात है कि ओलंपिक पदक के 50वें साल और उनकी मृत्यु के 15वें साल में 2001 में जाकर उन्हें अर्जुन सम्मान मिल सका. इस बीच एक तथ्य यह भी है कि जाधव अकेले ऐसे ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनको कोई पद्म सम्मान नहीं दिया गया.
एक गरीब परिवार औऱ तमाम संघर्ष से निकलकर दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाले एक गैरद्विज खिलाड़ी की उपेक्षा का यह मामला साधारण नहीं है, बल्कि गंभीर पक्षपात एवं सामाजिक पूर्वाग्रह का मामला भी दिखता है. हालांकि एक तथ्य यह भी है कि ओलंपिक में ज्यादातर बार मूलनिवासी (दलित-आदिवासी-पिछड़े) समाज के प्रतिभाओं ने ही देश का मान रखा है. चाहे वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हों, मुक्केबाज मैरीकॉम हो, निशानेबाज दीपीका कुमारी हो या फिर अब दीपा कर्माकर. ‘ध्यानचंद’ के साथ ‘के.डी. जाधव’ को भारत रत्न से सम्मानित कर भारत के माथे पर लगे इस पक्षपात और पूर्वाग्रह के कलंक को धोने का काम वर्तमान या भविष्य की कोई भारत सरकार कब करती है इसका इंतजार रहेगा. स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही 14 अगस्त को के.डी. जाधव की पुण्यतिथि होती है. इस महान ओलंपियन और देश का मान बढ़ाने वाले प्रेरणा पुरुष को नमन.
(जन्म: 15 जनवरी, 1926- मृत्यु: 14 अगस्त, 1984) बहुजन बाला दीपा कर्माकर से गोल्ड मेडल की उम्मीद
 ब्राजील के रियो के मशहूर मरकाना स्टेडियम में ‘सांबा’ नृत्य के साथ खेलों के महाकुम्भ ओलम्पिक की शुरुआत हो चुकी है. इसमें हिस्सा ले रहे 209 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है. अमेरिका की युवा निशानेबाज वर्जिनिया थ्रेसर ने रिओ ओलम्पिक का पहला गोल्ड जीत कर गोल्ड मैडल जीतने की होड़ की शुरुआत कर दी है. ओलम्पिक के शुरुआती दो दिनों के मध्य ही अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने तैराकी की चार गुणा 100 मीटर की फ्रीस्टाइल रिले में नया रिकार्ड कायम करते हुए अपने गोल्ड मेडलों की संख्या 19 पर पहुंचाने के साथ कुल 23 पदक जीत कर खुद को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है, जिस पर पहुंचने का सपना देखने का दुस्साहस भविष्य में शायद ही कोई और खिलाड़ी करे. इस बीच नोवाक जोकोविक और महिला टेनिस स्टार वीनस भी अपने एकल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. जहां तक भारत का सवाल है लगता है ओलम्पिक में फिस्सडी साबित होने की परम्परा में बदलाव नहीं होने जा रहा है. टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और रिकार्ड सातवीं बार ओलम्पिक में भाग ले रहे चिरयुवा लिएंडर पेस पहले ही राउंड अपने-अपने डबल्स मुकाबले हार चुके है. पिस्टल किंग जीतू राइ, जिनसे काफी उम्मीदें थी, भी दस मीटर की एयर पिस्टल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. 2004 में दक्षिण कोरिया को 5-2 से हराने के 12 साल बाद रियो ओलम्पिक में आयरलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करने के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम जिस तरह दूसरे मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ खेल समाप्त होने के महज 3 सेकेण्ड पूर्व एक और गोल खाकर हार गयी, उससे नहीं लगता कि 36 साल बाद यह गोल्ड जीत कर भारतीयों को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करेगी. भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को 2008 के बीजिंग ओलम्पिक गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा से भी पुरुषों की दस मीटर की एयर राइफल में स्पर्धा से बड़ा धक्का लगा है. लोग उनसे एक और मैडल की उम्मीद लगाये हुए थे, पर वे चौथे स्थान पर रहे. बहरहाल 31वें ओलम्पिक में भारी निराशा के बीच दीपा कर्मकार एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी हैं. उन्होंने जिम्नास्टिक के फाइनल में जगह बनाकर एक इतिहास रचने के साथ ही भारतीयों को निराशा से उबरने का एक बड़ा आधार सुलभ करा दिया है.
जहां तक इतिहास रचने का सवाल है 9 अगस्त,1993 को अगरतला के एक बहुजन परिवार में जन्मीं दीपा ने इसी अप्रैल में 31वें ओलम्पिक खेलों की कलात्मक (आर्टिस्टिक) जिम्नास्टिक्स में जगह बनाकर पहले ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है. इतिहास रचने के बाद उम्मीदों का पहाड़ सर लिए दीपा रियो पहुंची थीं. किन्तु इस्पाती टेम्परामेंट से पुष्ट दीपा प्रत्याशा के बोझ को दरकिनार के अपना स्वाभाविक खेल दिखाई और 14 अगस्त को होने वाले फाइनल में जगह बना लीं. अब पूरा देश सांसे रोके 14 अगस्त का इंतजार करने लगा है. उधर दीपा के कोच बीएस नंदी तनाव में घिर गए हैं. वह इसलिए कि अप्रैल में ही दीपा ने रियो में आयोजित टेस्ट इवेंट वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता था इसलिए पूरा देश सोच रहा है कि वह स्वर्ण लेकर ही देश लौटेगी. बहरहाल दीपा पदक जीत कर एक और नया इतिहास बना पाती हैं या नहीं, इसका पता तो 14 अगस्त को ही चल पायेगा. किन्तु यदि वह पदक नहीं भी जीत पातीं हैं तो भी जिस तरह उन्होंने ओलम्पिक में फाइनल तक सफ़र तय किया है, उससे प्रेरणा लेकर चाहें तो देश के खेल अधिकारी भारतीय खेलों की शक्ल बदल सकते हैं.
काबिले गौर है कि किसी जमाने में राष्ट्र के शौर्य का प्रतिबिम्बन युद्ध के मैदान में होता था, पर बदले जमाने में अब यह खेलों के मैदानों में होने लगा है. 21वीं सदी में विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में गण्य होने के पहले चीन ने अपना लोहा खेल के क्षेत्र में ही मनवाया था. लेकिन युद्ध हो या खेल, दोनों में ही जिस्मानी दमखम की जरुरत होती है. विशेषकर खेलों में उचित प्रशिक्षण और सुविधाओं से बढ़कर, सबसे आवश्यक दम-ख़म ही होता है. माइकल फेल्प्स, सर्गई बुबका, कार्ल लुईस, माइकल जॉनसन, मोहम्मद अली, माइक टायसन, मेरियन जोन्स, जैकी जयनार, इयान थोर्पे, सेरेना विलियम्स जैसे सर्वकालीन महान खिलाड़ियों की गगनचुम्बी सफलता के मूल में अन्यान्य सहायक कारणों के साथ, प्रमुख कारण उनका जिस्मानी दम-ख़म ही रहा है. दम-ख़म के अभाव में ही हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियाड, कॉमन वेल्थ गेम्स इत्यादि में फिसड्डी साबित होते रहे हैं.
जहां तक जिस्मानी दम-ख़म का सवाल है, हमारी भौगोलिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं है. लेकिन इससे उत्पन्न प्रतिकूलता से जूझ कर भी कुछ जातियां अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता का परिचय देती रही हैं. गर्मी-सर्दी-बारिश की उपेक्षा कर ये जातियां अपने जिस्मानी दम-ख़म के बूते अन्न उपजा कर राष्ट्र का पेट भरती रही हैं. जन्मसूत्र से महज कायिक श्रम करने वाली इन्ही परिश्रमी जातियों की संतानों में से खसाबा जाधव, मैरी कॉम, पीटी उषा, ज्योतिर्मय सिकदार, कर्णम मल्लेश्वरी, सुशील कुमार, विजयेन्द्र सिंह, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बाइचुंग भूटिया इत्यादि ने दम-ख़म वाले खेलों में भारत का मान बढाया है.
हॉकी में भारत जितनी भी सफलता अर्जित किया, प्रधान योगदान उत्पादक जातियों से आये खिलाडियों का रहा है. यहाँ अनुत्पादक जातियों से प्रकाश पादुकोण, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली इत्यादि ने वैसे ही खेलों में सफलता पायी जिनमें दम-ख़म नहीं, प्रधानतः तकनीकी कौशल व अभ्यास के सहारे चैंपियन हुआ जा सकता है. जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इसमें फ़ास्ट बोलिंग ही जिस्मानी दम-ख़म की मांग करती है. किन्तु दम-ख़म के अभाव में अनुत्पादक जातियों से आये भागवत चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट, दिलीप दोशी, आर अश्विन इत्यादि सिर्फ स्पिन में ही महारत हासिल कर सके,जिसमें दम-ख़म कम कलाइयों की करामात ही प्रमुख होती है. दम-ख़म से जुड़े फ़ास्ट बोलिंग में भारत की स्थिति पूरी तरह शर्मसार होने से जिन्होंने बचाया, वे कपिल देव, जाहिर खान, उमेश यादव, मोहम्मद शमी इत्यादि उत्पादक जातियों की संताने हैं. आज भारत में बल्लेबाजी को विस्फोटक रूप देने का श्रेय जिन कपिल देव, विनोद काम्बली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, शिखर धवन इत्यादि को जाता है, वे श्रमजीवी जातियों की ही संताने हैं. ओलम्पिक के जिमनास्ट जैसे खेल के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर दीपा कर्मकार ने ,यह सत्य नए सिरे से उजागर कर दिया है कि उत्पादक जातियों में जन्मे खिलाड़ी ही दम-ख़म वाले खेलों में सफल हो सकते हैं. दीपा की सफलता का यही सन्देश है कि हमारे खेल चयनकर्ता प्रतिभा तलाश के लिए पॉश कालोनियों का मोह त्याग कर अस्पृश्य, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं जंगल-पहाड़ों में वास कर आदिवासियों के बीच जाएं, यदि चीन की भांति भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो वंचित समाजों में जन्मी प्रतिभाओं को इसलिए भी प्रोत्साहित करना जरुरी है क्योंकि दुनिया भर में अश्वेत, महिला इत्यादि जन्मजात वंचितों में खुद को प्रमाणित करने की एक उत्कट चाह पैदा हुई है. वे खुद को प्रमाणित करने की अपनी चाह को पूरा करने के लिए खेलों को माध्यम बना रहे हैं. उनकी इस चाह का अनुमान लगा कर उन्हें दूर-दूर रखने वाले यूरोपीय देश अब अश्वेत खेल-प्रतिभाओं को नागरिकता प्रदान करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. इससे जर्मनी तक अछूता नहीं है.
स्मरण रहे एक समय हिटलर ने घोषणा की थी-सिर के ऊपर शासन कर रहे हैं ईश्वर और धरती पर शासन करने की क्षमता संपन्न एकमात्र जाति है जर्मन, विशुद्ध आर्य-रक्त उनके ही शासन काल में 1936 में बर्लिन में अनुष्ठित हुआ था ओलम्पिक. हिटलर का दावा था कि सिर्फ आर्य-रक्त ओलम्पिक में परचम फहराएगा. किन्तु आर्य-रक्त के नील गर्व को ध्वस्त कर उस ओलम्पिक में श्रेष्ठ क्रीड़ाविद जेसी ओवेन्स एवरेस्ट शिखर बन कर उभरे. अमेरिका के तरुण एथलीट, ग्रेनाईट से भी काले जेसी ओवेन्स जब बार-बार विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े हो कर गोल्ड मैडल ग्रहण कर रहे थे, श्वेतकाय लोग छोटे हो जाते थे. जेसी ओवेन्स ने 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जम्प और फिर रिले रेस:ट्रैक फिल्ड से चार-चार स्वर्ण पदक ले जीते थे. हिटलर उनकी वह सफलता बर्दाश्त न कर सके. ओवेन्स को सम्मान देना तो दूर, अनार्य रक्त के श्रेष्ठत्व से असहिष्णु हिटलर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. ब्रिटेन के लीवर पूल में जो काले कभी भेंड़-बकरियों की तरह बिकने के लिए लाये जाते थे, उन्हीं में से किसी की संतान जेसी ओवेन्स ने नस्ल विशेष की श्रेष्ठता की मिथ्या अवधारणा को ध्वंस करने की जो मुहीम बर्लिन ओलम्पिक से शुरू किया, परवर्तीकाल में खुद को प्रमाणित करने की चाह में उसे मीलों आगे बढ़ा दिया. गैरी सोबर्स, फ्रैंक वारेल, माइकल होल्डिंग, माल्कॉम मार्शल, विवि रिचर्ड्स, आर्थर ऐश, टाइगर वुड, मोहम्मद अली, होलीफील्ड, कार्ल लुईस, मोरिस ग्रीन, मर्लिन ओटो, सेरेना विलियम्स इत्यादि ने. खेलों के जरिये खुद को प्रमाणित करने की वंचित नस्लों की उत्कट चाह का अनुमान लगाकर ही हिटलर के देशवासियों ने रक्त-श्रेष्ठता का भाव विसर्जित कर देशहित में अनार्य रक्त का आयात शुरू किया. आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि खेलों में सबसे अधिक नस्लीय-विविधता हिटलर के ही देश में है. अब हिटलर के देश में कई अश्वेत खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करते देखना, एक आम बात होती जा रही है.
बहरहाल देशहित में ताकतवर अश्वेतों के प्रति श्वेतों, विशेषकर आर्य जर्मनों में आये बदलाव से प्रेरणा लेकर भारत के विविध खेल संघों के प्रमुखों को भी वंचित जातियों के खिलाड़ियों को प्रधानता देने का मन बनाना चाहिए. हालांकि खेल संघों पर हावी प्रभु जातियों के लिए यह काम आसान नहीं है. इसके लिए उन्हें राष्ट्रहित में उस वर्णवादी मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा जिसके वशीभूत होकर इस देश के द्रोणाचार्य, कर्णों को रणांगन से दूर रख एवं एकलव्यों का अंगूठा काट कर, अर्जुनों को चैंपियन बनवाते रहे हैं. अगर 21वीं सदी में भी खेल संघों में छाये द्रोणाचार्यों की मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन नहीं आता है तो भारत क्रिकेट, शतरंज, तास, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड इत्यादि खेलों में ही इतराने के लिए अभिशप्त रहेगा और ओलम्पिक मैडल देश के लिए सपना बनते जायेगा.
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. बहुजन डायवर्सिटी मिशन के अध्यक्ष हैं. उनसे संपर्क उनके मोबाइल नंबर 09313186503 पर किया जा सकता है.
ब्राजील के रियो के मशहूर मरकाना स्टेडियम में ‘सांबा’ नृत्य के साथ खेलों के महाकुम्भ ओलम्पिक की शुरुआत हो चुकी है. इसमें हिस्सा ले रहे 209 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है. अमेरिका की युवा निशानेबाज वर्जिनिया थ्रेसर ने रिओ ओलम्पिक का पहला गोल्ड जीत कर गोल्ड मैडल जीतने की होड़ की शुरुआत कर दी है. ओलम्पिक के शुरुआती दो दिनों के मध्य ही अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने तैराकी की चार गुणा 100 मीटर की फ्रीस्टाइल रिले में नया रिकार्ड कायम करते हुए अपने गोल्ड मेडलों की संख्या 19 पर पहुंचाने के साथ कुल 23 पदक जीत कर खुद को ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है, जिस पर पहुंचने का सपना देखने का दुस्साहस भविष्य में शायद ही कोई और खिलाड़ी करे. इस बीच नोवाक जोकोविक और महिला टेनिस स्टार वीनस भी अपने एकल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. जहां तक भारत का सवाल है लगता है ओलम्पिक में फिस्सडी साबित होने की परम्परा में बदलाव नहीं होने जा रहा है. टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और रिकार्ड सातवीं बार ओलम्पिक में भाग ले रहे चिरयुवा लिएंडर पेस पहले ही राउंड अपने-अपने डबल्स मुकाबले हार चुके है. पिस्टल किंग जीतू राइ, जिनसे काफी उम्मीदें थी, भी दस मीटर की एयर पिस्टल मुकाबले से बाहर हो चुके हैं. 2004 में दक्षिण कोरिया को 5-2 से हराने के 12 साल बाद रियो ओलम्पिक में आयरलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करने के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम जिस तरह दूसरे मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ खेल समाप्त होने के महज 3 सेकेण्ड पूर्व एक और गोल खाकर हार गयी, उससे नहीं लगता कि 36 साल बाद यह गोल्ड जीत कर भारतीयों को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करेगी. भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को 2008 के बीजिंग ओलम्पिक गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा से भी पुरुषों की दस मीटर की एयर राइफल में स्पर्धा से बड़ा धक्का लगा है. लोग उनसे एक और मैडल की उम्मीद लगाये हुए थे, पर वे चौथे स्थान पर रहे. बहरहाल 31वें ओलम्पिक में भारी निराशा के बीच दीपा कर्मकार एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी हैं. उन्होंने जिम्नास्टिक के फाइनल में जगह बनाकर एक इतिहास रचने के साथ ही भारतीयों को निराशा से उबरने का एक बड़ा आधार सुलभ करा दिया है.
जहां तक इतिहास रचने का सवाल है 9 अगस्त,1993 को अगरतला के एक बहुजन परिवार में जन्मीं दीपा ने इसी अप्रैल में 31वें ओलम्पिक खेलों की कलात्मक (आर्टिस्टिक) जिम्नास्टिक्स में जगह बनाकर पहले ही एक बड़ा इतिहास रच दिया है. इतिहास रचने के बाद उम्मीदों का पहाड़ सर लिए दीपा रियो पहुंची थीं. किन्तु इस्पाती टेम्परामेंट से पुष्ट दीपा प्रत्याशा के बोझ को दरकिनार के अपना स्वाभाविक खेल दिखाई और 14 अगस्त को होने वाले फाइनल में जगह बना लीं. अब पूरा देश सांसे रोके 14 अगस्त का इंतजार करने लगा है. उधर दीपा के कोच बीएस नंदी तनाव में घिर गए हैं. वह इसलिए कि अप्रैल में ही दीपा ने रियो में आयोजित टेस्ट इवेंट वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता था इसलिए पूरा देश सोच रहा है कि वह स्वर्ण लेकर ही देश लौटेगी. बहरहाल दीपा पदक जीत कर एक और नया इतिहास बना पाती हैं या नहीं, इसका पता तो 14 अगस्त को ही चल पायेगा. किन्तु यदि वह पदक नहीं भी जीत पातीं हैं तो भी जिस तरह उन्होंने ओलम्पिक में फाइनल तक सफ़र तय किया है, उससे प्रेरणा लेकर चाहें तो देश के खेल अधिकारी भारतीय खेलों की शक्ल बदल सकते हैं.
काबिले गौर है कि किसी जमाने में राष्ट्र के शौर्य का प्रतिबिम्बन युद्ध के मैदान में होता था, पर बदले जमाने में अब यह खेलों के मैदानों में होने लगा है. 21वीं सदी में विश्व आर्थिक महाशक्ति के रूप में गण्य होने के पहले चीन ने अपना लोहा खेल के क्षेत्र में ही मनवाया था. लेकिन युद्ध हो या खेल, दोनों में ही जिस्मानी दमखम की जरुरत होती है. विशेषकर खेलों में उचित प्रशिक्षण और सुविधाओं से बढ़कर, सबसे आवश्यक दम-ख़म ही होता है. माइकल फेल्प्स, सर्गई बुबका, कार्ल लुईस, माइकल जॉनसन, मोहम्मद अली, माइक टायसन, मेरियन जोन्स, जैकी जयनार, इयान थोर्पे, सेरेना विलियम्स जैसे सर्वकालीन महान खिलाड़ियों की गगनचुम्बी सफलता के मूल में अन्यान्य सहायक कारणों के साथ, प्रमुख कारण उनका जिस्मानी दम-ख़म ही रहा है. दम-ख़म के अभाव में ही हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियाड, कॉमन वेल्थ गेम्स इत्यादि में फिसड्डी साबित होते रहे हैं.
जहां तक जिस्मानी दम-ख़म का सवाल है, हमारी भौगोलिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं है. लेकिन इससे उत्पन्न प्रतिकूलता से जूझ कर भी कुछ जातियां अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता का परिचय देती रही हैं. गर्मी-सर्दी-बारिश की उपेक्षा कर ये जातियां अपने जिस्मानी दम-ख़म के बूते अन्न उपजा कर राष्ट्र का पेट भरती रही हैं. जन्मसूत्र से महज कायिक श्रम करने वाली इन्ही परिश्रमी जातियों की संतानों में से खसाबा जाधव, मैरी कॉम, पीटी उषा, ज्योतिर्मय सिकदार, कर्णम मल्लेश्वरी, सुशील कुमार, विजयेन्द्र सिंह, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, बाइचुंग भूटिया इत्यादि ने दम-ख़म वाले खेलों में भारत का मान बढाया है.
हॉकी में भारत जितनी भी सफलता अर्जित किया, प्रधान योगदान उत्पादक जातियों से आये खिलाडियों का रहा है. यहाँ अनुत्पादक जातियों से प्रकाश पादुकोण, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, गगन नारंग, गीत सेठी, विश्वनाथ आनंद, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली इत्यादि ने वैसे ही खेलों में सफलता पायी जिनमें दम-ख़म नहीं, प्रधानतः तकनीकी कौशल व अभ्यास के सहारे चैंपियन हुआ जा सकता है. जहां तक क्रिकेट का सवाल है, इसमें फ़ास्ट बोलिंग ही जिस्मानी दम-ख़म की मांग करती है. किन्तु दम-ख़म के अभाव में अनुत्पादक जातियों से आये भागवत चन्द्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट, दिलीप दोशी, आर अश्विन इत्यादि सिर्फ स्पिन में ही महारत हासिल कर सके,जिसमें दम-ख़म कम कलाइयों की करामात ही प्रमुख होती है. दम-ख़म से जुड़े फ़ास्ट बोलिंग में भारत की स्थिति पूरी तरह शर्मसार होने से जिन्होंने बचाया, वे कपिल देव, जाहिर खान, उमेश यादव, मोहम्मद शमी इत्यादि उत्पादक जातियों की संताने हैं. आज भारत में बल्लेबाजी को विस्फोटक रूप देने का श्रेय जिन कपिल देव, विनोद काम्बली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, शिखर धवन इत्यादि को जाता है, वे श्रमजीवी जातियों की ही संताने हैं. ओलम्पिक के जिमनास्ट जैसे खेल के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर दीपा कर्मकार ने ,यह सत्य नए सिरे से उजागर कर दिया है कि उत्पादक जातियों में जन्मे खिलाड़ी ही दम-ख़म वाले खेलों में सफल हो सकते हैं. दीपा की सफलता का यही सन्देश है कि हमारे खेल चयनकर्ता प्रतिभा तलाश के लिए पॉश कालोनियों का मोह त्याग कर अस्पृश्य, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं जंगल-पहाड़ों में वास कर आदिवासियों के बीच जाएं, यदि चीन की भांति भारत को विश्व महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो वंचित समाजों में जन्मी प्रतिभाओं को इसलिए भी प्रोत्साहित करना जरुरी है क्योंकि दुनिया भर में अश्वेत, महिला इत्यादि जन्मजात वंचितों में खुद को प्रमाणित करने की एक उत्कट चाह पैदा हुई है. वे खुद को प्रमाणित करने की अपनी चाह को पूरा करने के लिए खेलों को माध्यम बना रहे हैं. उनकी इस चाह का अनुमान लगा कर उन्हें दूर-दूर रखने वाले यूरोपीय देश अब अश्वेत खेल-प्रतिभाओं को नागरिकता प्रदान करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं. इससे जर्मनी तक अछूता नहीं है.
स्मरण रहे एक समय हिटलर ने घोषणा की थी-सिर के ऊपर शासन कर रहे हैं ईश्वर और धरती पर शासन करने की क्षमता संपन्न एकमात्र जाति है जर्मन, विशुद्ध आर्य-रक्त उनके ही शासन काल में 1936 में बर्लिन में अनुष्ठित हुआ था ओलम्पिक. हिटलर का दावा था कि सिर्फ आर्य-रक्त ओलम्पिक में परचम फहराएगा. किन्तु आर्य-रक्त के नील गर्व को ध्वस्त कर उस ओलम्पिक में श्रेष्ठ क्रीड़ाविद जेसी ओवेन्स एवरेस्ट शिखर बन कर उभरे. अमेरिका के तरुण एथलीट, ग्रेनाईट से भी काले जेसी ओवेन्स जब बार-बार विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े हो कर गोल्ड मैडल ग्रहण कर रहे थे, श्वेतकाय लोग छोटे हो जाते थे. जेसी ओवेन्स ने 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जम्प और फिर रिले रेस:ट्रैक फिल्ड से चार-चार स्वर्ण पदक ले जीते थे. हिटलर उनकी वह सफलता बर्दाश्त न कर सके. ओवेन्स को सम्मान देना तो दूर, अनार्य रक्त के श्रेष्ठत्व से असहिष्णु हिटलर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. ब्रिटेन के लीवर पूल में जो काले कभी भेंड़-बकरियों की तरह बिकने के लिए लाये जाते थे, उन्हीं में से किसी की संतान जेसी ओवेन्स ने नस्ल विशेष की श्रेष्ठता की मिथ्या अवधारणा को ध्वंस करने की जो मुहीम बर्लिन ओलम्पिक से शुरू किया, परवर्तीकाल में खुद को प्रमाणित करने की चाह में उसे मीलों आगे बढ़ा दिया. गैरी सोबर्स, फ्रैंक वारेल, माइकल होल्डिंग, माल्कॉम मार्शल, विवि रिचर्ड्स, आर्थर ऐश, टाइगर वुड, मोहम्मद अली, होलीफील्ड, कार्ल लुईस, मोरिस ग्रीन, मर्लिन ओटो, सेरेना विलियम्स इत्यादि ने. खेलों के जरिये खुद को प्रमाणित करने की वंचित नस्लों की उत्कट चाह का अनुमान लगाकर ही हिटलर के देशवासियों ने रक्त-श्रेष्ठता का भाव विसर्जित कर देशहित में अनार्य रक्त का आयात शुरू किया. आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि खेलों में सबसे अधिक नस्लीय-विविधता हिटलर के ही देश में है. अब हिटलर के देश में कई अश्वेत खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करते देखना, एक आम बात होती जा रही है.
बहरहाल देशहित में ताकतवर अश्वेतों के प्रति श्वेतों, विशेषकर आर्य जर्मनों में आये बदलाव से प्रेरणा लेकर भारत के विविध खेल संघों के प्रमुखों को भी वंचित जातियों के खिलाड़ियों को प्रधानता देने का मन बनाना चाहिए. हालांकि खेल संघों पर हावी प्रभु जातियों के लिए यह काम आसान नहीं है. इसके लिए उन्हें राष्ट्रहित में उस वर्णवादी मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा जिसके वशीभूत होकर इस देश के द्रोणाचार्य, कर्णों को रणांगन से दूर रख एवं एकलव्यों का अंगूठा काट कर, अर्जुनों को चैंपियन बनवाते रहे हैं. अगर 21वीं सदी में भी खेल संघों में छाये द्रोणाचार्यों की मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन नहीं आता है तो भारत क्रिकेट, शतरंज, तास, कैरम बोर्ड, बिलियर्ड इत्यादि खेलों में ही इतराने के लिए अभिशप्त रहेगा और ओलम्पिक मैडल देश के लिए सपना बनते जायेगा.
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं. बहुजन डायवर्सिटी मिशन के अध्यक्ष हैं. उनसे संपर्क उनके मोबाइल नंबर 09313186503 पर किया जा सकता है. गुजरातः जातिवाद की भेंट चढ़ें 27 दलित परिवार, अपना गांव छोड़कर बने शरणार्थी
 गुजरात के एक गांव से दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबर आई है. वहां दलितों के 27 परिवारों को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया. ये सभी परिवार अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शरणार्थियों की तरह रहने पर मजबूर हैं. यह मामला गुजरात बंसकअनथा जिले का है. ये सभी लोग दो साल पहले तक जिले के घदा नाम के गांव में रहते थे लेकिन अब ये 15 किलोमीटर दूर सोदापुर में रहने को मजबूर हैं. यहां इन लोगों के पास करने को कोई खास काम नहीं है और साथ ही साथ इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है. लोगों के मुताबिक, उनके गांव में छूआछूत इतने बड़े पैमाने पर है कि इसकी वजह से एक शख्स की जान तक ले ली गई थी. यह जिला आलू की खेती के लिए मशहूर है. यहां आलू के अलावा मूंगफली, बाजरा भी उगाया जाता है. ये दलित परिवार भी वहां लगभग 100 बीघे जमीन पर खेती किया करते थे. इन दलित परिवारों ने बताया कि छुआछूत से परेशान होकर उनके परिवार की लड़कियों के साथ-साथ लड़कों ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया. उनके मुताबिक, स्कूल वहां से दूर था और स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव होता था. बच्चे उनसे बोलने को तैयार नहीं होते थे.
ये लोग बताते हैं कि उनके परिवार में से रमेश नाम का एक लड़का था. 22 साल का रमेश पढ़ा-लिखा थ. एक दिन वह घदा के मंदिर में चला गया. इस पर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया और उसे ट्रेक्टर से कुचलकर मार दिया गया. इसके बाद गांव वालों ने सरकारी दफ्तरों के बाहर 5 साल तक प्रदर्शन किया. आखिर में दो साल पहले इन सबको सोदापुर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन इन लोगों के लिए अबतक पक्के घर नहीं बनवाए गए हैं. वहीं घदा गांव के पुराने सरपंच का कहना है कि गांव में छुआछूत नहीं है. वहीं रमेश के मर्डर पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बस एक एक्सिडेंट था.
लेकिन ये सभी दलित परिवार अब वाले सरपंच को बहुत अच्छा मानते हैं. उसका नाम अमरसिंर राजपूत है. वह इनकी काफी मदद भी कर रहा है. उसी के प्रयासों के तहत कुछ परिवार वापस घदा आ भी रहे हैं. बाकी जो परिवार अब सोदापुर में ही रहना चाहते हैं फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है. परिवारों ने बताया कि सरकार ने जमीन देने के बाद प्रत्येक घर के लिए 45 हजार रुपए दिए थे लेकिन उनमें से 10 हजार तो सिर्फ उस जगह का भराव करवाने में ही लग गए.
गुजरात के एक गांव से दलितों पर हो रहे अत्याचार की खबर आई है. वहां दलितों के 27 परिवारों को उन्हीं के गांव से निकाल दिया गया. ये सभी परिवार अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर शरणार्थियों की तरह रहने पर मजबूर हैं. यह मामला गुजरात बंसकअनथा जिले का है. ये सभी लोग दो साल पहले तक जिले के घदा नाम के गांव में रहते थे लेकिन अब ये 15 किलोमीटर दूर सोदापुर में रहने को मजबूर हैं. यहां इन लोगों के पास करने को कोई खास काम नहीं है और साथ ही साथ इनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है. लोगों के मुताबिक, उनके गांव में छूआछूत इतने बड़े पैमाने पर है कि इसकी वजह से एक शख्स की जान तक ले ली गई थी. यह जिला आलू की खेती के लिए मशहूर है. यहां आलू के अलावा मूंगफली, बाजरा भी उगाया जाता है. ये दलित परिवार भी वहां लगभग 100 बीघे जमीन पर खेती किया करते थे. इन दलित परिवारों ने बताया कि छुआछूत से परेशान होकर उनके परिवार की लड़कियों के साथ-साथ लड़कों ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया. उनके मुताबिक, स्कूल वहां से दूर था और स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव होता था. बच्चे उनसे बोलने को तैयार नहीं होते थे.
ये लोग बताते हैं कि उनके परिवार में से रमेश नाम का एक लड़का था. 22 साल का रमेश पढ़ा-लिखा थ. एक दिन वह घदा के मंदिर में चला गया. इस पर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया और उसे ट्रेक्टर से कुचलकर मार दिया गया. इसके बाद गांव वालों ने सरकारी दफ्तरों के बाहर 5 साल तक प्रदर्शन किया. आखिर में दो साल पहले इन सबको सोदापुर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन इन लोगों के लिए अबतक पक्के घर नहीं बनवाए गए हैं. वहीं घदा गांव के पुराने सरपंच का कहना है कि गांव में छुआछूत नहीं है. वहीं रमेश के मर्डर पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बस एक एक्सिडेंट था.
लेकिन ये सभी दलित परिवार अब वाले सरपंच को बहुत अच्छा मानते हैं. उसका नाम अमरसिंर राजपूत है. वह इनकी काफी मदद भी कर रहा है. उसी के प्रयासों के तहत कुछ परिवार वापस घदा आ भी रहे हैं. बाकी जो परिवार अब सोदापुर में ही रहना चाहते हैं फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है. परिवारों ने बताया कि सरकार ने जमीन देने के बाद प्रत्येक घर के लिए 45 हजार रुपए दिए थे लेकिन उनमें से 10 हजार तो सिर्फ उस जगह का भराव करवाने में ही लग गए. स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका
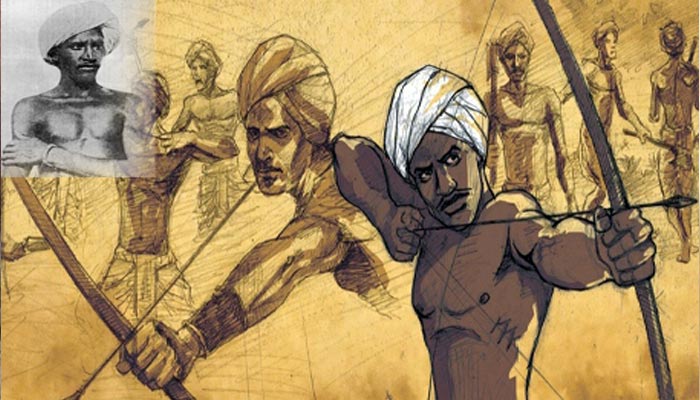 भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आन्दोलन बताया है. हकीकत में सन् 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू कर दिया था. “क्रान्ति कोष” के लेखक श्री कृष्ण “सरल” ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल सन् 1757 से सन् 1961 तक माना है. सन् 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी. सन् 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर गोवा का विलय भारत में किया गया था. स्वतंत्रता आन्दोलन का काल खण्ड यही माना जाना चाहिए.
स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गये. पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध नहीं लड़े. इसका प्रमुख कारण है आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बटा हुआ था. आज भी बंटा हुआ है. भारत में 428 जनजातियाँ अधिसूचित हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या 642 है. जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में निवास करते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियां है. ये 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं. गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के चौबीस परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं. पूर्वोत्तर के सात राज्यों-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा में आदिवासियों का बाहुल्य है. यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती प्रदेश बिहार और झारखण्ड जनजाति आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं. आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं.
मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और वे ईसाई धर्म को मानते हैं. त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिन्दू धर्म को मानते हैं. छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोड़वा, ध्रुव तथा राजगोंड में सगा समाज है. गोंड एक ही समाज होते हुए भी उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है. (आदिवासी सत्ता अंक 2, मार्च 2016) इस तरह आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं. इसलिए अपनी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग-अलग लड़ी. फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आन्दोलनों ने दिया. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा करने में आदिवासी आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कहा था अंग्रेज भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएं. महात्मा गांधी राजनैतिक सत्ता का हस्तान्तरण चाहते थे. उनका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था. सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. राजनैतिक सत्ता प्राप्ति से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जाय. इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार आन्दोलन चलाया. आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता. साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे. साहूकार से एक बार लिया हुआ कर्ज पीढ़ियों तक चुकता नहीं हो पाता था. अंततः साहूकार जमींदार की मदद से आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे. इसलिए आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी थी. यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आन्दोलन में पूर्ण स्वायत्तत्ता की मांग की थी.
महात्मा गांधी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था. महात्मा गांधी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचारों की कभी खिलाफत नहीं की. उनके खिलाफ कभी नहीं बोले. वे उनके समर्थक बने रहे. साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति रही. अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया. उन्होंने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया. ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे. राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे. इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी. आदिवासी जब जमींदारों और राजा-महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे. उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था. आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे. इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था. आदिवासियों का आन्दोलन ज्यादा व्यापक था.
आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी. अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी. आधुनिक हथियार-बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था. सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी. साहूकारों के पास धन-दौलत की ताकत थी. इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परम्परागत साधन तीन-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे. आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे. संसाधनों की कमी थी. इसलिए हर आन्दोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी. सन् 1855 में संथाल (झारखण्ड) के आदिवासी वीर योद्धा सिद्दू और कान्हू का विद्रोह हुआ. इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया. आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया. अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए. अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दे दिए गए. कत्ले आम हुआ. इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गये. रमणिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है. इसी तरह सन् 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आन्दोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आन्दोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गई.
भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन सन् 1780 में संथाल परगना में प्रारम्भ किया. दो आदिवासी वीरों तिलका और मांझी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया. यह आन्दोलन सन् 1790 तक चला. इसे ‘दामिन विद्रोह’ कहते हैं. तिलका और मांझी की गतिविधियों से अंग्रेजी सेना परेशान हो चुकी थी. इन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई. तिलका को इसकी भनक लग चुकी थी. यह देखने के लिए कि अंग्रेज सेना कहा तक पहुंची है, तिलका ताड़ के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गया. संयोग से अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छुपी हुई थी. उसका नेतृत्व मि. क्लीववलैण्ड कर रहे थे. उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था. वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा. सेना ने भी पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया था. क्लीवलैण्ड ने तिलका को ललकारा और पेड़ के नीचे उतर कर आत्म समर्पण के लिए कहा. तिलका ने क्लीवलैण्ड पर एक तीर चलाया जो उसकी छाती में जाकर लगा. क्लीवलैण्ड नीचे गिर पड़ा. छटपटाने लगा. सेना उसे संभालने के लिए भागी. इस बीच तिलका फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में गायब हो गया. अंग्रेजी सेना ने तिलका को पकड़ने के लिए छापामार युद्ध का सहारा किया. अंत में अंग्रेज सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल हो गई. अपनी हानि और बदला लेने के लिए तिलका को अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी. अपने प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए तिलका शहीद हो गया. तिलका स्वतंत्रता आन्दोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए. लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद घोषित कर दिया. सच्चाई यह है कि मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलका शहीद हुआ था.
भारत का सही इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया. सवर्ण इतिहासकारों ने जो भी लिखा वह पक्षपातपूर्ण और एक तरफा लिखा. विडम्बना है कि दलितों और आदिवासियों को सदैव इतिहास से बाहर रखा गया. उनके बड़े से बड़े त्याग, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में उल्लेख तक नहीं किया गया. सन् 1780 से सन् 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों स्वतंत्रता आन्दोलन किए. सन् 1780 का “दामिन विद्रोह” जो तिलका मांझी ने चलाया, सन् 1855 का “सिहू कान्हू विद्रोह”, सन् 1828 से 1832 तक बुधू भगत द्वारा चलाया गया “लरका आन्दोलन” बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आन्दोलन हैं. इतिहास में इन आन्दोलनों का कहीं जिक्र तक नहीं है. इसी तरह आदिवासी क्रान्तिवीरों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण गंवाएं उनका भी इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुआ. मध्य प्रदेश के नीमाड़ का पहला विद्रोही भील तांतिया उर्फ टंटिया मामा सन् 1888 में शहीद हुआ. इसी तरह आदिवासी युग पुरूष बिरसा मुण्डा सन् 1900 में शहीद हुआ. जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. सन् 1913 में हुए मानगढ़ आन्दोलन के नायक गोविन्द गुरू का भी इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है. इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया अलबता इनके इतिहास को विकृत और विलुप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आदिवासी आन्दोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए वीर नारायणसिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुण्डा को डकैत और लुटेरा बताया, जबकि वे आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आन्दोलनों का सफल नेतृत्व किया है. इतिहासकारों ने अपने लेखन धर्म को निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया.
इतिहास की सच्चाई यह है कि सन् 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आन्दोलनों में लाखों आदिवासी मारे गये. दूसरी तरफ सन् 1857 से 1947 तक 90 वर्षों में गैर आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गये होंगे. अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार सन् 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुआ था. उसमें 379 लोग शहीद हुए थे. इसके मुकाबले सन् 1855 में हुए सिहू और कान्हू विद्रोह में 10 हजार आदिवासी शहीद हुए थे. आदिवासियों के ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं. यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने इन आन्दोलनों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया.
इतिहासकारों ने ऐसा करके भारत के सम्पूर्ण इतिहास को ही संदिग्ध और अविश्वसनीय बना दिया है. निसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आज आवश्यकता सही इतिहास लेखन की है.
भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति को स्वतंत्रता संग्राम का पहला आन्दोलन बताया है. हकीकत में सन् 1857 से 100 साल पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन शुरू कर दिया था. “क्रान्ति कोष” के लेखक श्री कृष्ण “सरल” ने राष्ट्रीय आन्दोलन का काल सन् 1757 से सन् 1961 तक माना है. सन् 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हराकर भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी थी. सन् 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाकर गोवा का विलय भारत में किया गया था. स्वतंत्रता आन्दोलन का काल खण्ड यही माना जाना चाहिए.
स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है. यह सच है कि आदिवासियों द्वारा चलाये गए आन्दोलन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर ही लड़े गये. पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने कभी अंग्रेजों के विरूद्ध युद्ध नहीं लड़े. इसका प्रमुख कारण है आदिवासी कई उपजातियों और समूहों में बटा हुआ था. आज भी बंटा हुआ है. भारत में 428 जनजातियाँ अधिसूचित हैं जबकि इनकी वास्तविक संख्या 642 है. जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में निवास करते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत आदिवासी जातियां है. ये 19 राज्यों और 6 केन्द्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं. गुजरात के डांग जिले से लेकर बंगाल के चौबीस परगना तक देश के 70 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं. पूर्वोत्तर के सात राज्यों-मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और त्रिपुरा में आदिवासियों का बाहुल्य है. यही कारण है कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती प्रदेश बिहार और झारखण्ड जनजाति आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं. आदिवासी पूर्वोत्तर के सात राज्यों के अलावा झारखण्ड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में बसे हुए हैं.
मेघालय में 16 तरह की जनजातियां हैं और वे ईसाई धर्म को मानते हैं. त्रिपुरा में 19 जनजातियां हैं जो ईसाई, बौद्ध और हिन्दू धर्म को मानते हैं. छत्तीसगढ़ के विलासपुर संभाग में जेवरा गोंड के अलावा सरगुजिया, रतनपुरिया, मटकोड़वा, ध्रुव तथा राजगोंड में सगा समाज है. गोंड एक ही समाज होते हुए भी उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं है. (आदिवासी सत्ता अंक 2, मार्च 2016) इस तरह आदिवासी कई समूहों में बटे हुए हैं. इसलिए अपनी स्वायत्तता की लड़ाई भी अलग-अलग लड़ी. फिर भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को आधार आदिवासियों के इन्हीं आन्दोलनों ने दिया. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन को खड़ा करने में आदिवासी आन्दोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
महात्मा गांधी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कहा था अंग्रेज भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएं. महात्मा गांधी राजनैतिक सत्ता का हस्तान्तरण चाहते थे. उनका उद्देश्य राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना था. सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़ी। डॉ. अम्बेडकर ने कहा सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है. राजनैतिक सत्ता प्राप्ति से पहले दलितों को सामाजिक समानता और स्वतंत्रता दी जाय. इसीलिए उन्होंने अछूतोद्धार आन्दोलन चलाया. आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी, जितनी सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रता. साहूकार आदिवासियों का जमकर शोषण कर रहे थे. साहूकार से एक बार लिया हुआ कर्ज पीढ़ियों तक चुकता नहीं हो पाता था. अंततः साहूकार जमींदार की मदद से आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते थे. इसलिए आदिवासियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी थी. यही कारण है कि आदिवासियों ने हर आन्दोलन में पूर्ण स्वायत्तत्ता की मांग की थी.
महात्मा गांधी ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया था. महात्मा गांधी ने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के अन्याय और अत्याचारों की कभी खिलाफत नहीं की. उनके खिलाफ कभी नहीं बोले. वे उनके समर्थक बने रहे. साहूकारों के शोषण के संबंध में भी उनकी यही नीति रही. अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर सीधा शासन नहीं किया. उन्होंने राजा-महाराजाओं, सामंतों और जमींदारों के माध्यम से शासन चलाया. ब्रिटिश शासकों को कोई कानून भारतीय जनता पर लागू करवाना होता तो इन्हीं के मार्फत लागू करवाते थे. राजस्व वसूली भी राजा-महाराजाओं और जमींदारों के माध्यम से ही करते थे. इसलिए आदिवासियों की सीधी लड़ाई जमींदारों और सामंतों से होती थी. आदिवासी जब जमींदारों और राजा-महाराजाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे तब वे अंग्रेजी हुकूमत से मदद मांगते थे. उनकी मदद के लिए अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को अंग्रेजी सेना और जमींदारों से सीधा मुकाबला करना पड़ता था. आदिवासी साहूकारों के भी खिलाफ थे. इसलिए साहूकार भी जमींदारों का साथ देते थे. ऐसी स्थिति में आदिवासियों को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के हर आन्दोलन में अंग्रेजी हुकूमत के साथ-साथ सामंतों और साहूकारों से भी संघर्ष करना पड़ा था. आदिवासियों का आन्दोलन ज्यादा व्यापक था.
आदिवासियों को स्वतंत्रता आन्दोलनों की भारी कीमत चुकानी पड़ी. अंग्रेजों के पास भारी संख्या में सुसज्जित सेना थी. आधुनिक हथियार-बंदूकें, तोपें, गोला और बारूद था. सामंतों के पास प्रशिक्षित पुलिस फोर्स थी. साहूकारों के पास धन-दौलत की ताकत थी. इनके मुकाबले में आदिवासियों के पास युद्ध के परम्परागत साधन तीन-कमान, भाले, फरसे और गण्डासे थे. आदिवासी आर्थिक रूप से कमजोर थे. संसाधनों की कमी थी. इसलिए हर आन्दोलन में आदिवासियों को जान-माल की भारी क्षति उठानी पड़ी. सन् 1855 में संथाल (झारखण्ड) के आदिवासी वीर योद्धा सिद्दू और कान्हू का विद्रोह हुआ. इसमें 30-35 हजार आदिवासियों ने भाग लिया. आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया. अनेक अंग्रेज सैनिक और अधिकारी मारे गए. अंत में पूरे क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर दिया गया. मार्शल लॉ लागू कर दिया गया. देखते ही गोली मारने के आदेश सेना को दे दिए गए. कत्ले आम हुआ. इसमें 10 हजार आदिवासी मारे गये. रमणिका गुप्ता तथा माता प्रसाद ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है. इसी तरह सन् 1913 में मानगढ़ में हुए आदिवासी आन्दोलन में भी 1500 आदिवासी शहीद हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि आदिवासी आन्दोलनों में लाखों आदिवासियों की जानें गई.
भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आन्दोलन सन् 1780 में संथाल परगना में प्रारम्भ किया. दो आदिवासी वीरों तिलका और मांझी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया. यह आन्दोलन सन् 1790 तक चला. इसे ‘दामिन विद्रोह’ कहते हैं. तिलका और मांझी की गतिविधियों से अंग्रेजी सेना परेशान हो चुकी थी. इन्हें पकड़ने के लिए सेना भेजी गई. तिलका को इसकी भनक लग चुकी थी. यह देखने के लिए कि अंग्रेज सेना कहा तक पहुंची है, तिलका ताड़ के ऊँचे पेड़ पर चढ़ गया. संयोग से अंग्रेजी सेना पास की झाड़ियों में छुपी हुई थी. उसका नेतृत्व मि. क्लीववलैण्ड कर रहे थे. उसने तिलका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था. वह घोड़े पर सवार होकर पेड़ के पास पहुंचा. सेना ने भी पेड़ के चारों तरफ घेरा डाल दिया था. क्लीवलैण्ड ने तिलका को ललकारा और पेड़ के नीचे उतर कर आत्म समर्पण के लिए कहा. तिलका ने क्लीवलैण्ड पर एक तीर चलाया जो उसकी छाती में जाकर लगा. क्लीवलैण्ड नीचे गिर पड़ा. छटपटाने लगा. सेना उसे संभालने के लिए भागी. इस बीच तिलका फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में गायब हो गया. अंग्रेजी सेना ने तिलका को पकड़ने के लिए छापामार युद्ध का सहारा किया. अंत में अंग्रेज सेना तिलका को गिरफ्तार करने में सफल हो गई. अपनी हानि और बदला लेने के लिए तिलका को अंग्रेजों ने पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी. अपने प्रदेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए तिलका शहीद हो गया. तिलका स्वतंत्रता आन्दोलन का पहला शहीद माना जाना चाहिए. लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने सन् 1857 की क्रान्ति में शहीद हुए मंगल पाण्डे को स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद घोषित कर दिया. सच्चाई यह है कि मंगल पाण्डे से 70 साल पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में तिलका शहीद हुआ था.
भारत का सही इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया. सवर्ण इतिहासकारों ने जो भी लिखा वह पक्षपातपूर्ण और एक तरफा लिखा. विडम्बना है कि दलितों और आदिवासियों को सदैव इतिहास से बाहर रखा गया. उनके बड़े से बड़े त्याग, बलिदान और शौर्य गाथाओं का इतिहास में उल्लेख तक नहीं किया गया. सन् 1780 से सन् 1857 तक आदिवासियों ने अनेकों स्वतंत्रता आन्दोलन किए. सन् 1780 का “दामिन विद्रोह” जो तिलका मांझी ने चलाया, सन् 1855 का “सिहू कान्हू विद्रोह”, सन् 1828 से 1832 तक बुधू भगत द्वारा चलाया गया “लरका आन्दोलन” बहुत प्रसिद्ध आदिवासी आन्दोलन हैं. इतिहास में इन आन्दोलनों का कहीं जिक्र तक नहीं है. इसी तरह आदिवासी क्रान्तिवीरों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण गंवाएं उनका भी इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 1857 में शहीद हुआ. मध्य प्रदेश के नीमाड़ का पहला विद्रोही भील तांतिया उर्फ टंटिया मामा सन् 1888 में शहीद हुआ. इसी तरह आदिवासी युग पुरूष बिरसा मुण्डा सन् 1900 में शहीद हुआ. जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. सन् 1913 में हुए मानगढ़ आन्दोलन के नायक गोविन्द गुरू का भी इतिहास में कहीं उल्लेख तक नहीं है. इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया अलबता इनके इतिहास को विकृत और विलुप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई. आदिवासी आन्दोलनकारियों की छवि खराब करने के लिए वीर नारायणसिंह, टंटिया मामा और बिरसा मुण्डा को डकैत और लुटेरा बताया, जबकि वे आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय रहे हैं और स्वतंत्रता आन्दोलनों का सफल नेतृत्व किया है. इतिहासकारों ने अपने लेखन धर्म को निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं निभाया.
इतिहास की सच्चाई यह है कि सन् 1780 से 1857 तक 77 वर्षों में आदिवासियों द्वारा किए गए स्वतंत्रता आन्दोलनों में लाखों आदिवासी मारे गये. दूसरी तरफ सन् 1857 से 1947 तक 90 वर्षों में गैर आदिवासियों द्वारा किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनों में एक हजार लोग भी नहीं मारे गये होंगे. अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में सबसे बड़ा नरसंहार सन् 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुआ था. उसमें 379 लोग शहीद हुए थे. इसके मुकाबले सन् 1855 में हुए सिहू और कान्हू विद्रोह में 10 हजार आदिवासी शहीद हुए थे. आदिवासियों के ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं. यह अलग बात है कि इतिहासकारों ने इन आन्दोलनों का कहीं उल्लेख तक नहीं किया.
इतिहासकारों ने ऐसा करके भारत के सम्पूर्ण इतिहास को ही संदिग्ध और अविश्वसनीय बना दिया है. निसंदेह स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. आज आवश्यकता सही इतिहास लेखन की है. दलित आंदोलन से बैकफुट पर भाजपा
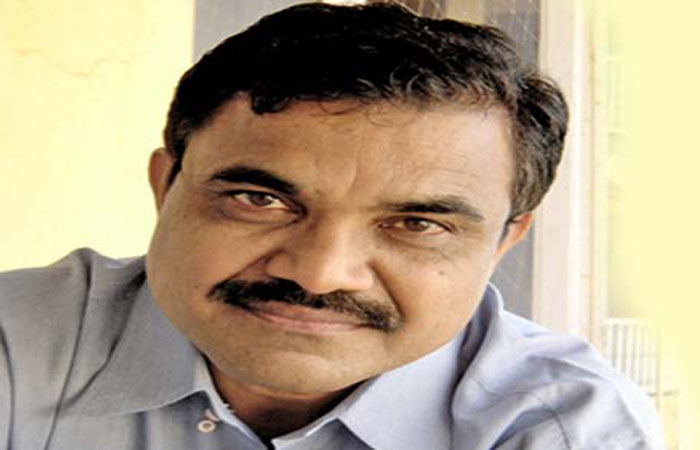 हाल ही में सहज रूप से शुरू हुए दलित आंदोलनों की लहर में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर देश भर के छात्रों का विरोध हो या फिर गुजरात में सबकी आंखों के सामने चार दलित नौजवानों को सरेआम पीटे जाने की शर्मनाक घटना पर राज्य में चल रहा विरोध हो, या फिर मुंबई में ऐतिहासिक आंबेडकर भवन को गिराए जाने पर 19 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन हो, या राजस्थान में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या पर उभरा गुस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष द्वारा की “वेश्या वाली टिप्पणी” पर राज्य में होने वाला भारी विरोध हो, भाजपा के खिलाफ दलितों के गुस्से को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. भाजपा के दलित हनुमान चाहे इस आग को जितना भी बुझाने की कोशिश करें, यह नामुमकिन है कि अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों तक यह बुझ पाएगी. इससे भी बढ़ कर, इन प्रदर्शनों में उठ खड़े होने का एक जज्बा भी है, एक ऐसा जज्बा जिसमें इसका अहसास भरा हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है. अगर यह बात सही है तो फिर यह संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की परियोजना की जड़ों में मट्ठा डाल सकती है.
रोहिथ की बार-बार हत्या
रोहिथ की संस्थागत हत्या के बारे में अब सब इतना जानते हैं कि उस पर यहां अलग से चर्चा करना जरूरी नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है वो हत्या से कम आपराधिक नहीं है. गाचीबावड़ी पुलिस ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवादास्पद वाइस चांसलर अप्पा राव पोडिले, भाजपा सांसद और मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और एचसीयू में एबीवीपी के अध्यक्ष एन. सुशील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की. रोहिथ की मौत ने छात्रों में आंदोलन की चिन्गारी सुलगा दी थी, जिन्होंने देश भर में ज्वाइंट एक्शन कमेटियां गठित की थीं. इसने अप्पा राव को कैंपस से भाग जाने पर मजबूर किया था.
लेकिन 22 मार्च को, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखने पर वो एकाएक वापस लौटे. स्वाभाविक रूप से आंदोलनकारी छात्रों ने वाइस-चांसलर के आवास के बाहर, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्हें पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ने घेर रखा था. जब आंदोलनकारी छात्रों ने एबीवीपी के सदस्यों को इमारत के भीतर देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. उन्होंने भीतर जाना चाहा. दरवाजे पर होने वाली इस धक्का-मुक्की की ओट में पुलिस ने गंभीर लाठी चार्ज किया. पुलिस से बातें करने गए दो फैकल्टी सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने छात्रों को कई किलोमीटर तक झाड़ियों में खदेड़ते हुए पीटा. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ भी की.
सभी 27 छात्र और दो फैकल्टी सदस्य प्रो. के.वाई. रत्नम और तथागत सेनगुप्ता को दो पुलिस वैनों में भर दिया गया और फिर हैदराबाद की सड़कों पर घंटों तक चक्कर लगाती उन वैनों में उन पर बेरहम हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ. देर शाम तक उनके ठिकाने की कोई खबर नहीं थी. आखिर वे सात दिनों तक कैद रहने के बाद जमानत पर ही बाहर आ सके. रोहिथ को इंसाफ देने का तो सवाल ही नहीं था, जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उन्हें ही सजाएं दी जा रही थीं.
मानो इतना ही काफी न हो, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसरों को बाद में निलंबित कर दिया गया. जब विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर उन्होंने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करते हुए इसका विरोध किया तो जनता और अनेक प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन की बाढ़ आ गई. नतीजों से डरे हुए अप्पा राव के होश ठिकाने आए और उन्होंने निलंबन के आदेश वापस लिए.
विवादास्पद मंत्री और सबसे अहम मानव संसाधन मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिहाज से सबसे नाकाबिल स्मृति ईरानी ने अपने और अपने चापलूसों की करतूतों को जायज ठहराने के लिए संसद में झूठ का पुलिंदा पेश करने में अपना सारा का सारा नाटकीय कौशल लगा दिया. जो कुछ हुआ था, उस पर पछताने के बजाए उन्होंने रोहिथ के इंसाफ का आंदोलन करने वालों पर आक्रामक हमला किया. रोहिथ की जाति पर सवाल उठा कर इस मामले को भटकाने की घिनौनी कौशिशें की गईं मानो उनका दलितपन उन्हें हाथोहाथ इंसाफ दिला देगा और उनका दलित न होना अपराधियों के अपराध को हल्का कर देगा.
तेलंगाना राज्य की पूरी ताकत-जिसके लिए करीब 600 लोगों ने अपनी जान दे दी थी और उनमें से अनेक दलित थे-मातम में डूबी हुई मां पर टूट पड़ी कि वो अपनी जाति साबित करें. रोहिथ के पास दलित होने का जाति प्रमाणपत्र होने के बावजूद, एक दलित की जिंदगी जीने और मरने के बावजूद, तेलंगाना प्रशासन ने यह अफवाह फैलाई कि वो दलित नहीं, एक वड्डेरा थे. यह साबित करने के लिए परिवार को जगह-जगह दौड़ाया गया कि रोहिथ असल में एक दलित थे. उन्हें अपने बेटे को खो देने के दर्द को परे कर देना पड़ा. किस्मत से सरकार की सारी तरकीबें नाकाम रहीं और रोहिथ का दलित होना साबित हुआ.
जैसी कि उम्मीद थी, अपराधियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा. वे सभी ताकत के अपने पदों पर जमे हुए हैं, जबकि इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को आखिरी हदों तक धकेला जा रहा है. अप्पा राव ने उस दलित वीथि को हटा दिया है, जो रोहिथ और उनके चार निष्कासित साथियों की आखिरी शरण स्थली थी, जिसे उन्होंने शॉपकॉम पर खड़ा किया था. यह जगह मौजूदा आंदोलन का एक प्रतीकात्मक केंद्र थी. वहां लगाई गई आंबेडकर की प्रतिमा भी चुरा ली गई और रोहिथ के अस्थायी स्मारक पर लगाए गए रोहिथ के पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया गया.
गुजरात में गुंडागर्दी
11 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार, जाति द्वारा नियत अपने पेशे के मुताबिक एक मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहा था, कि गौ रक्षा समिति का भेष धरे शिव सेना का एक समूह उनके पास पहुंचा. उन्होंने गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को उठा लिया. उन्होंने उनकी कमर में जंजीर बांध कर उन्हें एक एसयूवी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए उना कस्बे तब ले आए, जहां एक पुलिस थाने के करीब उनको कई घंटों तक सबकी नजरों के सामने पीटा गया.
हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन्हें इस पर कभी भी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी इस खौफनाक हरकत का वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक भी किया. लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. इससे भड़क उठे दलित खुद ब खुद सड़कों पर उतर पड़े. हालांकि गुजरात कभी भी दलितों की स्थिति के लिहाज से आदर्श राज्य नहीं रहा था, लेकिन यह दलितों पर ऐसे दिन-दहाड़े अत्याचार का कभी गवाह नहीं रहा था.
राज्य भर में दलितों के भारी विरोध प्रदर्शनों की एक स्वाभाविक लहर दौड़ गई. करीब 30 दलितों ने अपने समुदाय के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की. लेकिन सबसे समझदारी भरी कार्रवाई मवेशियों की लाशों को अनेक जगहों पर कलेक्टर कार्यालयों के सामने डाल देना था. दलितों ने एकजुटता जाहिर करने की एक गैरमामूली कदम उठाते हुए लाशें उठाने और उनका चमड़ा उतारने का अपना परंपरागत काम रोक दिया और इस तरह इनसे होने वाली आमदनी की भी कुर्बानी दी.
28 जुलाई के द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर जगह सड़ती हुई लाशें एक महामारी का खतरा बन गई हैं. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में करीब एक करोड़ गायें और भैंसें हैं जिनके मरने की दर 10 फीसदी है. इसका मतलब ये है कि हर रोज राज्य भर में 2,740 मवेशी मरते हैं. किसी जगह पर ऐसी ही पड़ी एक लाश की बदबू जनता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और ऐसे में ऊपर दी गई तादाद तो एक तबाही ही ला सकती है.
गौरक्षा संस्थाओं को होश आ गया है और वे यह कबूल करने को मजबूर हुई हैं कि वो इस समस्या के बारे में नहीं जानती थीं और अब वे लाशों का निबटारा करने के तरीके खोजेंगी. अगर देश भर के नहीं तो पूरे राज्य में मैला ढोने के काम में लगे दलितों (सरकारों द्वारा कसम खा कर उनके वजूद को नकारने के बावजूद उनकी तादाद हजारों में है) और इसी तरह पूरे राज्य के सफाई कर्मियों को भी इस विरोध का हिस्सा बन जाना चाहिए.
आम्बेडकर की विरासत चकनाचूर
25 जून की रात में आम्बेडकरियों का भेस धरे सैकड़ों गुंडे दो बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मुंबई में दादर में स्थित ऐतिहासिक आम्बेडकर भवन और आम्बेडकर प्रेस को गिरा दिया. ऐसा उन्होंने रत्नाकर गायकवाड़ के कहने पर किया, जो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे हैं. प्रेस का एक ऐतिहासिक मूल्य था, क्योंकि उसका संबंध बाबासाहेब आम्बेडकर से था. उनके अहम अखबारों में से दो जनता और प्रबुद्ध भारत यहीं से छपते और प्रकाशित होते थे और यह 1940 के दशक में आम्बेडकरी आंदोलन का एक केंद्र भी था. उनके निधन के बाद भी यह एक केंद्र बना रहा; भूमि संघर्ष पर आंदोलन, ‘रिडल्स’ विवाद पर आंदोलन और नामांतर संघर्षों की योजना यहीं बनी और उन अमल हुआ.
दूसरी इमारत आम्बेडकर भवन एक एकमंजिला, अंग्रेजी के “यू” अक्षर के उल्टे शक्ल की थी जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था. इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए जिस बहाने की ओट ली गई, कि वे ढांचागत रूप से खतरनाक थे, वे जाहिर तौर पर गायकवाड़ द्वारा “गढ़े” गए थे. इस दुस्साहस भरी कार्रवाई से और इससे भी ज्यादा जिस शर्मनाक और उद्दंड तरीके से उसको जायज ठहराया जा रहा था, उससे लोग भौंचक रह गए. जैसा कि इसके पहले और इसके बाद होने वाली घटनाओं ने उजागर किया, गायकवाड़ राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हाथों का मोहरा भर थे.
ट्रस्ट की विवादास्पद स्थिति से वाकिफ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 17 मंजिला आम्बेडकर भवन के लिए चोरी-छिपे भूमिपूजन किया (और मजे की बात है कि यह पूजा कहीं और की गई) और इसके लिए 60 करोड़ के अनुदान का ऐलान भी किया. 25 जून को जो कुछ हुआ था, वह खुल्लम-खुल्ला एक आपराधिक करतूत थी, जिसको मजबूरन गायकवाड़ को कबूल करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से बचने के लिए उनकी संवैधानिक हैसियत का एक झूठा बहाने को सामने कर दिया गया.
गायकवाड़ और भाजपा सरकार के अपराधों से नाराजगी के साथ 19 जुलाई को मुंबई में एक भारी मोर्चा निकाला गया. घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने दलितों के भीतर वर्गीय बंटवारे को सबसे बदसूरत तरीके से उजागर किया. जहां उच्च मध्य वर्ग के दलितों ने गायकवाड़ का समर्थन किया, जिसमें प्रवासी दलित (डायस्पोरा) तबका और दलित नौकरशाहों से मिले हराम के पैसों पर आरामतलबी की जिंदगी जीते बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं. दूसरी तरफ दलितों की व्यापक बहुसंख्या ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और आम्बेडकर परिवार का समर्थन किया जो गायकवाड़ के खिलाफ खड़े थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के तीनों पोते आमतौर पर स्वतंत्र रहे हैं और कांग्रेस या भाजपा के साथ सहयोग करने से इन्कार किया है. राजनीतिक रूप से उनका नजरिया अवाम के हक में रहा है और उन्होंने जनसंघर्षों का समर्थन किया है. चाहे जितना भी कमजोर हो, आज वे अकेले आम्बेडकरी प्रतिष्ठान है जो पूरी मजबूती से हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ हैं.
इसलिए भाजपा के लिए उनकी छवि को बदनाम करना जरूरी है. इस काम को पूरा करने के लिए मध्यवर्ग के दलितों के एक हिस्से को चुपचाप उकसाया जा रहा है. धीरे-धीरे उन्होंने यह प्रचार खड़ा किया है कि बाबासाहेब आम्बेडकर के वारिस आम्बेडकरी नहीं बल्कि माओवाद के समर्थक हैं. कम से कम एक दलित अखबार महानायक पिछले पांच बरसों से इस झूठ को पूरे उन्माद के साथ फैलाता आ रहा है. इमारतों को तोड़े जाने के इस पूरे नाटक के जरिए भाजपा का इरादा इसी मकसद को हासिल करने का था. गायकवाड़ ने तीनों पोतों और उनके पिता यशवंतराव आम्बेडकर को गैर कानूनी कब्जा करने वाले नालायक और गुंडा बताया.
आम्बेडकर भवन को गिराना और आम्बेडकर के परिवार की छवि को मिट्टी में मिलाना, गायकवाड़ के ये वो दो जुड़वां काम थे जिनके लिए उन्हें देश भर में भड़कते जनता के गुस्से की अनदेखी करते हुए भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है. इस खुलेआम आपराधिक मामले में पुलिस और राज्य मशीनरी जिस तरह पेश आती रही है और आ रही है उसी से सरकार का तौर-तरीका साफ हो जाता है.
दलित “हनुमानों” की बेशर्मी
भाजपा अपने तीनों दलित रामों को अपना ‘हनुमान’ बना देने में कामयाब रही है. उन्होंने कुछ तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को भी लालच देते हुए अपनी हां में हां मिलाने के लिए अपनी तरफ खींचा है. गुजरात में दलित नौजवानों को पीटे जाने पर देश भर में भड़क उठे गुस्से के ताप में भी, एक दलित “हनुमान” ऐसा था जो बेशर्मी से यह कहता फिर रहा था कि दलितों पर अत्याचारों से गुजरात का नाम नहीं जोड़ा जाए. जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध के आंकड़ों को गलत और संदर्भ से हटा कर पेश किया, उसी से उनकी गुलामी और बौद्धिक बेईमानी जाहिर होती है. एक तरफ जब गैर-दलित पैनलिस्ट गुजरात में भड़के गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, यह पिट्ठू बड़े भद्दे तरीके से यह बहस कर रहा था कि जातीय अत्याचारों के मामले में गुजरात अनेक राज्यों से बेहतर है.
तथ्य ये है कि दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं के मामले में गुजरात के सिर पर, ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का एक खास ताज रखा हुआ है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का “वाइब्रेट गुजरात” का जाप चरम पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों (एससी) की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की तादाद उसके पहले वाले साल के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई. इसके नतीजे में राज्य देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया.
पहले गलत तरीका अपनाते हुए एनसीआरबी अत्याचारों की गिनती प्रति लाख आबादी पर करता आ रहा था; सिर्फ 2012 से यह प्रति लाख एससी आबादी के संदर्भ में घटनाओं को जुटा रहा है. इसलिए एनसीआरबी तालिकाओं में दी गई एससी के खिलाफ अपराध की घटनाओं की दरों को सही आंकड़ों में बदलने की जरूरत होगी, लेकिन उनसे भी राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति के बदलने की संभावना कम ही है.
हत्या और बलात्कार जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात बदतरीन राज्यों में से है. तालिका एक भारत के बड़े राज्यों में 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें मुहैया कराती है, ताकि दिखाया जा सके कि कैसे दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए गुजरात का नाम ऊपर के राज्यों में आता है.
हाल ही में सहज रूप से शुरू हुए दलित आंदोलनों की लहर में एक खास भाजपा-विरोधी रंग है. चाहे वह रोहिथ वेमुला की सांस्थानिक हत्या पर देश भर के छात्रों का विरोध हो या फिर गुजरात में सबकी आंखों के सामने चार दलित नौजवानों को सरेआम पीटे जाने की शर्मनाक घटना पर राज्य में चल रहा विरोध हो, या फिर मुंबई में ऐतिहासिक आंबेडकर भवन को गिराए जाने पर 19 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन हो, या राजस्थान में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के कथित बलात्कार और हत्या पर उभरा गुस्सा हो या फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए भाजपा के उपाध्यक्ष द्वारा की “वेश्या वाली टिप्पणी” पर राज्य में होने वाला भारी विरोध हो, भाजपा के खिलाफ दलितों के गुस्से को साफ-साफ महसूस किया जा सकता है. भाजपा के दलित हनुमान चाहे इस आग को जितना भी बुझाने की कोशिश करें, यह नामुमकिन है कि अगले साल राज्यों में होने वाले चुनावों तक यह बुझ पाएगी. इससे भी बढ़ कर, इन प्रदर्शनों में उठ खड़े होने का एक जज्बा भी है, एक ऐसा जज्बा जिसमें इसका अहसास भरा हुआ है कि उनके साथ धोखा हुआ है. अगर यह बात सही है तो फिर यह संघ परिवार के हिंदू राष्ट्र की परियोजना की जड़ों में मट्ठा डाल सकती है.
रोहिथ की बार-बार हत्या
रोहिथ की संस्थागत हत्या के बारे में अब सब इतना जानते हैं कि उस पर यहां अलग से चर्चा करना जरूरी नहीं है. लेकिन जिस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है वो हत्या से कम आपराधिक नहीं है. गाचीबावड़ी पुलिस ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विवादास्पद वाइस चांसलर अप्पा राव पोडिले, भाजपा सांसद और मोदी के मंत्रिमंडल के मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और एचसीयू में एबीवीपी के अध्यक्ष एन. सुशील कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए उत्पीड़न अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है. लेकिन पुलिस ने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की. रोहिथ की मौत ने छात्रों में आंदोलन की चिन्गारी सुलगा दी थी, जिन्होंने देश भर में ज्वाइंट एक्शन कमेटियां गठित की थीं. इसने अप्पा राव को कैंपस से भाग जाने पर मजबूर किया था.
लेकिन 22 मार्च को, मामला थोड़ा ठंडा पड़ता दिखने पर वो एकाएक वापस लौटे. स्वाभाविक रूप से आंदोलनकारी छात्रों ने वाइस-चांसलर के आवास के बाहर, जहां वे एक मीटिंग कर रहे थे, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया. उन्हें पुलिस की एक बड़ी सी टुकड़ी ने घेर रखा था. जब आंदोलनकारी छात्रों ने एबीवीपी के सदस्यों को इमारत के भीतर देखा तो उन्हें बड़ा धक्का लगा. उन्होंने भीतर जाना चाहा. दरवाजे पर होने वाली इस धक्का-मुक्की की ओट में पुलिस ने गंभीर लाठी चार्ज किया. पुलिस से बातें करने गए दो फैकल्टी सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया. उन्होंने छात्रों को कई किलोमीटर तक झाड़ियों में खदेड़ते हुए पीटा. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ भी की.
सभी 27 छात्र और दो फैकल्टी सदस्य प्रो. के.वाई. रत्नम और तथागत सेनगुप्ता को दो पुलिस वैनों में भर दिया गया और फिर हैदराबाद की सड़कों पर घंटों तक चक्कर लगाती उन वैनों में उन पर बेरहम हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ. देर शाम तक उनके ठिकाने की कोई खबर नहीं थी. आखिर वे सात दिनों तक कैद रहने के बाद जमानत पर ही बाहर आ सके. रोहिथ को इंसाफ देने का तो सवाल ही नहीं था, जो लोग इसकी मांग कर रहे थे उन्हें ही सजाएं दी जा रही थीं.
मानो इतना ही काफी न हो, गिरफ्तार किए गए प्रोफेसरों को बाद में निलंबित कर दिया गया. जब विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर उन्होंने अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल करते हुए इसका विरोध किया तो जनता और अनेक प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन की बाढ़ आ गई. नतीजों से डरे हुए अप्पा राव के होश ठिकाने आए और उन्होंने निलंबन के आदेश वापस लिए.
विवादास्पद मंत्री और सबसे अहम मानव संसाधन मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिहाज से सबसे नाकाबिल स्मृति ईरानी ने अपने और अपने चापलूसों की करतूतों को जायज ठहराने के लिए संसद में झूठ का पुलिंदा पेश करने में अपना सारा का सारा नाटकीय कौशल लगा दिया. जो कुछ हुआ था, उस पर पछताने के बजाए उन्होंने रोहिथ के इंसाफ का आंदोलन करने वालों पर आक्रामक हमला किया. रोहिथ की जाति पर सवाल उठा कर इस मामले को भटकाने की घिनौनी कौशिशें की गईं मानो उनका दलितपन उन्हें हाथोहाथ इंसाफ दिला देगा और उनका दलित न होना अपराधियों के अपराध को हल्का कर देगा.
तेलंगाना राज्य की पूरी ताकत-जिसके लिए करीब 600 लोगों ने अपनी जान दे दी थी और उनमें से अनेक दलित थे-मातम में डूबी हुई मां पर टूट पड़ी कि वो अपनी जाति साबित करें. रोहिथ के पास दलित होने का जाति प्रमाणपत्र होने के बावजूद, एक दलित की जिंदगी जीने और मरने के बावजूद, तेलंगाना प्रशासन ने यह अफवाह फैलाई कि वो दलित नहीं, एक वड्डेरा थे. यह साबित करने के लिए परिवार को जगह-जगह दौड़ाया गया कि रोहिथ असल में एक दलित थे. उन्हें अपने बेटे को खो देने के दर्द को परे कर देना पड़ा. किस्मत से सरकार की सारी तरकीबें नाकाम रहीं और रोहिथ का दलित होना साबित हुआ.
जैसी कि उम्मीद थी, अपराधियों पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा. वे सभी ताकत के अपने पदों पर जमे हुए हैं, जबकि इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों को आखिरी हदों तक धकेला जा रहा है. अप्पा राव ने उस दलित वीथि को हटा दिया है, जो रोहिथ और उनके चार निष्कासित साथियों की आखिरी शरण स्थली थी, जिसे उन्होंने शॉपकॉम पर खड़ा किया था. यह जगह मौजूदा आंदोलन का एक प्रतीकात्मक केंद्र थी. वहां लगाई गई आंबेडकर की प्रतिमा भी चुरा ली गई और रोहिथ के अस्थायी स्मारक पर लगाए गए रोहिथ के पोर्ट्रेट को बिगाड़ दिया गया.
गुजरात में गुंडागर्दी
11 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में उना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में एक दलित परिवार, जाति द्वारा नियत अपने पेशे के मुताबिक एक मरी हुई गाय का चमड़ा उतार रहा था, कि गौ रक्षा समिति का भेष धरे शिव सेना का एक समूह उनके पास पहुंचा. उन्होंने गाय की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को पीटा और फिर चार नौजवानों को उठा लिया. उन्होंने उनकी कमर में जंजीर बांध कर उन्हें एक एसयूवी से बांध दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए उना कस्बे तब ले आए, जहां एक पुलिस थाने के करीब उनको कई घंटों तक सबकी नजरों के सामने पीटा गया.
हमलावरों को इस बात को लेकर यकीन था कि उन्हें इस पर कभी भी किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी इस खौफनाक हरकत का वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक भी किया. लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया. इससे भड़क उठे दलित खुद ब खुद सड़कों पर उतर पड़े. हालांकि गुजरात कभी भी दलितों की स्थिति के लिहाज से आदर्श राज्य नहीं रहा था, लेकिन यह दलितों पर ऐसे दिन-दहाड़े अत्याचार का कभी गवाह नहीं रहा था.
राज्य भर में दलितों के भारी विरोध प्रदर्शनों की एक स्वाभाविक लहर दौड़ गई. करीब 30 दलितों ने अपने समुदाय के साथ होने वाली नाइंसाफियों को उजागर करने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की. लेकिन सबसे समझदारी भरी कार्रवाई मवेशियों की लाशों को अनेक जगहों पर कलेक्टर कार्यालयों के सामने डाल देना था. दलितों ने एकजुटता जाहिर करने की एक गैरमामूली कदम उठाते हुए लाशें उठाने और उनका चमड़ा उतारने का अपना परंपरागत काम रोक दिया और इस तरह इनसे होने वाली आमदनी की भी कुर्बानी दी.
28 जुलाई के द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में हर जगह सड़ती हुई लाशें एक महामारी का खतरा बन गई हैं. पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में करीब एक करोड़ गायें और भैंसें हैं जिनके मरने की दर 10 फीसदी है. इसका मतलब ये है कि हर रोज राज्य भर में 2,740 मवेशी मरते हैं. किसी जगह पर ऐसी ही पड़ी एक लाश की बदबू जनता की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और ऐसे में ऊपर दी गई तादाद तो एक तबाही ही ला सकती है.
गौरक्षा संस्थाओं को होश आ गया है और वे यह कबूल करने को मजबूर हुई हैं कि वो इस समस्या के बारे में नहीं जानती थीं और अब वे लाशों का निबटारा करने के तरीके खोजेंगी. अगर देश भर के नहीं तो पूरे राज्य में मैला ढोने के काम में लगे दलितों (सरकारों द्वारा कसम खा कर उनके वजूद को नकारने के बावजूद उनकी तादाद हजारों में है) और इसी तरह पूरे राज्य के सफाई कर्मियों को भी इस विरोध का हिस्सा बन जाना चाहिए.
आम्बेडकर की विरासत चकनाचूर
25 जून की रात में आम्बेडकरियों का भेस धरे सैकड़ों गुंडे दो बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने मुंबई में दादर में स्थित ऐतिहासिक आम्बेडकर भवन और आम्बेडकर प्रेस को गिरा दिया. ऐसा उन्होंने रत्नाकर गायकवाड़ के कहने पर किया, जो एक रिटायर्ड नौकरशाह हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति करवाने में कामयाब रहे हैं. प्रेस का एक ऐतिहासिक मूल्य था, क्योंकि उसका संबंध बाबासाहेब आम्बेडकर से था. उनके अहम अखबारों में से दो जनता और प्रबुद्ध भारत यहीं से छपते और प्रकाशित होते थे और यह 1940 के दशक में आम्बेडकरी आंदोलन का एक केंद्र भी था. उनके निधन के बाद भी यह एक केंद्र बना रहा; भूमि संघर्ष पर आंदोलन, ‘रिडल्स’ विवाद पर आंदोलन और नामांतर संघर्षों की योजना यहीं बनी और उन अमल हुआ.
दूसरी इमारत आम्बेडकर भवन एक एकमंजिला, अंग्रेजी के “यू” अक्षर के उल्टे शक्ल की थी जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था. इन दोनों इमारतों को गिराने के लिए जिस बहाने की ओट ली गई, कि वे ढांचागत रूप से खतरनाक थे, वे जाहिर तौर पर गायकवाड़ द्वारा “गढ़े” गए थे. इस दुस्साहस भरी कार्रवाई से और इससे भी ज्यादा जिस शर्मनाक और उद्दंड तरीके से उसको जायज ठहराया जा रहा था, उससे लोग भौंचक रह गए. जैसा कि इसके पहले और इसके बाद होने वाली घटनाओं ने उजागर किया, गायकवाड़ राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हाथों का मोहरा भर थे.
ट्रस्ट की विवादास्पद स्थिति से वाकिफ मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित 17 मंजिला आम्बेडकर भवन के लिए चोरी-छिपे भूमिपूजन किया (और मजे की बात है कि यह पूजा कहीं और की गई) और इसके लिए 60 करोड़ के अनुदान का ऐलान भी किया. 25 जून को जो कुछ हुआ था, वह खुल्लम-खुल्ला एक आपराधिक करतूत थी, जिसको मजबूरन गायकवाड़ को कबूल करना पड़ा. उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने से बचने के लिए उनकी संवैधानिक हैसियत का एक झूठा बहाने को सामने कर दिया गया.
गायकवाड़ और भाजपा सरकार के अपराधों से नाराजगी के साथ 19 जुलाई को मुंबई में एक भारी मोर्चा निकाला गया. घटनाओं के इस पूरे सिलसिले ने दलितों के भीतर वर्गीय बंटवारे को सबसे बदसूरत तरीके से उजागर किया. जहां उच्च मध्य वर्ग के दलितों ने गायकवाड़ का समर्थन किया, जिसमें प्रवासी दलित (डायस्पोरा) तबका और दलित नौकरशाहों से मिले हराम के पैसों पर आरामतलबी की जिंदगी जीते बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं. दूसरी तरफ दलितों की व्यापक बहुसंख्या ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की और आम्बेडकर परिवार का समर्थन किया जो गायकवाड़ के खिलाफ खड़े थे. बाबासाहेब आम्बेडकर के तीनों पोते आमतौर पर स्वतंत्र रहे हैं और कांग्रेस या भाजपा के साथ सहयोग करने से इन्कार किया है. राजनीतिक रूप से उनका नजरिया अवाम के हक में रहा है और उन्होंने जनसंघर्षों का समर्थन किया है. चाहे जितना भी कमजोर हो, आज वे अकेले आम्बेडकरी प्रतिष्ठान है जो पूरी मजबूती से हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ हैं.
इसलिए भाजपा के लिए उनकी छवि को बदनाम करना जरूरी है. इस काम को पूरा करने के लिए मध्यवर्ग के दलितों के एक हिस्से को चुपचाप उकसाया जा रहा है. धीरे-धीरे उन्होंने यह प्रचार खड़ा किया है कि बाबासाहेब आम्बेडकर के वारिस आम्बेडकरी नहीं बल्कि माओवाद के समर्थक हैं. कम से कम एक दलित अखबार महानायक पिछले पांच बरसों से इस झूठ को पूरे उन्माद के साथ फैलाता आ रहा है. इमारतों को तोड़े जाने के इस पूरे नाटक के जरिए भाजपा का इरादा इसी मकसद को हासिल करने का था. गायकवाड़ ने तीनों पोतों और उनके पिता यशवंतराव आम्बेडकर को गैर कानूनी कब्जा करने वाले नालायक और गुंडा बताया.
आम्बेडकर भवन को गिराना और आम्बेडकर के परिवार की छवि को मिट्टी में मिलाना, गायकवाड़ के ये वो दो जुड़वां काम थे जिनके लिए उन्हें देश भर में भड़कते जनता के गुस्से की अनदेखी करते हुए भाजपा सरकार से समर्थन मिल रहा है. इस खुलेआम आपराधिक मामले में पुलिस और राज्य मशीनरी जिस तरह पेश आती रही है और आ रही है उसी से सरकार का तौर-तरीका साफ हो जाता है.
दलित “हनुमानों” की बेशर्मी
भाजपा अपने तीनों दलित रामों को अपना ‘हनुमान’ बना देने में कामयाब रही है. उन्होंने कुछ तथाकथित दलित बुद्धिजीवियों को भी लालच देते हुए अपनी हां में हां मिलाने के लिए अपनी तरफ खींचा है. गुजरात में दलित नौजवानों को पीटे जाने पर देश भर में भड़क उठे गुस्से के ताप में भी, एक दलित “हनुमान” ऐसा था जो बेशर्मी से यह कहता फिर रहा था कि दलितों पर अत्याचारों से गुजरात का नाम नहीं जोड़ा जाए. जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय अपराध शोध ब्यूरो (एनसीआरबी) के अपराध के आंकड़ों को गलत और संदर्भ से हटा कर पेश किया, उसी से उनकी गुलामी और बौद्धिक बेईमानी जाहिर होती है. एक तरफ जब गैर-दलित पैनलिस्ट गुजरात में भड़के गुस्से को जायज ठहरा रहे थे, यह पिट्ठू बड़े भद्दे तरीके से यह बहस कर रहा था कि जातीय अत्याचारों के मामले में गुजरात अनेक राज्यों से बेहतर है.
तथ्य ये है कि दलितों पर अत्याचारों की घटनाओं के मामले में गुजरात के सिर पर, ऊपर के पांच राज्यों में लगातार बने रहने का एक खास ताज रखा हुआ है. 2013 में जब आने वाले आम चुनावों और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ताजपोशी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का “वाइब्रेट गुजरात” का जाप चरम पर पहुंचा, अनुसूचित जातियों (एससी) की प्रति लाख आबादी पर अत्याचारों की तादाद उसके पहले वाले साल के 25.23 से बढ़ कर 29.21 हो गई. इसके नतीजे में राज्य देश का चौथा सबसे बदतर राज्य बन गया.
पहले गलत तरीका अपनाते हुए एनसीआरबी अत्याचारों की गिनती प्रति लाख आबादी पर करता आ रहा था; सिर्फ 2012 से यह प्रति लाख एससी आबादी के संदर्भ में घटनाओं को जुटा रहा है. इसलिए एनसीआरबी तालिकाओं में दी गई एससी के खिलाफ अपराध की घटनाओं की दरों को सही आंकड़ों में बदलने की जरूरत होगी, लेकिन उनसे भी राज्यों के बीच में गुजरात की तुलनात्मक स्थिति के बदलने की संभावना कम ही है.
हत्या और बलात्कार जैसे बड़े अत्याचारों के मामले में भी गुजरात बदतरीन राज्यों में से है. तालिका एक भारत के बड़े राज्यों में 2012 और 2013 के लिए इन अत्याचारों की दरें मुहैया कराती है, ताकि दिखाया जा सके कि कैसे दलितों के खिलाफ अपराधों के लिए गुजरात का नाम ऊपर के राज्यों में आता है.
मौर्या जी, आप चले तो गए, करेंगे क्या?
 मौर्या जी, सबसे पहले तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका अभिवादन ‘जय भीम’ से करूं या फिर ‘कुछ और’ कहूं. खैर पाला आपने बदला है, हमारी विचारधारा आज भी वहीं है सो आपको जय भीम. कुछ महीने पहले ही आपसे रायबरेली में मुलाकात हुई थी. आप और मैं दोनों उस कार्यक्रम के अतिथि थे. आपने शानदार बोला था. यहां तक कि बाकी सभी ने आपको सुनने के लिए अपना भाषण संक्षिप्त ही रखा था. आप खूब गरजे थे. फिर से वही गोबर और गणेश की बात सुना डाली थी, जिसको लेकर आप विवादों में भी रहे थे और जिस कारण बहुजन समाज आपका मान-सम्मान करता रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने खूब ताली पीटी थी. बस यह जानकर थोड़ा झटका लगा है कि आप जैसा विचारधारा में जिंदा रहने वाला आदमी एक ऐसी पार्टी में क्यों चला गया, जिससे अम्बेडकरवाद का सबसे ज्यादा संघर्ष है.
आप से जब बाबासाहेब की 125वीं जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को लखनऊ में मुलाकात हुई थी तो यह तो समझ में आ गया था कि आप पार्टी से नाराज हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतना नाराज हैं. आपने जब पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो भी तमाम लोग कहते रहे कि आप भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहता रहा कि स्वामी जी भाजपा में नहीं जाएंगे. लेकिन जब आप भाजपा में चले गए हैं तो सोचता हूं कि अच्छा होता कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया होता या फिर किसी अन्य पार्टी में चले गए होते. खैर, जब आपने ‘भगवा’ ओढ़ ही लिया है तो ये बताइए कि अब आप करेंगे क्या? क्या आप अठावले की तरह ‘बहन जी’ को भला-बुरा कहेंगे (जिसकी शुरुआत आप कर ही चुके हैं). जिस ‘गणेश’ को कल तक आप ‘गोबर गणेश’ कह कर हिन्दूवादी व्यवस्था का मजाक उड़ाते थे, क्या अब उसी के सामने माथा टेकेंगे या फिर अनुप्रिया पटेल की तरह आरक्षण की समीक्षा की मांग उठाएंगे? जाहिर है आप सब करेंगे.
अच्छा एक बात बताइए, यह सब कर के आपको अगर कुछ लाभ भी हासिल हो जाएगा तो क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? तो क्या बहुजन समाज यह माने कि आज तक आप बाबासाहेब और मान्यवर की बात झूठ कहते आए हैं? सिर्फ अपने फायदे और पद के लिए. खैर बहुजन समाज ने ऐसे कई झटके पहले भी खाए हैं, उसे अब तो आदत सी हो गई है. उसे अब संभलना भी आ गया है. लेकिन मैं सोचता हूं कि आप जहां गए हैं, यूपी चुनाव के बाद अगर उसने आपको दुत्कार दिया तो आप क्या करेंगे?
मौर्या जी, सबसे पहले तो यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका अभिवादन ‘जय भीम’ से करूं या फिर ‘कुछ और’ कहूं. खैर पाला आपने बदला है, हमारी विचारधारा आज भी वहीं है सो आपको जय भीम. कुछ महीने पहले ही आपसे रायबरेली में मुलाकात हुई थी. आप और मैं दोनों उस कार्यक्रम के अतिथि थे. आपने शानदार बोला था. यहां तक कि बाकी सभी ने आपको सुनने के लिए अपना भाषण संक्षिप्त ही रखा था. आप खूब गरजे थे. फिर से वही गोबर और गणेश की बात सुना डाली थी, जिसको लेकर आप विवादों में भी रहे थे और जिस कारण बहुजन समाज आपका मान-सम्मान करता रहा है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने खूब ताली पीटी थी. बस यह जानकर थोड़ा झटका लगा है कि आप जैसा विचारधारा में जिंदा रहने वाला आदमी एक ऐसी पार्टी में क्यों चला गया, जिससे अम्बेडकरवाद का सबसे ज्यादा संघर्ष है.
आप से जब बाबासाहेब की 125वीं जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को लखनऊ में मुलाकात हुई थी तो यह तो समझ में आ गया था कि आप पार्टी से नाराज हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इतना नाराज हैं. आपने जब पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो भी तमाम लोग कहते रहे कि आप भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहता रहा कि स्वामी जी भाजपा में नहीं जाएंगे. लेकिन जब आप भाजपा में चले गए हैं तो सोचता हूं कि अच्छा होता कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया होता या फिर किसी अन्य पार्टी में चले गए होते. खैर, जब आपने ‘भगवा’ ओढ़ ही लिया है तो ये बताइए कि अब आप करेंगे क्या? क्या आप अठावले की तरह ‘बहन जी’ को भला-बुरा कहेंगे (जिसकी शुरुआत आप कर ही चुके हैं). जिस ‘गणेश’ को कल तक आप ‘गोबर गणेश’ कह कर हिन्दूवादी व्यवस्था का मजाक उड़ाते थे, क्या अब उसी के सामने माथा टेकेंगे या फिर अनुप्रिया पटेल की तरह आरक्षण की समीक्षा की मांग उठाएंगे? जाहिर है आप सब करेंगे.
अच्छा एक बात बताइए, यह सब कर के आपको अगर कुछ लाभ भी हासिल हो जाएगा तो क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? तो क्या बहुजन समाज यह माने कि आज तक आप बाबासाहेब और मान्यवर की बात झूठ कहते आए हैं? सिर्फ अपने फायदे और पद के लिए. खैर बहुजन समाज ने ऐसे कई झटके पहले भी खाए हैं, उसे अब तो आदत सी हो गई है. उसे अब संभलना भी आ गया है. लेकिन मैं सोचता हूं कि आप जहां गए हैं, यूपी चुनाव के बाद अगर उसने आपको दुत्कार दिया तो आप क्या करेंगे? आनंदी बेन का जाना: गुजरात में दलित-अल्पसंख्यक आन्दोलन को दबाने की एक कवायद
 हम प्रतिवर्ष समूचे राष्ट्र को उद्वेलित कर देने वाले “स्वतंत्रता दिवस” समारोह धूमधाम से मनाते हैं. इस अवसर पर भारत छोड़ो आन्दोलन का याद आना स्वाभाविक ही है. भारत छोड़ो आन्दोलन का वह समय था जब हमारे लक्ष्यों और आदर्शों की निष्ठा ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दिया था. उस आन्दोलन के न तो जातियाँ ही आड़े आईं और न ही धर्म. फिर आजादी प्राप्त होने के बाद क्या हो गया कि सामाजिक न्याय के सूत्रधार जाति-भेद की विषमता मिटाने के नाम पर व धार्मिक ठेकेदार धर्म के नाम पर जातिगत एवं धार्मिक विद्वेष और राजनैतिक मोर्चोंबन्दी को पुख्ता कर रहे हैं. आदमी को आदमी से दूर करने लगे हैं. आजादी प्राप्ति से पूर्व के जो राष्ट्रीय लक्ष्य एवं मूल्य, जो आदर्श भारतीयों को सामूहिक रूप से स्फुरित करते थे, जैसे बिखर गए हैं. आत्मनिर्भरता के सुस्वप्न में देखा राष्ट्रीय स्वाभिमान जैसे आज विलुप्त हो गया है. हमारी राजनीति का तो लगता है, शील ही भंग हो गया है. आस्थाएं डगमगा रही हैं. सामाजिक न्याय का लक्ष्य मात्र भाषणों या फिर कागजों में सिमटकर रह गया है. आजादी प्राप्ति के बाद की राजनीति ने अवसरवादिता एवं शून्यवाद को ही जन्म दिया है. नीति और नीयत दोनों ही गुड़-गोबर हो गई हैं. मूल्यों के बिखराव के वर्तमान दौर में सभी राजनैतिक पार्टियां उठापटक में लगी हैं. “आओ! सरकार सरकार खेलें” के खेल में लिप्त हैं. भारतीयता जैसे नैपथ्य में चली गई है. धर्मांधता, जातीयता, धन-लोलुपता और विलासता राजनैतिक मंच पर निर्वसन थिरक रही है. राजनैतिक नारे दिशाहीनता ही पैदा कर रहे हैं. सरकारी स्तर से ग्रामीणों हेतु शिक्षा की आड़ में विदेशियों को पुन: भारत आने का न्यौता दिया गया. सरकार ने बेशक इसे आर्थिक सुधार की मुहिम कहा था, किंतु ये था तो परतंत्रता का ही द्योतक. भारत जैसे स्वाभिमानी और विकासशील राष्ट्र के लिए यह गर्वित होने की बात नहीं है. भारत की आम-जनता के लिए यह हानिकारक ही सिद्ध होगी. समाज में हिंसा और भ्रष्टाचार निरंतर निर्बाध गति से बढ़ता जा रहा है. लोगों की मानसिकता हिंसक होती जा रही है. ऐसे में बेहतर प्रशासन की उम्मीद रखना मिथ्या विचार ही होगा.
यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार संत्री से लेकर मंत्री तक अपनी पहुँच बना चुका है. सुनने को मिलता है कि आजादी प्राप्त होने से पहले देश में केवल पाँच प्रतिशत काला धन था जबकि आज देश में 80 प्रतिशत से भी अधिक काला धन है. यह निरंतर सिकुड़ती और कलुषित मानसिकता का ही परिणाम है. भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कभी कोई भूखा शायद ही रोटी की चोरी करता होगा, किंतु आज अमीर और अमीर बनने के लिए चोरी करता है. सरकारी सौदों में पनपता भ्रष्टाचार करोड़ों-अरबों से कम नहीं होता. ऐसे तमाम घोटालों के पीछे किन-किन ताकतों का हाथ होता है, किसको नहीं पता? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर कोई क्या कर सकता है? हाँ! अगर जनता ही एकजुट हो जाए तो कुछ बात बन सकती है.
इन्दिरा गान्धी का “गरीबी हटाओ” नारा, राजीव गान्धी का 21वीं सदी में प्रवेश करने का नारा, सत्ता में आई प्रत्येक राजनैतिक पार्टी, सत्ता में आने के बाद के 100 दिनों में मंहगाई कम करने का वायदा बड़े जोर-शोर से करती है किंतु मंहगाई है कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है. तमाम के तमाम राजनैतिक वायदे आम-जनता की आँख में धूल झोंकने का काम करते हैं. मोदी जी का “सबका साथ, सबका विकास” नारा एक जुमला ही सिद्ध हुआ है. 100 दिन में काले धन की वापसी के वादे को भाजपा के अध्यक्ष “एक राजनीतिक जुमला” सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी कर चुके हैं. राजनैतिक मंचों से धार्मिक-घोष ने राजनीति में और कालिख घोल दी है. मनुवादी प्रयोगशाला में फला-फूला भारतीय समाज आज भी पूरी तरह साम्प्रदायिकता के चंगुल में फँसा हुआ है. साम्प्रदायिकता को लेकर जिस प्रकार की समस्या भारत देश में है, शायद ही किसी अन्य देश में हो. यह भी सत्य है कि विविधताओं और विभिन्नताओं से भरा भारत जैसा कोई दूसरा देश हो. जाति-दर-जाति से निर्मित हमारे सामजिक ढाँचे को देखकर सब दाँतों तले उँगलियाँ दबाते हैं. जाति-प्रथा का सम्पूर्ण ढाँचा ही सामाजिक दृष्टि से ऊँच-नीच की मानसिकता पर आधारित है. वर्तमान में गौ-रक्षा के नाम पर हो रहे जातीय दंगे, मारपीट, और दलित जातियों की महिलाओं के साथ हो रहे निरंतर बलात्कार, सरकारी और सामाजिक स्तर पर अल्पसंख्यकों और दलितों के हितों की अनदेखी कोई नई बात नहीं किंतु वर्तमान सरकार के समय में तो अति ही हो गई है. भाजपा और भाजपा की पैत्रिक संस्था को लगता है कि शायद यह उनकी अंतिम सरकार होगी तभी तो वह अपने तमाम एजेंडों को इसी काल में पूरा करने के फिराक में धार्मिक और जातीय दंगे भड़काने के काम जुटी है. सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाकर सत्ता में बने रहना उनका एक मात्र मकसद बनकर रह गया है.
व्यापक स्तर पर जाति या मजहब आधारित सांप्रदायिक झगड़े भारत में बेशक नए लगते हों किंतु इसके मूल में जो घृणा-भाव काम करता है, वह नया नहीं है. अंग्रेजों के आने तक शायद यें बातें भारतीयों को ज्यादा परेशान न करती हों. विभिन्न जातियों के लोग कभी-कभार आपस में थोड़ी-बहुत गाली-गलौज अथवा सिर-फुट्टवल तो कर लेते थे, किंतु इस प्रकार के द्वेष को देर तक न ढोते थे. आज जो भी सांप्रदायिक झगड़े भारत में हो रहे हैं, वे सब राजनीति की देन हैं. आश्चर्यजनक तो यह है कि जाति-प्रथा के पोषक ही आज जाति-पाँति के उभरने की बात करने लगे हैं. उनसे कोई तो पूछे कि भारत में जाति-पाँति का वर्चस्व कब नहीं था. अंतर केवल इतना है कि पहले का दलित लुट-पिटकर भी चुप रहने को बाध्य था, पर आज का दलित में जातीय चेतना जाग उठी है. वह सामाजिक न्याय और सम्मान पाने की बात पर उतारू है. हालिया हिंसक वारदातों पर प्रधान मंत्री की चुप्पी न केवल प्रधान मंत्री पद की गरिमा पर प्रहार है अपितु उनके गुप्त एजेंडे का खुलासा भी कर रही है. लगता है कि मोदी जी ने असामाजिक तत्वों को दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को कुचलने की खुली छूट दे रखी है.
गौरतलब है कि साम्प्रदायिक घृणा देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है. पंजाब में सिख साम्प्रदायिकता, असम में बोडो समस्या, कश्मीर में मुस्लिम साम्प्रदायिकता, अब गाय के नाम पर तथाकथित गौ-रक्षकों का तांडव ..तो कहीं कोई और समस्या, यह है आज के भारत में साम्प्रदायिकता का विकराल रूप. इन सबको पीछे छोड़ती हुई, एक और बड़ी समस्या है, साम्प्रदायिक ताकतों के सिर पर चढ़ा “हिन्दू-राष्ट्र” की स्थापना का भूत. पहले से ही जातियों में विभाजित जनता को किसी न किसी मुद्दे पर और बाँटना, विभिन्न वर्गों में मतभेदों को मनभेद में बदलना और उसे बढ़ावा देना सत्ता-लाभ प्राप्त करना ही आज की राजनीति की नियति बन गई है.
नवभारत टाइम्स (24.07.2016) में राजनीतिक एक्सपर्ट नीरजा चौधरी कहती है कि राजनीति में ह्युमर कम होता जा रहा है क्योंकि इसकी जगह राजनीतिक कटुता ने ले ली है. जहाँ कटुता होती है वहाँ ह्युमर नहीं रहता. जब सब अपने आप को सीरियसली लेने लगते हैं, तब भी ह्युमर दूर भागता है. पहले लोगों के विचारों में मतभेद होता था लेकिन हंसी-खुशी का माहौल बना रहता था. राजनेता एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते थे, एक-दूसरे का विरोध भी किया करते थे लेकिन माहौल में मधुरता होती थी. अब सोच का दायरा बेहद संकीर्ण हो गया है, जिसमें ह्युमर की जगह ही नहीं बची है. जाहिर है कि अब मतभेद से ज्यादा मनभेद होता है. ….जब दिल ही नहीं मिल रहे तो ह्युमर कैसा? सबसे प्रमुख दो दलों के शीर्ष नेताओं तक में बातचीत नहीं होती…सब एक संकुचित दायरे में सोचने लगे हैं. अब सरकार और विपक्षी दलों के बीच के संबंध सामान्य हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं लगता. खेद की बात है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने ऐसे खड़े नजर आते हैं…. जैसे दो देशों की सैनाएं जबकि रिश्तों को सामान्य बनाना सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों पर ही निर्भर करता है. लेकिन ज्यादा.सत्ता पक्ष पर क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसा करने की स्थिति में होता है. यहाँ इस सवाल का उठना लाजिम है कि राजनेताओं के बीच रोजाना होने वाली गाली-गलौज से क्या लोकतंत्र की मर्यादा को आहत नहीं हो रही है?
यहाँ यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज की केन्द्र सरकार बैसाखियों के सहारे नहीं टिकी है, बल्कि पूरे बहुमत से सता में है. जिससे सरकार का रवैया एक तानाशाह जैसा दिख रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार की शह पर ही देश में कमजोर वर्गों को किसी न किसी मुद्दे पर निशाना बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री की इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखना, इस बात का प्रमाण है. अभी हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री को महज इसलिए हटाया गया कि वो गुजरात में तारी दंगों/फसादातों को सुलझाने में नहीं, बल्कि दबाने में ना कामयाब रहीं. कहना ये है कि वर्तमान सरकार चाहे तो पटेल आन्दोलन हो, या फिर गुजरात में ही तथाकथित गौ-रक्षकों द्वारा चर्मकार दलितों पर अमानवीय मारपीट का मामला हो, या हरियाणा में दलित किशोरियों के साथ हुए दोहरे बलात्कार का मामला हो, या फिर उत्तर प्रदेश में इखलाख का मामला हो, या फिर मुम्बई में बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को तहस-नहस करना हो. ….आज की केन्द्र सरकार इन मामलों को सुलझाने के बजाय इन मामलों को दबाने का प्रयास करती रही है, किंतु ऐसा कर नहीं पाई. परिणाम स्वरूप अब बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपना शिकार बनाया है. हो सकता है कि कल हरियाणा के मुख्य मंत्री की बारी आ जाए…उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटा दिया जाए कि वो जाट आन्दोलन को दबाने में असफल रहे. बारी राजस्थान की भी आ सकती है. अखबारों की छपी टिप्पणियों तो यह ही स्पष्ट हो रहा कि गुजरात की मुख्य मंत्री आनंदी बेन का जाना गुजरात में दलित आन्दोलन को दबाने की एक साजिश है. बीजेपी का मानना है कि गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री में दलित और पटेल आन्दोलन की क्षमता है.
चलते-चलते…. आनन्दी बेन के त्यागपत्रके एक दिन बाद ही गौ-रक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को केन्द्र में रखकर प्रधानमंत्री के बयान का आना क्या कोई सवाल खड़ा नहीं करता? इससे यह कतई स्पष्ट होता है कि अब प्रधानमंत्री ने भी देशभर में तेजी से पनप रहे गौरक्षा के नाम पर दलित और मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ चल रहे दलित और मुस्लिम आन्दोलन को दबाने का ही प्रयास है. पता नहीं कि जब प्रधान मंत्री को इतना पता है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है और तथाकथिक गौरक्षकों में लगभग 80 प्रतिशत असामाजिक तत्व शामिल है और अपनी-अपनी दुकानदारी को चमका रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौररक्षकों के खिलाफ इतनी देर बाद छह जुलाई को पहली बार मुंह खोला. माना तो ये जा रहा है कि मोदी जी ने संघ और बीजेपी शासित राज्यों पर अप्रत्यक्ष रुप से निशाना साधा है किंतु ऐसा लगता नहीं है. उनका ये बयान अगामी वर्ष में कई राज्यों होने वाले चुनावों के मद्देनजर दलितों और अल्पसंख्यकों में उपजे आक्रोश को कुछ ठंडा करने की एक राजनीतिक कवायद है. लेकिन उनका ये मकसद किस सीमा तक पूरा होगा यह एक प्रश्नचिन्ह ही है. हार्दिक पटेल ने तो ऐलान कर दिया है कि इस कवायद से पटेल आन्दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका आन्दोलन और तेजी से चलेगा. दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी इस छलावे में नहीं आना चाहिए और अपने आन्दोलन पर अडिग रहना चाहिए अन्यथा उनकी आगामी पीढ़ियां उन्हें सदियों तक माफ नहीं करेंगी.
लेखक तेजपाल सिंह तेज (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार की कई किताबें प्रकाशित हैं- दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, तूफाँ की ज़द में ( गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन-झुन, खेल-खेल में आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली ( शब्द चित्र), दो निबन्ध संग्रह और अन्य. तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक और चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक रहे हैं. स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर इन दिनों अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक का संपादन कर रहे हैं. हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार ( 1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से सम्मानित.
हम प्रतिवर्ष समूचे राष्ट्र को उद्वेलित कर देने वाले “स्वतंत्रता दिवस” समारोह धूमधाम से मनाते हैं. इस अवसर पर भारत छोड़ो आन्दोलन का याद आना स्वाभाविक ही है. भारत छोड़ो आन्दोलन का वह समय था जब हमारे लक्ष्यों और आदर्शों की निष्ठा ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दिया था. उस आन्दोलन के न तो जातियाँ ही आड़े आईं और न ही धर्म. फिर आजादी प्राप्त होने के बाद क्या हो गया कि सामाजिक न्याय के सूत्रधार जाति-भेद की विषमता मिटाने के नाम पर व धार्मिक ठेकेदार धर्म के नाम पर जातिगत एवं धार्मिक विद्वेष और राजनैतिक मोर्चोंबन्दी को पुख्ता कर रहे हैं. आदमी को आदमी से दूर करने लगे हैं. आजादी प्राप्ति से पूर्व के जो राष्ट्रीय लक्ष्य एवं मूल्य, जो आदर्श भारतीयों को सामूहिक रूप से स्फुरित करते थे, जैसे बिखर गए हैं. आत्मनिर्भरता के सुस्वप्न में देखा राष्ट्रीय स्वाभिमान जैसे आज विलुप्त हो गया है. हमारी राजनीति का तो लगता है, शील ही भंग हो गया है. आस्थाएं डगमगा रही हैं. सामाजिक न्याय का लक्ष्य मात्र भाषणों या फिर कागजों में सिमटकर रह गया है. आजादी प्राप्ति के बाद की राजनीति ने अवसरवादिता एवं शून्यवाद को ही जन्म दिया है. नीति और नीयत दोनों ही गुड़-गोबर हो गई हैं. मूल्यों के बिखराव के वर्तमान दौर में सभी राजनैतिक पार्टियां उठापटक में लगी हैं. “आओ! सरकार सरकार खेलें” के खेल में लिप्त हैं. भारतीयता जैसे नैपथ्य में चली गई है. धर्मांधता, जातीयता, धन-लोलुपता और विलासता राजनैतिक मंच पर निर्वसन थिरक रही है. राजनैतिक नारे दिशाहीनता ही पैदा कर रहे हैं. सरकारी स्तर से ग्रामीणों हेतु शिक्षा की आड़ में विदेशियों को पुन: भारत आने का न्यौता दिया गया. सरकार ने बेशक इसे आर्थिक सुधार की मुहिम कहा था, किंतु ये था तो परतंत्रता का ही द्योतक. भारत जैसे स्वाभिमानी और विकासशील राष्ट्र के लिए यह गर्वित होने की बात नहीं है. भारत की आम-जनता के लिए यह हानिकारक ही सिद्ध होगी. समाज में हिंसा और भ्रष्टाचार निरंतर निर्बाध गति से बढ़ता जा रहा है. लोगों की मानसिकता हिंसक होती जा रही है. ऐसे में बेहतर प्रशासन की उम्मीद रखना मिथ्या विचार ही होगा.
यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार संत्री से लेकर मंत्री तक अपनी पहुँच बना चुका है. सुनने को मिलता है कि आजादी प्राप्त होने से पहले देश में केवल पाँच प्रतिशत काला धन था जबकि आज देश में 80 प्रतिशत से भी अधिक काला धन है. यह निरंतर सिकुड़ती और कलुषित मानसिकता का ही परिणाम है. भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कभी कोई भूखा शायद ही रोटी की चोरी करता होगा, किंतु आज अमीर और अमीर बनने के लिए चोरी करता है. सरकारी सौदों में पनपता भ्रष्टाचार करोड़ों-अरबों से कम नहीं होता. ऐसे तमाम घोटालों के पीछे किन-किन ताकतों का हाथ होता है, किसको नहीं पता? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर कोई क्या कर सकता है? हाँ! अगर जनता ही एकजुट हो जाए तो कुछ बात बन सकती है.
इन्दिरा गान्धी का “गरीबी हटाओ” नारा, राजीव गान्धी का 21वीं सदी में प्रवेश करने का नारा, सत्ता में आई प्रत्येक राजनैतिक पार्टी, सत्ता में आने के बाद के 100 दिनों में मंहगाई कम करने का वायदा बड़े जोर-शोर से करती है किंतु मंहगाई है कि निरंतर बढ़ती ही जा रही है. तमाम के तमाम राजनैतिक वायदे आम-जनता की आँख में धूल झोंकने का काम करते हैं. मोदी जी का “सबका साथ, सबका विकास” नारा एक जुमला ही सिद्ध हुआ है. 100 दिन में काले धन की वापसी के वादे को भाजपा के अध्यक्ष “एक राजनीतिक जुमला” सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी कर चुके हैं. राजनैतिक मंचों से धार्मिक-घोष ने राजनीति में और कालिख घोल दी है. मनुवादी प्रयोगशाला में फला-फूला भारतीय समाज आज भी पूरी तरह साम्प्रदायिकता के चंगुल में फँसा हुआ है. साम्प्रदायिकता को लेकर जिस प्रकार की समस्या भारत देश में है, शायद ही किसी अन्य देश में हो. यह भी सत्य है कि विविधताओं और विभिन्नताओं से भरा भारत जैसा कोई दूसरा देश हो. जाति-दर-जाति से निर्मित हमारे सामजिक ढाँचे को देखकर सब दाँतों तले उँगलियाँ दबाते हैं. जाति-प्रथा का सम्पूर्ण ढाँचा ही सामाजिक दृष्टि से ऊँच-नीच की मानसिकता पर आधारित है. वर्तमान में गौ-रक्षा के नाम पर हो रहे जातीय दंगे, मारपीट, और दलित जातियों की महिलाओं के साथ हो रहे निरंतर बलात्कार, सरकारी और सामाजिक स्तर पर अल्पसंख्यकों और दलितों के हितों की अनदेखी कोई नई बात नहीं किंतु वर्तमान सरकार के समय में तो अति ही हो गई है. भाजपा और भाजपा की पैत्रिक संस्था को लगता है कि शायद यह उनकी अंतिम सरकार होगी तभी तो वह अपने तमाम एजेंडों को इसी काल में पूरा करने के फिराक में धार्मिक और जातीय दंगे भड़काने के काम जुटी है. सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाकर सत्ता में बने रहना उनका एक मात्र मकसद बनकर रह गया है.
व्यापक स्तर पर जाति या मजहब आधारित सांप्रदायिक झगड़े भारत में बेशक नए लगते हों किंतु इसके मूल में जो घृणा-भाव काम करता है, वह नया नहीं है. अंग्रेजों के आने तक शायद यें बातें भारतीयों को ज्यादा परेशान न करती हों. विभिन्न जातियों के लोग कभी-कभार आपस में थोड़ी-बहुत गाली-गलौज अथवा सिर-फुट्टवल तो कर लेते थे, किंतु इस प्रकार के द्वेष को देर तक न ढोते थे. आज जो भी सांप्रदायिक झगड़े भारत में हो रहे हैं, वे सब राजनीति की देन हैं. आश्चर्यजनक तो यह है कि जाति-प्रथा के पोषक ही आज जाति-पाँति के उभरने की बात करने लगे हैं. उनसे कोई तो पूछे कि भारत में जाति-पाँति का वर्चस्व कब नहीं था. अंतर केवल इतना है कि पहले का दलित लुट-पिटकर भी चुप रहने को बाध्य था, पर आज का दलित में जातीय चेतना जाग उठी है. वह सामाजिक न्याय और सम्मान पाने की बात पर उतारू है. हालिया हिंसक वारदातों पर प्रधान मंत्री की चुप्पी न केवल प्रधान मंत्री पद की गरिमा पर प्रहार है अपितु उनके गुप्त एजेंडे का खुलासा भी कर रही है. लगता है कि मोदी जी ने असामाजिक तत्वों को दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज को कुचलने की खुली छूट दे रखी है.
गौरतलब है कि साम्प्रदायिक घृणा देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है. पंजाब में सिख साम्प्रदायिकता, असम में बोडो समस्या, कश्मीर में मुस्लिम साम्प्रदायिकता, अब गाय के नाम पर तथाकथित गौ-रक्षकों का तांडव ..तो कहीं कोई और समस्या, यह है आज के भारत में साम्प्रदायिकता का विकराल रूप. इन सबको पीछे छोड़ती हुई, एक और बड़ी समस्या है, साम्प्रदायिक ताकतों के सिर पर चढ़ा “हिन्दू-राष्ट्र” की स्थापना का भूत. पहले से ही जातियों में विभाजित जनता को किसी न किसी मुद्दे पर और बाँटना, विभिन्न वर्गों में मतभेदों को मनभेद में बदलना और उसे बढ़ावा देना सत्ता-लाभ प्राप्त करना ही आज की राजनीति की नियति बन गई है.
नवभारत टाइम्स (24.07.2016) में राजनीतिक एक्सपर्ट नीरजा चौधरी कहती है कि राजनीति में ह्युमर कम होता जा रहा है क्योंकि इसकी जगह राजनीतिक कटुता ने ले ली है. जहाँ कटुता होती है वहाँ ह्युमर नहीं रहता. जब सब अपने आप को सीरियसली लेने लगते हैं, तब भी ह्युमर दूर भागता है. पहले लोगों के विचारों में मतभेद होता था लेकिन हंसी-खुशी का माहौल बना रहता था. राजनेता एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते थे, एक-दूसरे का विरोध भी किया करते थे लेकिन माहौल में मधुरता होती थी. अब सोच का दायरा बेहद संकीर्ण हो गया है, जिसमें ह्युमर की जगह ही नहीं बची है. जाहिर है कि अब मतभेद से ज्यादा मनभेद होता है. ….जब दिल ही नहीं मिल रहे तो ह्युमर कैसा? सबसे प्रमुख दो दलों के शीर्ष नेताओं तक में बातचीत नहीं होती…सब एक संकुचित दायरे में सोचने लगे हैं. अब सरकार और विपक्षी दलों के बीच के संबंध सामान्य हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं लगता. खेद की बात है कि सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने ऐसे खड़े नजर आते हैं…. जैसे दो देशों की सैनाएं जबकि रिश्तों को सामान्य बनाना सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों पर ही निर्भर करता है. लेकिन ज्यादा.सत्ता पक्ष पर क्योंकि सत्ता पक्ष ऐसा करने की स्थिति में होता है. यहाँ इस सवाल का उठना लाजिम है कि राजनेताओं के बीच रोजाना होने वाली गाली-गलौज से क्या लोकतंत्र की मर्यादा को आहत नहीं हो रही है?
यहाँ यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज की केन्द्र सरकार बैसाखियों के सहारे नहीं टिकी है, बल्कि पूरे बहुमत से सता में है. जिससे सरकार का रवैया एक तानाशाह जैसा दिख रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार की शह पर ही देश में कमजोर वर्गों को किसी न किसी मुद्दे पर निशाना बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री की इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रखना, इस बात का प्रमाण है. अभी हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री को महज इसलिए हटाया गया कि वो गुजरात में तारी दंगों/फसादातों को सुलझाने में नहीं, बल्कि दबाने में ना कामयाब रहीं. कहना ये है कि वर्तमान सरकार चाहे तो पटेल आन्दोलन हो, या फिर गुजरात में ही तथाकथित गौ-रक्षकों द्वारा चर्मकार दलितों पर अमानवीय मारपीट का मामला हो, या हरियाणा में दलित किशोरियों के साथ हुए दोहरे बलात्कार का मामला हो, या फिर उत्तर प्रदेश में इखलाख का मामला हो, या फिर मुम्बई में बाबा साहेब अम्बेडकर भवन को तहस-नहस करना हो. ….आज की केन्द्र सरकार इन मामलों को सुलझाने के बजाय इन मामलों को दबाने का प्रयास करती रही है, किंतु ऐसा कर नहीं पाई. परिणाम स्वरूप अब बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपना शिकार बनाया है. हो सकता है कि कल हरियाणा के मुख्य मंत्री की बारी आ जाए…उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटा दिया जाए कि वो जाट आन्दोलन को दबाने में असफल रहे. बारी राजस्थान की भी आ सकती है. अखबारों की छपी टिप्पणियों तो यह ही स्पष्ट हो रहा कि गुजरात की मुख्य मंत्री आनंदी बेन का जाना गुजरात में दलित आन्दोलन को दबाने की एक साजिश है. बीजेपी का मानना है कि गुजरात के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री में दलित और पटेल आन्दोलन की क्षमता है.
चलते-चलते…. आनन्दी बेन के त्यागपत्रके एक दिन बाद ही गौ-रक्षा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी को केन्द्र में रखकर प्रधानमंत्री के बयान का आना क्या कोई सवाल खड़ा नहीं करता? इससे यह कतई स्पष्ट होता है कि अब प्रधानमंत्री ने भी देशभर में तेजी से पनप रहे गौरक्षा के नाम पर दलित और मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ चल रहे दलित और मुस्लिम आन्दोलन को दबाने का ही प्रयास है. पता नहीं कि जब प्रधान मंत्री को इतना पता है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है और तथाकथिक गौरक्षकों में लगभग 80 प्रतिशत असामाजिक तत्व शामिल है और अपनी-अपनी दुकानदारी को चमका रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौररक्षकों के खिलाफ इतनी देर बाद छह जुलाई को पहली बार मुंह खोला. माना तो ये जा रहा है कि मोदी जी ने संघ और बीजेपी शासित राज्यों पर अप्रत्यक्ष रुप से निशाना साधा है किंतु ऐसा लगता नहीं है. उनका ये बयान अगामी वर्ष में कई राज्यों होने वाले चुनावों के मद्देनजर दलितों और अल्पसंख्यकों में उपजे आक्रोश को कुछ ठंडा करने की एक राजनीतिक कवायद है. लेकिन उनका ये मकसद किस सीमा तक पूरा होगा यह एक प्रश्नचिन्ह ही है. हार्दिक पटेल ने तो ऐलान कर दिया है कि इस कवायद से पटेल आन्दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका आन्दोलन और तेजी से चलेगा. दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी इस छलावे में नहीं आना चाहिए और अपने आन्दोलन पर अडिग रहना चाहिए अन्यथा उनकी आगामी पीढ़ियां उन्हें सदियों तक माफ नहीं करेंगी.
लेखक तेजपाल सिंह तेज (जन्म 1949) की गजल, कविता, और विचार की कई किताबें प्रकाशित हैं- दृष्टिकोण, ट्रैफिक जाम है, गुजरा हूँ जिधर से, तूफाँ की ज़द में ( गजल संग्रह), बेताल दृष्टि, पुश्तैनी पीड़ा आदि (कविता संग्रह), रुन-झुन, खेल-खेल में आदि ( बालगीत), कहाँ गई वो दिल्ली वाली ( शब्द चित्र), दो निबन्ध संग्रह और अन्य. तेजपाल सिंह साप्ताहिक पत्र ग्रीन सत्ता के साहित्य संपादक और चर्चित पत्रिका अपेक्षा के उपसंपादक रहे हैं. स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर इन दिनों अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक का संपादन कर रहे हैं. हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार ( 1995-96) तथा साहित्यकार सम्मान (2006-2007) से सम्मानित. हिन्दू धर्म ग्रंथ और महिला सम्मान का प्रश्न
 प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक एक उपमा जो स्त्रियों के लिए हमेशा दी जाती है, वह है कि सीता-सावित्री की तरह बनो. इस उपमा में सीता या सावित्री के व्यक्तित्व की ऊंचाईयों और गहराईयों को समझने की बात नहीं होती. यहां तो यह इसलिए कहा जाता है कि उनकी नजर में सीता और सावित्री अपने कुल के आदर्शों को ढोने वाली और अपने पति का अनुसरण करने वाली स्त्रियां थीं. हिन्दू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि शुरू से ही स्त्रियों के साथ छल होता आया है.
जब भी कभी कोई निर्णायक मोड़ आया तो सजा स्त्रियों को ही मिली. जिस प्रचलित कहानी के पात्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा बताया जाता है; उस भारत की माता यानी शकुंतला से राजा दुष्यंत ने प्रेम किया और गंधर्व विवाह भी किया. लेकिन अपने राज्य जाकर उन्हें भूल गए. जब शकुंतला उनके पास अपना हक मांगने पहुंची तो वह एक अंगूठी, जिसे दुष्यंत ने शकुंतला को निशानी के तौर पर दी थी के ना होने पर उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया. यह कैसा प्रेम था कि सिर्फ एक अंगूठी के ना होने पर राजा दुष्यंत ने अपनी प्रेमिका/पत्नी को पहचाना तक नहीं.
इसी प्रकार हिन्दू धर्मग्रंथों में प्रचलित कहानी के मुताबिक इंद्र ने जब छल से अहिल्या के साथ संबंध स्थापित किया तो अहिल्या के ऋषि पति ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया,. जबकि इंद्र को मिली सजा कुछ ही दिनों में माफ हो गई. क्या ये पुरूष-स्त्री के बीच का पक्षपात नहीं था? अहिल्या के साथ छल इंद्र ने किया था लेकिन सजा सिर्फ अहिल्या को क्यों? क्योंकि वह एक स्त्री थी? सीता जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहीं, उनके साथ वनवास गईं, राम से बदला लेने का निमित्त बन रावण द्वारा हर ली गईं. मात्र एक प्रजा के कहने पर राम ने उन्हें गर्भवती अवस्था में वन में छोड़ दिया. बाद में अपने पुत्रों का अपना होने का प्रमाण भी मांगा. ऐसे में राम से अच्छा तो रावण था जिसने सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तक नहीं.
एक खास वर्ग के लोग राम को मर्यादा पुरुषोतम कहते हैं तो क्या उस वर्ग के सभी पुरुषों को अपनी स्त्रियों के साथ राम के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए. लक्ष्मण जिन्होंने भातृ प्रेम की मिसाल स्थापित की, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया. भाई का फर्ज निभाने में वह पति का फर्ज भूल गए. महाभारत की नायिका द्रौपदी के साथ जो हुआ वो सर्वविदित है. क्या वह कोई वस्तु थीं, जिसे कुंति ने कहा कि सभी भाईयों में बांट लो. क्या पत्नी भी कोई बांटने की चीज है? इस तरह के कई उदाहरण हिन्दू धर्म ग्रंथों में भरे मिलेंगे, जहां आदर्श स्थापित करने के नाम पर स्त्रियों के साथ पक्षपात हुए. मगर इन सबके बावजूद इन स्त्रियों के जीवन चरित्र को हम गहराई से अध्ययन करें तो पाएंगे कि चाहे इनके साथ कितने भी पक्षपात हुए हों, इनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था. इन्होंने तभी तक सहा जब तक इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी. जब इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात हुई, इन्होंने बगावत की. उन्होंने एक पुरुष प्रधान समाज में अपनी गरिमा, अपनी पहचान को बनाए रखा.
द्रौपदी का चरित्र हमेशा विद्रोहीणी का रहा और ये सर्वविदित है कि महाभारत में युद्ध की जड़ में द्रौपदी ही थी. इसी तरह जब राम ने सीता के चरित्र पर ऊंगली उठाते हुए उनके पुत्रों का उनके होने का सबूत मांगा तो बजाए सबूत देने के सीता ने धरती में समा जाना बेहतर समझा. यह उनके चरित्र की दृढ़ता ही थी कि उन्होंने राम को मांफी भी मांगने का अवसर नहीं दिया. ये सारे पात्र काल्पनिक हैं या यथार्थ यह एक अलग तर्क है मगर जिन स्त्रियों का उल्लेख किया गया उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री चाहे जिस काल में भी हो उसके लिए अपने आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए.
प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक एक उपमा जो स्त्रियों के लिए हमेशा दी जाती है, वह है कि सीता-सावित्री की तरह बनो. इस उपमा में सीता या सावित्री के व्यक्तित्व की ऊंचाईयों और गहराईयों को समझने की बात नहीं होती. यहां तो यह इसलिए कहा जाता है कि उनकी नजर में सीता और सावित्री अपने कुल के आदर्शों को ढोने वाली और अपने पति का अनुसरण करने वाली स्त्रियां थीं. हिन्दू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि शुरू से ही स्त्रियों के साथ छल होता आया है.
जब भी कभी कोई निर्णायक मोड़ आया तो सजा स्त्रियों को ही मिली. जिस प्रचलित कहानी के पात्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा बताया जाता है; उस भारत की माता यानी शकुंतला से राजा दुष्यंत ने प्रेम किया और गंधर्व विवाह भी किया. लेकिन अपने राज्य जाकर उन्हें भूल गए. जब शकुंतला उनके पास अपना हक मांगने पहुंची तो वह एक अंगूठी, जिसे दुष्यंत ने शकुंतला को निशानी के तौर पर दी थी के ना होने पर उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया. यह कैसा प्रेम था कि सिर्फ एक अंगूठी के ना होने पर राजा दुष्यंत ने अपनी प्रेमिका/पत्नी को पहचाना तक नहीं.
इसी प्रकार हिन्दू धर्मग्रंथों में प्रचलित कहानी के मुताबिक इंद्र ने जब छल से अहिल्या के साथ संबंध स्थापित किया तो अहिल्या के ऋषि पति ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया,. जबकि इंद्र को मिली सजा कुछ ही दिनों में माफ हो गई. क्या ये पुरूष-स्त्री के बीच का पक्षपात नहीं था? अहिल्या के साथ छल इंद्र ने किया था लेकिन सजा सिर्फ अहिल्या को क्यों? क्योंकि वह एक स्त्री थी? सीता जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहीं, उनके साथ वनवास गईं, राम से बदला लेने का निमित्त बन रावण द्वारा हर ली गईं. मात्र एक प्रजा के कहने पर राम ने उन्हें गर्भवती अवस्था में वन में छोड़ दिया. बाद में अपने पुत्रों का अपना होने का प्रमाण भी मांगा. ऐसे में राम से अच्छा तो रावण था जिसने सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तक नहीं.
एक खास वर्ग के लोग राम को मर्यादा पुरुषोतम कहते हैं तो क्या उस वर्ग के सभी पुरुषों को अपनी स्त्रियों के साथ राम के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए. लक्ष्मण जिन्होंने भातृ प्रेम की मिसाल स्थापित की, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया. भाई का फर्ज निभाने में वह पति का फर्ज भूल गए. महाभारत की नायिका द्रौपदी के साथ जो हुआ वो सर्वविदित है. क्या वह कोई वस्तु थीं, जिसे कुंति ने कहा कि सभी भाईयों में बांट लो. क्या पत्नी भी कोई बांटने की चीज है? इस तरह के कई उदाहरण हिन्दू धर्म ग्रंथों में भरे मिलेंगे, जहां आदर्श स्थापित करने के नाम पर स्त्रियों के साथ पक्षपात हुए. मगर इन सबके बावजूद इन स्त्रियों के जीवन चरित्र को हम गहराई से अध्ययन करें तो पाएंगे कि चाहे इनके साथ कितने भी पक्षपात हुए हों, इनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था. इन्होंने तभी तक सहा जब तक इनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी. जब इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात हुई, इन्होंने बगावत की. उन्होंने एक पुरुष प्रधान समाज में अपनी गरिमा, अपनी पहचान को बनाए रखा.
द्रौपदी का चरित्र हमेशा विद्रोहीणी का रहा और ये सर्वविदित है कि महाभारत में युद्ध की जड़ में द्रौपदी ही थी. इसी तरह जब राम ने सीता के चरित्र पर ऊंगली उठाते हुए उनके पुत्रों का उनके होने का सबूत मांगा तो बजाए सबूत देने के सीता ने धरती में समा जाना बेहतर समझा. यह उनके चरित्र की दृढ़ता ही थी कि उन्होंने राम को मांफी भी मांगने का अवसर नहीं दिया. ये सारे पात्र काल्पनिक हैं या यथार्थ यह एक अलग तर्क है मगर जिन स्त्रियों का उल्लेख किया गया उन्होंने यह साबित किया कि स्त्री चाहे जिस काल में भी हो उसके लिए अपने आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए. अजाक्स की रैली से प्रदेश में कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा है- जे.एन. कंसोटिया
 12 जून के बाद मध्य प्रदेश में हचलच बढ़ गई है. कारण मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी संघ यानि ‘अजाक्स’ की भोपाल में हुई वह रैली है, जिसमें प्रदेश भर से पहुंचे लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी. इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ को देखकर सरकार इतने दबाव में आ गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद यह घोषणा करनी पड़ी कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता. यह सफल कार्यक्रम अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष जे.एन. कंसोटिया के नेतृत्व में हुआ. 1993 में गठित हुए अजाक्स के श्री कंसोटिया 2005 से अध्यक्ष हैं. इस कर्मचारी आंदोलन को लेकर ‘दलित दस्तक’ के संपादक अशोक दास ने भोपाल में जे.एन. कंसोटिया से बात की.
12 जून की रैली के बाद क्या फर्क पड़ा है?
– देखिए, उस रैली के बाद दो बदलाव आया है. अच्छी बात यह है कि उस रैली में सरकार ने जो घोषणा की थी, उसके अनुसार कार्यवाही कर रही है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो अजाक्स द्वारा उठाए गए मुद्दों के पक्ष में काम करेगी. कार्यक्रम में एससी/एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों की एकता सामने आई है, जिससे उनके बीच उत्साह बढ़ा है. उनकी हिम्मत बढ़ी है कि वह बड़ा काम कर सकते हैं. जो एक निगेटिव बात हुई है वह यह है कि हमारे ही बीच के दो-तीन लोग गुटबंदी करने लगे हैं. उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है, जिसमें दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है. हालांकि उनके साथ समाज के लोग नहीं गए हैं.
अजाक्स की मांगे क्या है?
– रिजर्वेशन इन प्रोमोशन कंटिन्यू होना चाहिए. बैकलाग भरा जाए. छात्रों को स्कॉलरशिप टाइम से मिले. विद्यार्थियों के हॉस्टल का मुद्दा देखा जाए. सबको हॉस्टल की सुविधा मिले. इसके साथ ही सेल्फ इम्प्लाइमेंट के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए. इसके लिए समय पर फंडिंग हो. हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय भी हो.
अजाक्स की गतिविधियों की बात करें तो यह संगठन किन मुद्दों को देखता है?
– हम अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मुद्दों को देखते हैं. सरकार के नियम-कानून और संवैधानिक दायरे में रहते हुए यह संगठन काम करता है. चूंकि हमारा संगठन सामाजिक है, इसलिए जब हम चर्चा करते हैं तो कर्मचारियों की सेवाओं के साथ-साथ समाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं कि समाज में किस तरह जागरूकता लाई जाए. समाज के लोगों को उनके शिक्षा के अधिकार, समानता के अधिकार और उनको प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करते हैं. हम ‘पे बैक टू सोसाइटी’ के मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं कि जिस समाज ने हमको सबकुछ दिया है; उसके भी थोड़ा काम आ सकें. हम संगठन के माध्यम से समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं. उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम उनको मदद करते हैं.
आप किन परिस्थितियों से निकलते हुए आईएएस के पद तक पहुंचे. अपने बारे में बताइए.
– मैं राजस्थान का रहने वाला हूं. नागौर जिले के कुचामन सिटी का. निश्चित तौर पर मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां अभाव था. मैं फर्स्ट जेनरेशन का बंदा हूं. मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूं जिसने छठी कक्षा पास की. मेरे से पहले मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा-लिखा नहीं था. पिताजी के पास कोई संसाधन नहीं था. वो शू-मेकिंग का अपना परंपरागत काम करते थे. मेरे साथ यह अच्छी बात थी कि मुझे शुरू से ही पढ़ना अच्छा लगता था. मैंने मेहनत की तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला.
मेरा गांव टाउन है, तो वहीं से मैंने हाई स्कूल पास किया. फिर जयपुर के महाराजा कॉलेज पढ़ने गया. मैं बॉयलोजी का छात्र था क्योंकि मेरे घरवाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे. लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मेरे दूसरे भाई-बहन नहीं पढ़ पाते. क्योंकि डॉक्टरी का खर्चा ज्यादा होता है. मैंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दिया और सिंपल ग्रेजुएशन करने लगा ताकि मेरे दूसरे भाई-बहन भी पढ़ सकें और मैं अपने पिताजी की मदद कर सकूं. इस तरह मैं शासकीय सेवा में आया. बैंक में नौकरी करते हुए ही मैंने कंप्टीशन परीक्षा पास की और शासकीय सेवाओं में आया. मैं 1989 बैच में सीधे आईएएस के लिए चुना गया.
आप किन-किन पदों पर कहां-कहां रहें?
– मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर हुई. 92 के सिंहस्थ में वहीं एसडीएम था. रायगढ़, बिलासपुर (अभी छत्तीसगढ़) में असिस्टेंट कलेक्टर रहा. इधर रहते हुए ही मुझे आदिवासी इलाकों में काम करने का मौका मिला. खासकर बिरहोर जनजाति के लिए काम किया. मैं वहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर था. छतरपुर में दो साल कलेक्टर रहा, राजगढ़ में चार साल कलेक्टर रहा. कई और जगहों पर रहने के बाद भोपाल में कई विभागों में सेक्रेट्री रहा. अभी मैं मुख्य सचिव (महिला एवं बाल विकास) हूं.
सामाजिक सरोकार से आप कैसे जुड़े?
– मैंने बचपन से ही अनुसूचित जाति/ जनजाति की दिक्कतों को देखा है. जब मैं इस नौकरी में आया तो मुझे लगा कि मैं निचले पायदान पर खड़े इस समाज के लिए कुछ कर सकता हूं. योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमानुसार उनको प्राथमिकता दे सकता हूं. संवैधानिक दायरे और सरकारी सीमा में रहते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए. मध्य प्रदेश में आकर देखा कि यहां के आदिवासी भाईयों और अनुसूचित जाति के भाईयों को इसकी जरूरत भी है. उनके हित के लिए काम करने से उनको व्यवस्था में विश्वास भी होता. मेरा शुरू से यह सोचना रहा है कि जो शासन है और उसकी प्रजातंत्र की जो अवधारणा है वह हमेशा से एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है. और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को जनता के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए. और जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जाति/ जनजाति और गरीब चाहे वो किसी भी वर्ग का हो उन लोगों को है. इस तरह मैंने समाजिक दायित्वों को भी निभाना शुरू किया.
किससे प्रभावित रहें?
– देखिए, बचपन से तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था लेकिन जब बाबासाहेब को पढ़ा और जाना तो लगा कि जब उन्होंने इतने संघर्ष और मुश्किल के बावजूद देश के गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए इतना काम किया तो हमें भी सरकारी दायरे में रहते हुए यह करना चाहिए. ताकि हम देश एवं समाज के विकास की गति बढ़ा सके.
वंचित तबके से आने वाले अधिकारियों की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
– देखिए, मेरा मानना है कि जब सामान्य वर्ग का कोई अधिकारी होता है तो वंचित समाज को उससे उतनी अपेक्षा नहीं होती. लेकिन जब वंचित तबके का ही कोई व्यक्ति अधिकारी बनकर आता है तो उसे उसका समाज उम्मीद भरी नजरों से देखता है. उसे उम्मीद होती है कि उसके ही समाज से आना वाला व्यक्ति निश्चित ही संवेदनशील होगा. उसे इस तबके की दिक्कतें पता होंगी, इसलिए वो उम्मीद करता है जो जायज भी है.
क्या है अजाक्स
मध्य प्रदेश अनसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स एक सामाजिक संगठन है. यह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का संघ है और शासन से मान्यता प्राप्त है. प्रदेश के पूरे 51 जिलों में इसकी कार्यकारिणी है. संगठन 1993 में शुरू हुआ और 1994 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ. वरिष्ठ आई.ए.एस (रिटा.) अमर सिंह इसके अध्यक्ष रह चुके हैं. जे.एन. कंसोटिया सन् 2005 से इसके अध्यक्ष हैं.
12 जून के बाद मध्य प्रदेश में हचलच बढ़ गई है. कारण मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी एवं अधिकारी संघ यानि ‘अजाक्स’ की भोपाल में हुई वह रैली है, जिसमें प्रदेश भर से पहुंचे लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक साथ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी. इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ को देखकर सरकार इतने दबाव में आ गई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद यह घोषणा करनी पड़ी कि आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता. यह सफल कार्यक्रम अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष जे.एन. कंसोटिया के नेतृत्व में हुआ. 1993 में गठित हुए अजाक्स के श्री कंसोटिया 2005 से अध्यक्ष हैं. इस कर्मचारी आंदोलन को लेकर ‘दलित दस्तक’ के संपादक अशोक दास ने भोपाल में जे.एन. कंसोटिया से बात की.
12 जून की रैली के बाद क्या फर्क पड़ा है?
– देखिए, उस रैली के बाद दो बदलाव आया है. अच्छी बात यह है कि उस रैली में सरकार ने जो घोषणा की थी, उसके अनुसार कार्यवाही कर रही है. सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो अजाक्स द्वारा उठाए गए मुद्दों के पक्ष में काम करेगी. कार्यक्रम में एससी/एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों की एकता सामने आई है, जिससे उनके बीच उत्साह बढ़ा है. उनकी हिम्मत बढ़ी है कि वह बड़ा काम कर सकते हैं. जो एक निगेटिव बात हुई है वह यह है कि हमारे ही बीच के दो-तीन लोग गुटबंदी करने लगे हैं. उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है, जिसमें दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है. हालांकि उनके साथ समाज के लोग नहीं गए हैं.
अजाक्स की मांगे क्या है?
– रिजर्वेशन इन प्रोमोशन कंटिन्यू होना चाहिए. बैकलाग भरा जाए. छात्रों को स्कॉलरशिप टाइम से मिले. विद्यार्थियों के हॉस्टल का मुद्दा देखा जाए. सबको हॉस्टल की सुविधा मिले. इसके साथ ही सेल्फ इम्प्लाइमेंट के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाए. इसके लिए समय पर फंडिंग हो. हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय भी हो.
अजाक्स की गतिविधियों की बात करें तो यह संगठन किन मुद्दों को देखता है?
– हम अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मुद्दों को देखते हैं. सरकार के नियम-कानून और संवैधानिक दायरे में रहते हुए यह संगठन काम करता है. चूंकि हमारा संगठन सामाजिक है, इसलिए जब हम चर्चा करते हैं तो कर्मचारियों की सेवाओं के साथ-साथ समाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं कि समाज में किस तरह जागरूकता लाई जाए. समाज के लोगों को उनके शिक्षा के अधिकार, समानता के अधिकार और उनको प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करते हैं. हम ‘पे बैक टू सोसाइटी’ के मुद्दे पर भी चर्चा करते हैं कि जिस समाज ने हमको सबकुछ दिया है; उसके भी थोड़ा काम आ सकें. हम संगठन के माध्यम से समाज के लोगों को प्रेरित करते हैं. उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम उनको मदद करते हैं.
आप किन परिस्थितियों से निकलते हुए आईएएस के पद तक पहुंचे. अपने बारे में बताइए.
– मैं राजस्थान का रहने वाला हूं. नागौर जिले के कुचामन सिटी का. निश्चित तौर पर मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां अभाव था. मैं फर्स्ट जेनरेशन का बंदा हूं. मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूं जिसने छठी कक्षा पास की. मेरे से पहले मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा-लिखा नहीं था. पिताजी के पास कोई संसाधन नहीं था. वो शू-मेकिंग का अपना परंपरागत काम करते थे. मेरे साथ यह अच्छी बात थी कि मुझे शुरू से ही पढ़ना अच्छा लगता था. मैंने मेहनत की तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला.
मेरा गांव टाउन है, तो वहीं से मैंने हाई स्कूल पास किया. फिर जयपुर के महाराजा कॉलेज पढ़ने गया. मैं बॉयलोजी का छात्र था क्योंकि मेरे घरवाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे. लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मेरे दूसरे भाई-बहन नहीं पढ़ पाते. क्योंकि डॉक्टरी का खर्चा ज्यादा होता है. मैंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दिया और सिंपल ग्रेजुएशन करने लगा ताकि मेरे दूसरे भाई-बहन भी पढ़ सकें और मैं अपने पिताजी की मदद कर सकूं. इस तरह मैं शासकीय सेवा में आया. बैंक में नौकरी करते हुए ही मैंने कंप्टीशन परीक्षा पास की और शासकीय सेवाओं में आया. मैं 1989 बैच में सीधे आईएएस के लिए चुना गया.
आप किन-किन पदों पर कहां-कहां रहें?
– मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर हुई. 92 के सिंहस्थ में वहीं एसडीएम था. रायगढ़, बिलासपुर (अभी छत्तीसगढ़) में असिस्टेंट कलेक्टर रहा. इधर रहते हुए ही मुझे आदिवासी इलाकों में काम करने का मौका मिला. खासकर बिरहोर जनजाति के लिए काम किया. मैं वहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर था. छतरपुर में दो साल कलेक्टर रहा, राजगढ़ में चार साल कलेक्टर रहा. कई और जगहों पर रहने के बाद भोपाल में कई विभागों में सेक्रेट्री रहा. अभी मैं मुख्य सचिव (महिला एवं बाल विकास) हूं.
सामाजिक सरोकार से आप कैसे जुड़े?
– मैंने बचपन से ही अनुसूचित जाति/ जनजाति की दिक्कतों को देखा है. जब मैं इस नौकरी में आया तो मुझे लगा कि मैं निचले पायदान पर खड़े इस समाज के लिए कुछ कर सकता हूं. योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमानुसार उनको प्राथमिकता दे सकता हूं. संवैधानिक दायरे और सरकारी सीमा में रहते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए. मध्य प्रदेश में आकर देखा कि यहां के आदिवासी भाईयों और अनुसूचित जाति के भाईयों को इसकी जरूरत भी है. उनके हित के लिए काम करने से उनको व्यवस्था में विश्वास भी होता. मेरा शुरू से यह सोचना रहा है कि जो शासन है और उसकी प्रजातंत्र की जो अवधारणा है वह हमेशा से एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है. और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को जनता के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए. और जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अनुसूचित जाति/ जनजाति और गरीब चाहे वो किसी भी वर्ग का हो उन लोगों को है. इस तरह मैंने समाजिक दायित्वों को भी निभाना शुरू किया.
किससे प्रभावित रहें?
– देखिए, बचपन से तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था लेकिन जब बाबासाहेब को पढ़ा और जाना तो लगा कि जब उन्होंने इतने संघर्ष और मुश्किल के बावजूद देश के गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए इतना काम किया तो हमें भी सरकारी दायरे में रहते हुए यह करना चाहिए. ताकि हम देश एवं समाज के विकास की गति बढ़ा सके.
वंचित तबके से आने वाले अधिकारियों की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
– देखिए, मेरा मानना है कि जब सामान्य वर्ग का कोई अधिकारी होता है तो वंचित समाज को उससे उतनी अपेक्षा नहीं होती. लेकिन जब वंचित तबके का ही कोई व्यक्ति अधिकारी बनकर आता है तो उसे उसका समाज उम्मीद भरी नजरों से देखता है. उसे उम्मीद होती है कि उसके ही समाज से आना वाला व्यक्ति निश्चित ही संवेदनशील होगा. उसे इस तबके की दिक्कतें पता होंगी, इसलिए वो उम्मीद करता है जो जायज भी है.
क्या है अजाक्स
मध्य प्रदेश अनसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ यानी अजाक्स एक सामाजिक संगठन है. यह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का संघ है और शासन से मान्यता प्राप्त है. प्रदेश के पूरे 51 जिलों में इसकी कार्यकारिणी है. संगठन 1993 में शुरू हुआ और 1994 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ. वरिष्ठ आई.ए.एस (रिटा.) अमर सिंह इसके अध्यक्ष रह चुके हैं. जे.एन. कंसोटिया सन् 2005 से इसके अध्यक्ष हैं. मैं बाबासाहेब की बहुत बड़ी फॉलोअर हूं- टीना डाबी
 टीना डाबी सिर्फ 22 साल की आर्ट्स ग्रेजुएट हैं और उन्होंने यूपीएससी 2015 में टॉप किया है. टीना दलित समुदाय से आती हैं. टीना दो बहन हैं और माता पिता दोनों इंजीनियर हैं. टीना ने पहली बार में ही यूपीएससी में टॉप किया है. टीना की इस सफलता को बहुजन समाज के लिए बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अबतक दलित समुदाय से किसी महिला ने यूपीएससी में टॉप नहीं किया था. टीना के जो शुरुआती इंटरव्यू आएं उसको लेकर वह विवादों में भी रहीं. कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की टीना ने बाबासाहेब का नाम नहीं लिया. तो फेसबुक और ट्विटर पर उनके फेक प्रोफाइल के जरिए आने वाले आरक्षण विरोधी संदेश और पीएम मोदी को आदर्श मानने की बात से भी वो विवादों में रही. हालांकि दलित दस्तक को दिए इंटरव्यू में टीना ने इन बातों को साफ कर दिया है. टीना खुद को बाबा साहेब अंबेडकर की बहुत बड़ी फॉलोअर बताती हैं. वहीं वह महिला उत्थान के लिए काम करने की बात कहती हैं. टीना डाबी से बात की शंभु कुमार सिंह ने-
टीना डाबी सिर्फ 22 साल की आर्ट्स ग्रेजुएट हैं और उन्होंने यूपीएससी 2015 में टॉप किया है. टीना दलित समुदाय से आती हैं. टीना दो बहन हैं और माता पिता दोनों इंजीनियर हैं. टीना ने पहली बार में ही यूपीएससी में टॉप किया है. टीना की इस सफलता को बहुजन समाज के लिए बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अबतक दलित समुदाय से किसी महिला ने यूपीएससी में टॉप नहीं किया था. टीना के जो शुरुआती इंटरव्यू आएं उसको लेकर वह विवादों में भी रहीं. कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की टीना ने बाबासाहेब का नाम नहीं लिया. तो फेसबुक और ट्विटर पर उनके फेक प्रोफाइल के जरिए आने वाले आरक्षण विरोधी संदेश और पीएम मोदी को आदर्श मानने की बात से भी वो विवादों में रही. हालांकि दलित दस्तक को दिए इंटरव्यू में टीना ने इन बातों को साफ कर दिया है. टीना खुद को बाबा साहेब अंबेडकर की बहुत बड़ी फॉलोअर बताती हैं. वहीं वह महिला उत्थान के लिए काम करने की बात कहती हैं. टीना डाबी से बात की शंभु कुमार सिंह ने-
टीना दलित दस्तक की तरफ से बधाई
– थैंक्स
22 साल की उम्र में पहला अटैंप्ट और सीधा टॉप, भरोसा था?
– रिजल्ट जानने के बाद बहुत खुशी हुई. परीक्षा देने के बाद इतनी उम्मीद थी कि चयन तो हो जाएगा. लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि टॉप करूंगी. टॉप करने के बाद से लग रहा है कि कोई सपना जी रही हूं.
आपकी मम्मी ने बताया कि आपको पांचवीं क्लास से ही वर्ल्ड ग्लोब की पूरी जानकारी थी.
– मम्मी पढ़ाती थी और मैं इंटरेस्टेड रहती थी कि जितना ज्यादा हो सके देश और दुनिया के बारे में सीख सकूं. हमेशा कोशिश रहती थी कि जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई कर सकूं.
आपके घर में इंजीनियरिंग बैक ग्राउंड है लेकिन आपने आर्ट्स को क्यों चुना ?
– घर में इंजनियरिंग का माहौल था. लेकिन मुझे इंजीनियरिंग समझ नहीं आई. मैंने 10+2 में साइंस लिया था, लेकिन दो महीने बाद ही आर्ट्स में चली गई. शुरू से ही तय कर लिया था कि जब सिविल सर्विस में ही जाना है तो फिर सोशल साइंस की ही पढ़ाई की जाए. यूपीएससी में आर्ट्स वाले ज्यादा सफल रहे हैं. फिर तय किया कि आर्ट्स ही पढ़ना है.
बहुत लोग सोचते हैं कि यूपीएससी करनेवाले लोग स्पेशल होते हैं. यह कितना सच है ?
– ऐसा कुछ नहीं है. मैं तो बिल्कुल साधारण लड़की हूं. सुपर टैलेंट की बात मैं नहीं मानती. हां, आपको मेहनत करते रहना पड़ता है. लगकर आप मेहनत करेंगे तो सफलता तय है. लगातार मेहनत करने पर सफलता मिलती ही है. बस लगे रहने पड़ता है वही मैंने किया.
टीना को आईएएस ही क्यों बनना था ?
– मेरा शुरू से ही सोशल काम में मन लगता था. मैं हमेशा से लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती थी. मैं कॉलेज में भी अपने ही क्लास की लड़कियों को इंग्लिश पढ़ने में मदद करती थी ताकि वह भी बेहतर कर सकें. सिविल सर्विस आपको बेहतर जिंदगी और अलग करने का मौका भी देता है. आईएएस की नौकरी प्रेस्टिजियस और अच्छी है.
जॉब के लिहाज से आईएएस अच्छा है. लेकिन सिविल सर्विस में आए लोग बहुत सोशल चेंज कर पाए हैं ऐसा ज्यादा नहीं दिखता है. पत्रकारिता में तो मशहूर है कि एसडीएम, डीएम और एसपी बाघ होते हैं जिनके बारे में आम लोग कहते हैं कि वो आपको खा जाएगा.
– ऐसा नहीं है लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स का बहुत योगदान है. काफी लोगों ने बेहतर काम किया है.
आईएएस को पैसा और पावर के लिए जाना जाता है. लेकिन आप कह रही हैं कि सोशल चेंज लाना है. पहली प्राथमिकता क्या होगी ?
– कई बार लगता है कि आईएएस के बारे में एक निगेटिव इमेज बन गई है. लेकिन अब जो लोग सिविल सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह बेहतर और ईमानदारी से काम करके दिखाएं और दूसरे के लिए उदाहरण बन सके. अगर आप अच्छे अधिकारी की तरह काम करेंगे तो दूसरे भी मजबूर होंगे कि वो ईमानदारी से बेहतर काम करें.
आपकी नजरों में समाज में किस तरह के भेदभाव हैं. आप सोशल साइंस की छात्रा हैं तो इन बातों को बेहतर जानती होंगी.
– अगर भेदभाव की बात करें तो जेंडर के आधार पर काफी भेदभाव है. जाति और धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है. सुधार हुआ है लेकिन और तेजी से सुधार की जरूरत है.
आपने इसलिए हरियाणा को कैडर चुना है कि वहां ज्यादा असमानता है. ज्यादा भेदभाव है.
– हरियाणा में समस्याएं हैं लेकिन तेजी से सुधार भी हुआ है. हां ये सच है कि लिंग अनुपात में हरियाणा की हालत ज्यादा खराब है. ये भी सच है कि महिलाओं का मुद्दा मेरे लिए ज्यादा जरूरी हैं ऐसे में मैं काफी तेजी से वहां काम करूंगी. कोशिश करूंगी की बेहतर हालात बने.
आपने कहा कि जाति को लेकर भेदभाव है. किस तरह का भेदभाव है?
– देश में जाति को लेकर भेदभाव एक सच है. यह एक गंभीर मुद्दा है. इस पर बात करनी भी जरूरी है. लेकिन जितने सुधार हुए हैं उसपर भी बात करनी जरूरी है. इसी से आगे किस तरह सुधार हो सकता है इसे तय किया जा सकता है. मेरी कोशिश होगी कि भेदभाव को खत्म किया जा सके. सरकारी नीतियों के तहत जितने भी सुधार के कदम उठाए जा सकते हैं उसे उठाए. जिन लोगों के पास लाभ पहुंचना है उनके पास पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द भेदभाव खत्म हो.
आप सोशल साइंस की छात्रा हैं. कोई ऐसा समाज वैज्ञानिक जो भारत का हो और जिसने आप पर असर डाला हो.
– बहुत सारे समाज वैज्ञानिक हैं जिनको पढ़ती हूं. अमर्त्य सेन ने मुझे काफी प्रभावित किया है. जिस तरह से उन्होंने गरीबी, आरक्षण और सोशल जस्टिस पर लिखा है वो मुझे ज्यादा सही लगते हैं. उनकी बातों से सहमत हूं. भारत की ग्रोथ रेट पर उन्होंने बेहतरीन लिखा है.
तैयारी के लिए कोचिंग कितनी जरूरी है ?
– कोचिंग जरूरी है लेकिन कोचिंग की बदौलत ही सफल हुआ जा सकता है ये सही नहीं है. लेकिन कोचिंग से मदद जरूर मिलती है. जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वह अखबार पढ़कर या फिर जमकर किताबें पढ़कर सफल होते हैं. बिना कोचिंग किए भी लोग सफल होते हैं. कोचिंग जरूरी है लेकिन अंतिम सत्य नहीं है.
दिल्ली के सीएम केजरीवाल और केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात हुई. क्या बात हुई ?
– दोनों नेताओं ने बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. दोनों इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता, फिर भी मिले और शुभकामनाएं दी उसके लिए दिल से दोनों का शुक्रिया.
फैमिली का सपोर्ट कितना जरूरी है? घर का माहौल कैसा होना चाहिए ?
– परिवार का साथ बहुत जरूरी है. यूपीएससी की तैयारी एक चुनौती है. हर तीसरे दिन लगेगा का नहीं होगा. लेकिन आपको घर से और परिवार से समर्थन मिलता है तो फिर आप हिम्मत से जुट जाते हैं. इसलिए परिवार का साथ और सपोर्ट बहुत जरूरी है.
टीना मोर्डन एजुकेशन की बात करें तो सावित्री बाई फुले 1848 में पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोलती हैं. उससे पहले हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था. इस बदलाव को आप किस तरह देखती हैं?
– मुझे गर्व होता है कि एक वंचित समाज जो हमारा समाज है उसी समाज की महिला ने ही महिलाओं के लिए शिक्षा की शुरुआत की और उसे आगे बढ़ाया. सबसे बड़ी बात है कि जब आप महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा कदम था.
आपको क्या लगता है, अगर महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत और पहले होती तो उनकी हालत और बेहतर होती ?
– हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है. लेकिन धीरे-धीरे बदलाव हो रहे हैं. बदलाव धीरे-धीरे ही होता है. लेकिन हम बेहतर हो रहे हैं. लड़कियां मौका मिलते ही बेहतर करने लगी हैं. बदलाव हो रहा है.
आप महिला सुधार की बात करती हैं. कुछ लोगों का सवाल है कि भारत में अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल की नींव रखी. वो बराबरी के पक्षधर थे. लेकिन आपने उनका जिक्र नहीं किया, या फिर किसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं.
– आपने बिल्कुल सही कहा. मुझसे सीधे इस तरह के सवाल ही नहीं पूछे गए. पहली बार आपने ही पूछा है. बाबा साहेब के योगदान को तो भूला ही नहीं जा सकता. उन्होंने कितनी तकलीफों के बाद भी पढ़ाई की. उनकी वजह से बदलाव आए. उन्होंने ही पहले वीकर सेक्शन और महिलाओं के अधिकार की बात की. कितनी परेशानी में होने के बाद भी पढ़ाई पूरी की. कहां-कहां नहीं पढ़े. बाबा साहेब से मैं बहुत प्रभावित हूं. उनका पूरा जीवन ही विचारों से भरा है. मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूं. उनको तो भूलाया ही नहीं जा सकता.
बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए काम किया. उसे टीना कैसे आगे बढ़ाएगीं?
– बिल्कुल. बाबा साहेब का शिक्षा और महिलाओं के अधिकार पर जोर था. मैं भी महिलाओं की शिक्षा और लिंग अनुपात को लेकर काम करना चाहूंगी. सरकार की नीतियों को ठीक से लागू करवाने पर बदलाव जरूर आएगा.
आप खुद दो बहन हैं. आपने टॉप किया है. मतलब क्या समझा जाए कि ये बदलाव देश को दिशा देनेवाली है. महिलाओं का समय आ गया है.
– (टीना हंसते हुए) आज महिलाएं तेजी से ऊपर आ रही हैं. अब समय बदल गया है. मेहनत से वो आगे आ रही हैं. मैं खुद टॉपर बनी हूं. पहले भी टॉपर हुई हैं. तो बस अब समय महिलाओं का है. मेहनत कीजिए और समाज को बदलिए. लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं.
क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आप उस कैटेगरी से आती हैं जो हाशिए पर है. या आपको कभी महसूस कराया गया कि आप उस समाज से आती हैं जो आज भी मेन स्ट्रीम से दूर हैं ?
– सीधे कभी भेदभाव तो नहीं हुआ लेकिन यह भी सच है कि आज भी लोगों का इंटरेस्ट जाति में जरूर रहता है. जब स्कूल, कॉलेज में टॉप करती थी तो लोग यह जानने की कोशिश करते थे कि मैं किस जाति की हूं, और जानने के बाद कहते थे कि अरे वाह, इस जाति के लोग भी इतने बेहतर होते हैं. हां लेकिन उन लोगों ने फिर बाद में अपनाया कि अरे तुम तो बेहतर हो.
शहरों में हालात बदले हैं. आपको क्या लगता है.
– हां, शहर में अब जात-पात खत्म हो रहे हैं. लोग एक दूसरे को अपनाने लगे हैं. लेकिन हां, जाति एक मुद्दा तो है लेकिन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.
लड़कियों के साथ जिस तरह से हिंसा बढ़ी है उसे लेकर आप क्या सोचती हैं. इसके लिए कैसे काम करेंगी.
– हां, महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी हैं. मैं जरूर इसके लिए काम करना चाहूंगी. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो इसे कम किया जा सकता है. मैं जरूर महिलाओं की सुरक्षा को पर खास ध्यान दूंगी.
यूपीएससी की तैयारी करनेवाले छात्रों को क्या सलाह देंगी ?
– मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जमकर मेहनत करें. भरोसा बनाए रखिए. मेहनत का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है. खुद पर भरोसा कीजिए. हां, लगातार मेहनत कीजिए. सफलता जरूर मिलेगी.
और तैयारी करने वालों के मम्मी पापा के लिए क्या सलाह है?
– मम्मी-पापा के लिए यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों पर भरोसा रखिए. उनके साथ बात कीजिए. क्योंकि जब हम तैयारी होते हैं तो अपने दोस्तों और तमाम लोगों से दूर होते हैं. तब एक घर वाले ही साथ रहते हैं. उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए, सफलता जरूरी मिलेगी.
हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद
मैं अस्थायी बदलाव नहीं चाहता- कांशीराम
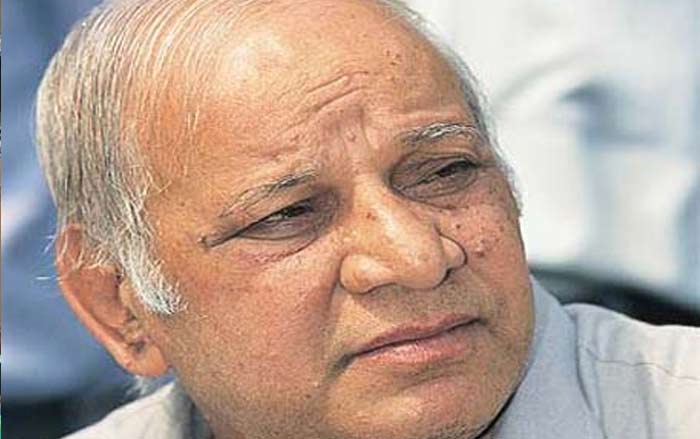 आज जब देश में राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ी हुई है, कांशीराम जी द्वारा दिए गए राष्ट्रवाद की परिभाषा गौर करने लायक है. मान्यवर कांशीराम दो राष्ट्रवाद के सिद्धान्त की बात कहते थे. एक वो जो सताए जाते हैं उनका राष्ट्रवाद और दूसरे जो सताते हैं, उनका राष्ट्रवाद. उनका मानना था कि अत्याचार करने और सताने वाले के लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा सामंतवाद है, जबकि मेरे लिए राष्ट्रवाद भारत की जनता है. 8 मार्च, 1987 को कांशीराम जी द्वारा इलस्ट्रेटिड वीकली के संवाददाता निखिल लक्ष्मण को दिए साक्षात्कार के जरिए हम मान्यवर को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन तीन दशक बाद भी वह इंटरव्यू बहुजन समाज को दिशा देने में सक्षम है.
प्रश्न- आप सभी राजनीतिक दलों के प्रति इतने विरोधी क्यों हैं, विशेषकर कम्युनिस्टों के?
उत्तर- मेरे विचार में सभी पार्टियां यथास्थिति की पोषक हैं. हमारे लिए राजनीति है बदलाव की राजनीति. मौजूदा पार्टियां यथास्थिति को बने रहने का कारण है. यही कारण है कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है. कम्युनिस्ट पार्टियां इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई हैं. वे परिवर्तन की बात करती हैं लेकिन काम यथास्थिति के लिए करती हैं. बीजेपी बेहतर है कम-से-कम यह बदलाव की बात कभी नहीं करते, इसलिए लोग धोखे में नहीं रहते. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां गरीबी दूर करने की बात करती हैं लेकिन काम गरीबी बनाये रखने का करती हैं. यदि गरीब, गरीब नहीं रहेगा तो ये लोग (यथास्थितिवादी) गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे.
प्रश्न- आपका कैडर महात्मा गांधी का इतना विरोधी क्यों है?
उत्तर- गांधी सभी बुराइयों की जड़ हैं। मैं बदलाव चाहता हूं। डॉ. अम्बेडकर बदलाव चाहते थे लेकिन गांधी यथास्थिति के रखवाले थे. वह शूद्रों को हमेशा शूद्र बनाए रखना चाहते थे. गांधी ने राष्ट्र को बांटने का काम किया लेकिन हम राष्ट्र को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, हम सभी बनावटी बंटवारों को मिटा देंगे।
प्रश्न- आप जातिवादी संगठन खड़ा करके जातिवाद को कैसे मिटा सकते हैं?
उत्तर- बीएसपी जातिवादी पार्टी नहीं है. यदि हम 6000 जातियों को जोड़ रहे हैं तो हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं?
प्रश्न- मुझे लगता है कि उच्च जातियों के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे बन्द हैं?
उत्तर- उच्च जातियां कहती हैं कि आप हमें शामिल क्यों नहीं करते. मैं कहता हूं कि आप सभी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं. यदि आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो आप यहां भी बदलाव रोक दोगे. उच्च जातियां हमारी पार्टी में शामिल हो सकती हैं लेकिन वे इसके नेता नहीं हो सकते. नेतृत्व पिछड़ी जातियों के हाथों में ही रहेगा. मुझे डर है कि जब उच्च जातियों के लोग हमारी पार्टी में आएंगे तो वे बदलाव की प्रक्रिया को रोकेंगे. जब यह डर समाप्त हो जाएगा तो वे हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं.
प्रश्न- जिन राजनीतिज्ञों से हमने दिल्ली में बात की वे कहते हैं कि यदि बीएसपी ने अपना ज्यादा लड़ाकूपन दिखाया तो वे राजनीति में खत्म कर देंगे।
उत्तर- हम उनको खत्म कर देंगे. क्योंकि जब इन्दिरा एक चमार के द्वारा खत्म की जा सकती है तब ये क्या बच सकते हैं. जब हम सशस्त्र सेनाओं में 90 फीसदी हैं, बीएसएफ में 70 फीसदी हैं, 50 फीसदी सीआरपीएफ और पुलिस में हैं तो हमारे साथ कौन अन्याय कर सकता है. एक जनरल के लिए जवानों की तुलना में कम गोलियां चाहिए. उनके पास जनरल हो सकते हैं, जवान नहीं.
प्रश्न- इसका अर्थ है आप हिंसा का प्रचार कर रहे हैं?
उत्तर- मैं शक्ति का प्रचार कर रहा हूं। हिंसा को रोकने के लिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, मेरे अलावा शिवसेना को कोई नहीं पछाड़ सकता, जब कभी मैं महाराष्ट्र आऊंगा मैं उनको खत्म कर दूंगा. शिवसेना की हिंसा खत्म हो जाएगी.
प्रश्न- आप ऐसा किस प्रकार करेंगे?
उत्तर- शिवसेना में कौन लोग हैं जो आग लगाते हैं और तोड़-फोड़ करते हैं. वे चार जातियां हैं-; अगाड़ी, भण्डारी, कोली और चमार. ये अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं. जब मैं महाराष्ट्र आऊंगा ये लोग मेरे पास आ जाएंगे.
प्रश्न- आप कैसे मानते हैं कि यूपी में बीएसपी का हश्र आरपीआई की शासक पार्टियों के साथ सौदेबाजी की ताकत की तरह खात्मा नहीं होगा?
उत्तर- आरपीआई ने कभी सौदेबाजी नहीं की. यह तो मांगने वाली पार्टी थी. यह सौदेबाजी करने के स्तर तक कभी नहीं पहुंची. मुझे याद है 1971 के आम चुनावों में 521 सीटों के लिए चुनावी समझौता हुआ, जिसमें 520 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी तथा बाकी एक पर आरपीआई. मुझे आरपीआई प्यारी है लेकिन इससे तुलना करने में मुझे घृणा है. यह एक ऐसी वेश्या है जो कौड़ियों में बिकती है. जब तक मैं जिन्दा हूं ऐसा बीएसपी के साथ कभी नहीं होगा.
हम बदलाव चाहते हैं. हम यथास्थिति वाली ताकतों से गठजोड़ नहीं चाहते. यदि सरकार हमारे सहयोग के बगैर नहीं बन सकती तो बदलाव की हमारी अपनी शर्तें होंगी. हम आधारभूत तथा ढांचागत बदलाव चाहते हैं बनावटी नहीं.
प्रश्न- आपके फंड के स्रोत के पीछे कुछ रहस्य है?
उत्तर- मेरे पास फंड विभिन्न स्रोतों से आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे. मेरा फंड ऐसे लोगों से आता है जो दौलत पैदा करते हैं. बहुजन समाज दौलत पैदा करता है. मैं उन्हीं से पैसा लेता हूं. लाखों लोग त्योहारों जैसे कुम्भ मेला इत्यादि पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, केवल अगला जन्म संवारने के लिए. कांशीराम उनको बताता है कि मैं अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन मैं वर्तमान जीवन का विशेषज्ञ हूं. मैं कहता हूं जिनको अगला जन्म संवारना है वे गंगा के किनारे ब्राह्मणों के पास जाओ, जिनको वर्तमान जीवन सुधारने में रुचि है वे मेरे पास आएं. इसलिए वे मेरी मीटिंगों के लिए दौड़ते हैं.
प्रश्न- वे कहते हैं कि आपने लखनऊ रैली पर बहुत पैसा खर्च किया है।
उत्तर- केवल बसों को किराये पर लेने के लिए ही 22 लाख रुपये खर्च किये गये. लेकिन मैं नाराज हूं. ये 22 करोड़ होने चाहिए थे. एक समय आएगा जब मेरे आह्वान पर 22 करोड़ तक लोग खर्च करेंगे. मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है. यदि खजाने से पैसा आता तो ये खाली हो जाता, मैं लगातार चलने वाले स्रोत से पैसा ले रहा हूं. मुझे सभी 542 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए केवल 1 करोड़ रुपया चाहिए. एक दिन वोटर कांशीराम को पैसा देने के लिए लाइन में खड़े होंगे, अगले दिन वे कांशीराम को वोट देने के लिए लाइन लगाएंगे.
प्रश्न- आपकी पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए?
उत्तर- आप सभी लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। कुछ लोग थक सकते हैं. कुछ को खरीदा जा सकता है. कुछ डर सकते हैं ऐसा लगातार चलता रहेगा. इससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे. मैंने एक ऐसा तरीका ईजाद (ढूंढा) किया है कि यदि किसी समय पर 10 आदमी छोड़कर जाते हैं तो हम उसी स्तर के 110 लोग तैयार कर लेंगे. जिनको हमने ‘डेडवुड’ (मृतकाठ) करके अलग किया है, उसी ‘मृत काठ’ को दूसरे जलाकर कुछ आग पैदा कर रहे हैं. वे उनको हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं.
प्रश्न- आप किस प्रकार के बदलाव की ओर देख रहे हैं?
उत्तर- मैं अस्थायी बदलाव नहीं चाहता. मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो टिकाऊ न हो. हम जो कर सकते हैं करेंगे लेकिन ये बरकरार रहना चाहिए और स्थायी बदलाव के द्वारा बरकरार रहना चाहिए.
अनुवाद- बिजेन्द्र सिंह विक्रम
आज जब देश में राष्ट्रवाद पर बहस छिड़ी हुई है, कांशीराम जी द्वारा दिए गए राष्ट्रवाद की परिभाषा गौर करने लायक है. मान्यवर कांशीराम दो राष्ट्रवाद के सिद्धान्त की बात कहते थे. एक वो जो सताए जाते हैं उनका राष्ट्रवाद और दूसरे जो सताते हैं, उनका राष्ट्रवाद. उनका मानना था कि अत्याचार करने और सताने वाले के लिए राष्ट्रवाद की परिभाषा सामंतवाद है, जबकि मेरे लिए राष्ट्रवाद भारत की जनता है. 8 मार्च, 1987 को कांशीराम जी द्वारा इलस्ट्रेटिड वीकली के संवाददाता निखिल लक्ष्मण को दिए साक्षात्कार के जरिए हम मान्यवर को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. तकरीबन तीन दशक बाद भी वह इंटरव्यू बहुजन समाज को दिशा देने में सक्षम है.
प्रश्न- आप सभी राजनीतिक दलों के प्रति इतने विरोधी क्यों हैं, विशेषकर कम्युनिस्टों के?
उत्तर- मेरे विचार में सभी पार्टियां यथास्थिति की पोषक हैं. हमारे लिए राजनीति है बदलाव की राजनीति. मौजूदा पार्टियां यथास्थिति को बने रहने का कारण है. यही कारण है कि पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ है. कम्युनिस्ट पार्टियां इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुई हैं. वे परिवर्तन की बात करती हैं लेकिन काम यथास्थिति के लिए करती हैं. बीजेपी बेहतर है कम-से-कम यह बदलाव की बात कभी नहीं करते, इसलिए लोग धोखे में नहीं रहते. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां गरीबी दूर करने की बात करती हैं लेकिन काम गरीबी बनाये रखने का करती हैं. यदि गरीब, गरीब नहीं रहेगा तो ये लोग (यथास्थितिवादी) गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे.
प्रश्न- आपका कैडर महात्मा गांधी का इतना विरोधी क्यों है?
उत्तर- गांधी सभी बुराइयों की जड़ हैं। मैं बदलाव चाहता हूं। डॉ. अम्बेडकर बदलाव चाहते थे लेकिन गांधी यथास्थिति के रखवाले थे. वह शूद्रों को हमेशा शूद्र बनाए रखना चाहते थे. गांधी ने राष्ट्र को बांटने का काम किया लेकिन हम राष्ट्र को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, हम सभी बनावटी बंटवारों को मिटा देंगे।
प्रश्न- आप जातिवादी संगठन खड़ा करके जातिवाद को कैसे मिटा सकते हैं?
उत्तर- बीएसपी जातिवादी पार्टी नहीं है. यदि हम 6000 जातियों को जोड़ रहे हैं तो हम जातिवादी कैसे हो सकते हैं?
प्रश्न- मुझे लगता है कि उच्च जातियों के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे बन्द हैं?
उत्तर- उच्च जातियां कहती हैं कि आप हमें शामिल क्यों नहीं करते. मैं कहता हूं कि आप सभी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं. यदि आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो आप यहां भी बदलाव रोक दोगे. उच्च जातियां हमारी पार्टी में शामिल हो सकती हैं लेकिन वे इसके नेता नहीं हो सकते. नेतृत्व पिछड़ी जातियों के हाथों में ही रहेगा. मुझे डर है कि जब उच्च जातियों के लोग हमारी पार्टी में आएंगे तो वे बदलाव की प्रक्रिया को रोकेंगे. जब यह डर समाप्त हो जाएगा तो वे हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं.
प्रश्न- जिन राजनीतिज्ञों से हमने दिल्ली में बात की वे कहते हैं कि यदि बीएसपी ने अपना ज्यादा लड़ाकूपन दिखाया तो वे राजनीति में खत्म कर देंगे।
उत्तर- हम उनको खत्म कर देंगे. क्योंकि जब इन्दिरा एक चमार के द्वारा खत्म की जा सकती है तब ये क्या बच सकते हैं. जब हम सशस्त्र सेनाओं में 90 फीसदी हैं, बीएसएफ में 70 फीसदी हैं, 50 फीसदी सीआरपीएफ और पुलिस में हैं तो हमारे साथ कौन अन्याय कर सकता है. एक जनरल के लिए जवानों की तुलना में कम गोलियां चाहिए. उनके पास जनरल हो सकते हैं, जवान नहीं.
प्रश्न- इसका अर्थ है आप हिंसा का प्रचार कर रहे हैं?
उत्तर- मैं शक्ति का प्रचार कर रहा हूं। हिंसा को रोकने के लिए मेरे पास शक्ति होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, मेरे अलावा शिवसेना को कोई नहीं पछाड़ सकता, जब कभी मैं महाराष्ट्र आऊंगा मैं उनको खत्म कर दूंगा. शिवसेना की हिंसा खत्म हो जाएगी.
प्रश्न- आप ऐसा किस प्रकार करेंगे?
उत्तर- शिवसेना में कौन लोग हैं जो आग लगाते हैं और तोड़-फोड़ करते हैं. वे चार जातियां हैं-; अगाड़ी, भण्डारी, कोली और चमार. ये अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं. जब मैं महाराष्ट्र आऊंगा ये लोग मेरे पास आ जाएंगे.
प्रश्न- आप कैसे मानते हैं कि यूपी में बीएसपी का हश्र आरपीआई की शासक पार्टियों के साथ सौदेबाजी की ताकत की तरह खात्मा नहीं होगा?
उत्तर- आरपीआई ने कभी सौदेबाजी नहीं की. यह तो मांगने वाली पार्टी थी. यह सौदेबाजी करने के स्तर तक कभी नहीं पहुंची. मुझे याद है 1971 के आम चुनावों में 521 सीटों के लिए चुनावी समझौता हुआ, जिसमें 520 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी तथा बाकी एक पर आरपीआई. मुझे आरपीआई प्यारी है लेकिन इससे तुलना करने में मुझे घृणा है. यह एक ऐसी वेश्या है जो कौड़ियों में बिकती है. जब तक मैं जिन्दा हूं ऐसा बीएसपी के साथ कभी नहीं होगा.
हम बदलाव चाहते हैं. हम यथास्थिति वाली ताकतों से गठजोड़ नहीं चाहते. यदि सरकार हमारे सहयोग के बगैर नहीं बन सकती तो बदलाव की हमारी अपनी शर्तें होंगी. हम आधारभूत तथा ढांचागत बदलाव चाहते हैं बनावटी नहीं.
प्रश्न- आपके फंड के स्रोत के पीछे कुछ रहस्य है?
उत्तर- मेरे पास फंड विभिन्न स्रोतों से आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे. मेरा फंड ऐसे लोगों से आता है जो दौलत पैदा करते हैं. बहुजन समाज दौलत पैदा करता है. मैं उन्हीं से पैसा लेता हूं. लाखों लोग त्योहारों जैसे कुम्भ मेला इत्यादि पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, केवल अगला जन्म संवारने के लिए. कांशीराम उनको बताता है कि मैं अगले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन मैं वर्तमान जीवन का विशेषज्ञ हूं. मैं कहता हूं जिनको अगला जन्म संवारना है वे गंगा के किनारे ब्राह्मणों के पास जाओ, जिनको वर्तमान जीवन सुधारने में रुचि है वे मेरे पास आएं. इसलिए वे मेरी मीटिंगों के लिए दौड़ते हैं.
प्रश्न- वे कहते हैं कि आपने लखनऊ रैली पर बहुत पैसा खर्च किया है।
उत्तर- केवल बसों को किराये पर लेने के लिए ही 22 लाख रुपये खर्च किये गये. लेकिन मैं नाराज हूं. ये 22 करोड़ होने चाहिए थे. एक समय आएगा जब मेरे आह्वान पर 22 करोड़ तक लोग खर्च करेंगे. मेरे लिए पैसों की कोई कमी नहीं है. यदि खजाने से पैसा आता तो ये खाली हो जाता, मैं लगातार चलने वाले स्रोत से पैसा ले रहा हूं. मुझे सभी 542 लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए केवल 1 करोड़ रुपया चाहिए. एक दिन वोटर कांशीराम को पैसा देने के लिए लाइन में खड़े होंगे, अगले दिन वे कांशीराम को वोट देने के लिए लाइन लगाएंगे.
प्रश्न- आपकी पार्टी से कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए?
उत्तर- आप सभी लोगों को एक साथ नहीं रख सकते। कुछ लोग थक सकते हैं. कुछ को खरीदा जा सकता है. कुछ डर सकते हैं ऐसा लगातार चलता रहेगा. इससे हम हतोत्साहित नहीं होंगे. मैंने एक ऐसा तरीका ईजाद (ढूंढा) किया है कि यदि किसी समय पर 10 आदमी छोड़कर जाते हैं तो हम उसी स्तर के 110 लोग तैयार कर लेंगे. जिनको हमने ‘डेडवुड’ (मृतकाठ) करके अलग किया है, उसी ‘मृत काठ’ को दूसरे जलाकर कुछ आग पैदा कर रहे हैं. वे उनको हमारे विरुद्ध प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं.
प्रश्न- आप किस प्रकार के बदलाव की ओर देख रहे हैं?
उत्तर- मैं अस्थायी बदलाव नहीं चाहता. मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो टिकाऊ न हो. हम जो कर सकते हैं करेंगे लेकिन ये बरकरार रहना चाहिए और स्थायी बदलाव के द्वारा बरकरार रहना चाहिए.
अनुवाद- बिजेन्द्र सिंह विक्रम गौरक्षा बनाम वंचित समाज और मुस्लिम
 आज के समय में भारतीय राजनीति की बात करें तो देश समाज का विकास नहीं वल्कि उसे नष्ट करने के लिए दीमक के समान अंदर ही अंदर खोखला किये जा रहा है. आने वाला समय देश व समाज के लिए घातक होता जा रहा है. सवर्ण-अवर्ण के बीच खाई बढ़ती जा रही है. वह चाहे पढ़े-लिखे हों या मजदूर किसान ही क्यों न हो इसका प्रमुख कारण यह है कि अब वंचित वर्ग जो (दलित अति दलित यह नाम दिया हुआ है सवर्णों का) पढ़-लिख गया है. अपने अधिकारों के प्रति सजग प्रहरी की तरह तैनात है. जहां अपरजाति के लोगों की मनमानी नहीं चल पा रही है वे बौखला गए हैं. अपना सनातनी धर्म व रामराज्य को स्थापित करने के लिए जहाँ कोई अवर्ण, सवर्ण के कार्य को न धारण करे यथा सम्बुक ऋषि. वे जैसा चाहतें हैं वैसा ही चलता रहे परन्तु अब ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि मैं ऊपर ही लिख चूका हूँ कि वंचित वर्ग के लोग शिक्षित और पढ़े-लिखे लोग है.
राजनीति में उनका भी अपना आस्तित्व है तभी तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश में वचितों की सरकार चार बार रह चुकी है और पांचवीं बार की तैयारी है. जो उन लोगों के आँख की किरकिरी बनीं हुई है और आये दिन उसकी छबि को खराब करने में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के हथकंडे अपनाएं जा रहे हैं. गाली-गलौज का माहौल पिछले कुछ हफ़्तों से बना हुआ है जो परिचायक है मानसिक संतुलन के खो देने का. राजनीतिक स्तर के निम्न होनें और देश के विकास का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जाना आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है. व्यक्ति राजनैतिक असंतोष का शिकार हो चुका है. वर्तमान समय के राजनीति धुरी की बात करें तो इसकी दो धुरियां है. एक गाय जो निरपराध पशु अपने भाग को पल-पल कोसती रहती है, उसे तो यह भी नही मालूम की उसका पति, बेटा बाप, भाई कौन है पल-पल में उसके नाते रिश्ते अपनों से बदलते रहते हैं पर तथाकथित एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो उसे अपनी माँ की हैशियत से देखते हैं. वे लोग बधाई के पात्र हैं जो पशु को भी सम्मान की दृष्टी से देखते हैं. पर तभी तक जब तक कि उसे राजनीतिक हाशिये पर न लिया जाय. जो राजनीति का दूध दुह रहा है वह उसे पालता नहीं और जो उसे पालने वाला है. मारे डर के नहीं पालता क्योंकि उसे डर है अपने जीवन के आस्तित्व को लेकर कब कोई बहसी बन बैठे और ऊना तथा मंदसौर कांड हो जाये. बीते दिनों की बात करें तो गुजरात में अनुसूचित जाति के युवकों को खम्भे से बांधकर बेरहमी से इसलिए मारा गया कि वे मरी गाय की खाल को निकाल रहे थे इसमें उन युवकों ने कौन सा पाप किया उसकी खाल से शुद्ध चमड़े का कौन सा जूता या बेल्ट अपने लिए बनाते. उन विचारों को तो पलास्टिक या फ़ोम के ही जूते मयस्सर होंगे रेडचिफ बूट के महंगे जूते देखना ही उनके लिए बड़ी बात है.
हमारे लालूप्रसाद यादव जी ने एक प्रश्न किया है कि जो लोग महंगा-महंगा जुतवा पहनता है ऊ काहे का बना होता है? हर हाल में यह जायज है जबाब दो. तब तो आप बाज़ार जाते हैं तो रेडचीफ़ और बूट का जूता मंगाते हैं. इतने बड़े गौमाता के भक्त हैं तो मत पहनिए चमड़े का जूता और बेल्ट, प्लास्टिक का प्रयोग करें. आप नहीं पहन सकते. इन्हें तो केवल-केवल मजदूर वर्ग ही पहनता है. वहीँ मंदसौर (मध्यप्रदेश) की घटना इससे भी कहीं ज्यादा निंदनीय है जहां मुस्लिम महिलाओं को इसलिए मारा-पिटा गया कि वे अपने निवाले के लिए मांस लेकर आ रहीं थीं. मज़े की बात यह है कि वह मांस जांच में गाय का न होकर वल्कि भैंस का पाया गया. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर क्षेत्र नोएडा में एक व्यक्ति का कत्ल भी इसी के चलते कर दिया गया था. अब इसे अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं तो और क्या कहें. जनता जहां स्वंय ही क़ानून और न्यायालय बनी हुई है. आख़िर काज़ी और पुलिस का कार्य जनता को किसने दिया. ऐसा ही चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब यहाँ के दूधमुंहे बच्चे भी क्रांति के लिए मैदान में आ डटेंगे.
दूसरी धूरी वंचित वर्ग का विशाल तबका है जिस पर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है. सभी पार्टियाँ उनकी सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फ़ेंकना चाहती हैं लेकिन जातिवाद को कोई नहीं. जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब समस्यायें जाने का नाम नहीं लेंगी. जातिवाद के नाम पर देश के कोने-कोने में आयें दिन लोग प्रतिदिन 18 व्यक्ति/मिनट प्रताड़ित होते रहते हैं. मजदूर किसान से लेकर छात्र और सरकारी मुलाज़िम तक सभी पीड़ित है. कोई मजदूरी में तो कोई शिक्षा में तो कोई चरित्रपंजिका में जाति के दंश को झेल रहा है और चुप हैं. अब तो हमारे राजनेता भी सुरक्षित नहीं वे भीं आम जनसमान्य की तरह अश्लील गालियों व् टिप्पड़ी के द्वारा लांक्षित किये जा रहें हैं उनकी अस्मत पर सवाल उठाये जा रहे हैं.उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है.
अम्बेडकरवादियों की विदेशी धरोहर( अम्बेडकर भवन) को ख़रीदा जा रहा है. अपने ही देश में जहां उनका कर्म क्षेत्र रहा है को मध्यरात्रि में उनके ईश्वर सदृश्य बाबा साहब के भवन (कर्मस्थान) को गिरा कर इतिहास को धूमिल किया जा रहा है. और यह अम्बेडकर के साथ हो रहा अन्याय वंचित वर्ग के सहन से बाहर है, वे एक पैगम्बर ही हैं जो उनकें मंडप की वेदी पर आ विराजें है जिनके सम्मुख नवदम्पति मरने जीने की कस्में उनकों साक्षी मानकर लेता है क्या वह कभी बर्दास्त करेगा. ये कैसा दलित प्रेम है. घर का चिराग बुझा कर शमशान मे आग जलाई जा रही है. यह वंचित वर्ग के लिए कोई पुण्य काम न करते हुए वल्कि अन्तरराष्ट्रीयता को भुनाया जा रहा है.
कोई उनके साथ चाय, तो कोई पांति में बैठकर खाना खा रहा है. अपने होर्डिंगों बैनर आदि पर फोटो अम्बेडकर की लगाते हैं. उनकी पहली प्रतिज्ञा की रीढ़ मारकर ही उनके सम्मुख लिखते है जय भोले जय श्रीराम आदि-आदि, लेकिन किसी ने शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लिखना उचित नहीं समझा. बाबा साहेब सदैव व्यक्तिवादी राजनीति को समाज के लिए कोड़ ही समझा परन्तु आज ख़ुद ही वे उसी के शिकार हो गएँ हैं. इससे बड़ी बिडम्बना और क्या हो सकती है. हाय तोबा हाय तोबा मची है अम्बेडकर के नाम की लूट लो….. देश की 70% पार्टियाँ अम्बेडकराईज्ड हो गयी हैं लेकिन सिद्धान्तः शून्य को इंगित कर रही हैं. इस अम्बेडकरपने से हमारे वंचित भाईयों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला मेरे अपने विचार के अनुसार अधोलिखित में से कोई एक कार्य वंचितों के लिये कर दिया जाय तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकेगाः-
1- सम्पूर्ण देश में सवर्ण-अवर्ण के बीच रोटी-बेटी का सम्बन्ध.
2- उन्हें उनका 1932 पूना-पैक्ट का अधिकार सम्प्रदायिक आवार्ड जिसे गाँधी जी के द्वारा छीन कर आरक्षण का तुच्छ टुकड़ा उनके सामने फेंक दिया गया था.
3- या सम्पूर्ण समाज को जातिविहीन कर समान पढ़ने-लिखने का अधिकार “ सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा हो मजदूर किसान”.
इस आधार पर किसी को विश्वास हो या न हो पर हमें पूरा विश्वास है कि वंचितों के जीवन में अभूत-पूर्व परिवर्तन किया जा सकेगा. वे देश समाज के लिए विकास की एक नयीं किरण लेकर आएंगे. उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा होगा जो यह कहते हैं कि दलित आरक्षण के बल पर पढ़-लिख कर आगे बढ़ते हैं.
उपरोक्त मांगों के आधार पर न यहां दोगली राजनीति होगी और न हि कहीं कोई दलित प्रताड़ित किया जायेगा और नहीं किसी की चरित्रपंजिका से खिलवाड़ होगा. उनका अपना जीवन अपने हाँथ होगा वे जैसा चाहेंगें वैसा जीवन जियेंगे. अपने देश की संसद के समय में भी प्रयाप्त बचत किया जा सकेगा जिस पर लाखो/मिनट खर्च किये जाते है केवल बहस के लिए. दलित समस्या की बहस को छोडकर देश के विकास की बात की जाएगी. वंचित वर्ग अपना विकास ख़ुद-ब-ख़ुद करेगा सबसे बड़ी बात तो यह है.कि वह किसी का मोहताज़ नहीं होगा. और फिर से वह अपने सिन्धुघाटी जैसी सर्वोच्च सभ्यता का विकास कर सकेगा अपने इतिहास को दोहरा सकेगा.
आज के समय में भारतीय राजनीति की बात करें तो देश समाज का विकास नहीं वल्कि उसे नष्ट करने के लिए दीमक के समान अंदर ही अंदर खोखला किये जा रहा है. आने वाला समय देश व समाज के लिए घातक होता जा रहा है. सवर्ण-अवर्ण के बीच खाई बढ़ती जा रही है. वह चाहे पढ़े-लिखे हों या मजदूर किसान ही क्यों न हो इसका प्रमुख कारण यह है कि अब वंचित वर्ग जो (दलित अति दलित यह नाम दिया हुआ है सवर्णों का) पढ़-लिख गया है. अपने अधिकारों के प्रति सजग प्रहरी की तरह तैनात है. जहां अपरजाति के लोगों की मनमानी नहीं चल पा रही है वे बौखला गए हैं. अपना सनातनी धर्म व रामराज्य को स्थापित करने के लिए जहाँ कोई अवर्ण, सवर्ण के कार्य को न धारण करे यथा सम्बुक ऋषि. वे जैसा चाहतें हैं वैसा ही चलता रहे परन्तु अब ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि मैं ऊपर ही लिख चूका हूँ कि वंचित वर्ग के लोग शिक्षित और पढ़े-लिखे लोग है.
राजनीति में उनका भी अपना आस्तित्व है तभी तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश में वचितों की सरकार चार बार रह चुकी है और पांचवीं बार की तैयारी है. जो उन लोगों के आँख की किरकिरी बनीं हुई है और आये दिन उसकी छबि को खराब करने में लगे हुए हैं, नाना प्रकार के हथकंडे अपनाएं जा रहे हैं. गाली-गलौज का माहौल पिछले कुछ हफ़्तों से बना हुआ है जो परिचायक है मानसिक संतुलन के खो देने का. राजनीतिक स्तर के निम्न होनें और देश के विकास का स्तर दिन प्रतिदिन कम होते जाना आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है. व्यक्ति राजनैतिक असंतोष का शिकार हो चुका है. वर्तमान समय के राजनीति धुरी की बात करें तो इसकी दो धुरियां है. एक गाय जो निरपराध पशु अपने भाग को पल-पल कोसती रहती है, उसे तो यह भी नही मालूम की उसका पति, बेटा बाप, भाई कौन है पल-पल में उसके नाते रिश्ते अपनों से बदलते रहते हैं पर तथाकथित एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो उसे अपनी माँ की हैशियत से देखते हैं. वे लोग बधाई के पात्र हैं जो पशु को भी सम्मान की दृष्टी से देखते हैं. पर तभी तक जब तक कि उसे राजनीतिक हाशिये पर न लिया जाय. जो राजनीति का दूध दुह रहा है वह उसे पालता नहीं और जो उसे पालने वाला है. मारे डर के नहीं पालता क्योंकि उसे डर है अपने जीवन के आस्तित्व को लेकर कब कोई बहसी बन बैठे और ऊना तथा मंदसौर कांड हो जाये. बीते दिनों की बात करें तो गुजरात में अनुसूचित जाति के युवकों को खम्भे से बांधकर बेरहमी से इसलिए मारा गया कि वे मरी गाय की खाल को निकाल रहे थे इसमें उन युवकों ने कौन सा पाप किया उसकी खाल से शुद्ध चमड़े का कौन सा जूता या बेल्ट अपने लिए बनाते. उन विचारों को तो पलास्टिक या फ़ोम के ही जूते मयस्सर होंगे रेडचिफ बूट के महंगे जूते देखना ही उनके लिए बड़ी बात है.
हमारे लालूप्रसाद यादव जी ने एक प्रश्न किया है कि जो लोग महंगा-महंगा जुतवा पहनता है ऊ काहे का बना होता है? हर हाल में यह जायज है जबाब दो. तब तो आप बाज़ार जाते हैं तो रेडचीफ़ और बूट का जूता मंगाते हैं. इतने बड़े गौमाता के भक्त हैं तो मत पहनिए चमड़े का जूता और बेल्ट, प्लास्टिक का प्रयोग करें. आप नहीं पहन सकते. इन्हें तो केवल-केवल मजदूर वर्ग ही पहनता है. वहीँ मंदसौर (मध्यप्रदेश) की घटना इससे भी कहीं ज्यादा निंदनीय है जहां मुस्लिम महिलाओं को इसलिए मारा-पिटा गया कि वे अपने निवाले के लिए मांस लेकर आ रहीं थीं. मज़े की बात यह है कि वह मांस जांच में गाय का न होकर वल्कि भैंस का पाया गया. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर क्षेत्र नोएडा में एक व्यक्ति का कत्ल भी इसी के चलते कर दिया गया था. अब इसे अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं तो और क्या कहें. जनता जहां स्वंय ही क़ानून और न्यायालय बनी हुई है. आख़िर काज़ी और पुलिस का कार्य जनता को किसने दिया. ऐसा ही चलता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब यहाँ के दूधमुंहे बच्चे भी क्रांति के लिए मैदान में आ डटेंगे.
दूसरी धूरी वंचित वर्ग का विशाल तबका है जिस पर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है. सभी पार्टियाँ उनकी सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फ़ेंकना चाहती हैं लेकिन जातिवाद को कोई नहीं. जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब समस्यायें जाने का नाम नहीं लेंगी. जातिवाद के नाम पर देश के कोने-कोने में आयें दिन लोग प्रतिदिन 18 व्यक्ति/मिनट प्रताड़ित होते रहते हैं. मजदूर किसान से लेकर छात्र और सरकारी मुलाज़िम तक सभी पीड़ित है. कोई मजदूरी में तो कोई शिक्षा में तो कोई चरित्रपंजिका में जाति के दंश को झेल रहा है और चुप हैं. अब तो हमारे राजनेता भी सुरक्षित नहीं वे भीं आम जनसमान्य की तरह अश्लील गालियों व् टिप्पड़ी के द्वारा लांक्षित किये जा रहें हैं उनकी अस्मत पर सवाल उठाये जा रहे हैं.उनका भी जीवन सुरक्षित नहीं है.
अम्बेडकरवादियों की विदेशी धरोहर( अम्बेडकर भवन) को ख़रीदा जा रहा है. अपने ही देश में जहां उनका कर्म क्षेत्र रहा है को मध्यरात्रि में उनके ईश्वर सदृश्य बाबा साहब के भवन (कर्मस्थान) को गिरा कर इतिहास को धूमिल किया जा रहा है. और यह अम्बेडकर के साथ हो रहा अन्याय वंचित वर्ग के सहन से बाहर है, वे एक पैगम्बर ही हैं जो उनकें मंडप की वेदी पर आ विराजें है जिनके सम्मुख नवदम्पति मरने जीने की कस्में उनकों साक्षी मानकर लेता है क्या वह कभी बर्दास्त करेगा. ये कैसा दलित प्रेम है. घर का चिराग बुझा कर शमशान मे आग जलाई जा रही है. यह वंचित वर्ग के लिए कोई पुण्य काम न करते हुए वल्कि अन्तरराष्ट्रीयता को भुनाया जा रहा है.
कोई उनके साथ चाय, तो कोई पांति में बैठकर खाना खा रहा है. अपने होर्डिंगों बैनर आदि पर फोटो अम्बेडकर की लगाते हैं. उनकी पहली प्रतिज्ञा की रीढ़ मारकर ही उनके सम्मुख लिखते है जय भोले जय श्रीराम आदि-आदि, लेकिन किसी ने शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लिखना उचित नहीं समझा. बाबा साहेब सदैव व्यक्तिवादी राजनीति को समाज के लिए कोड़ ही समझा परन्तु आज ख़ुद ही वे उसी के शिकार हो गएँ हैं. इससे बड़ी बिडम्बना और क्या हो सकती है. हाय तोबा हाय तोबा मची है अम्बेडकर के नाम की लूट लो….. देश की 70% पार्टियाँ अम्बेडकराईज्ड हो गयी हैं लेकिन सिद्धान्तः शून्य को इंगित कर रही हैं. इस अम्बेडकरपने से हमारे वंचित भाईयों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला मेरे अपने विचार के अनुसार अधोलिखित में से कोई एक कार्य वंचितों के लिये कर दिया जाय तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकेगाः-
1- सम्पूर्ण देश में सवर्ण-अवर्ण के बीच रोटी-बेटी का सम्बन्ध.
2- उन्हें उनका 1932 पूना-पैक्ट का अधिकार सम्प्रदायिक आवार्ड जिसे गाँधी जी के द्वारा छीन कर आरक्षण का तुच्छ टुकड़ा उनके सामने फेंक दिया गया था.
3- या सम्पूर्ण समाज को जातिविहीन कर समान पढ़ने-लिखने का अधिकार “ सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा हो मजदूर किसान”.
इस आधार पर किसी को विश्वास हो या न हो पर हमें पूरा विश्वास है कि वंचितों के जीवन में अभूत-पूर्व परिवर्तन किया जा सकेगा. वे देश समाज के लिए विकास की एक नयीं किरण लेकर आएंगे. उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा होगा जो यह कहते हैं कि दलित आरक्षण के बल पर पढ़-लिख कर आगे बढ़ते हैं.
उपरोक्त मांगों के आधार पर न यहां दोगली राजनीति होगी और न हि कहीं कोई दलित प्रताड़ित किया जायेगा और नहीं किसी की चरित्रपंजिका से खिलवाड़ होगा. उनका अपना जीवन अपने हाँथ होगा वे जैसा चाहेंगें वैसा जीवन जियेंगे. अपने देश की संसद के समय में भी प्रयाप्त बचत किया जा सकेगा जिस पर लाखो/मिनट खर्च किये जाते है केवल बहस के लिए. दलित समस्या की बहस को छोडकर देश के विकास की बात की जाएगी. वंचित वर्ग अपना विकास ख़ुद-ब-ख़ुद करेगा सबसे बड़ी बात तो यह है.कि वह किसी का मोहताज़ नहीं होगा. और फिर से वह अपने सिन्धुघाटी जैसी सर्वोच्च सभ्यता का विकास कर सकेगा अपने इतिहास को दोहरा सकेगा. बहुजन छात्र- युवाओं पर पुलिस दमन के निहितार्थ
 बिहार की राजधानी पटना में 3 अगस्त, 2016 को अपने हक-हकूक के लिए सड़क पर आवाज बुलंद करने उतरे दलित छात्रों पर पुलिसिया दमन की बर्बर कार्रवाई दुखद है क्योंकि दलितों का वोट सभी लेना चाहते हैं लेकिन उनको बराबरी का हक कोई भी वाकई दिल से नहीं देना चाहता.जेडीयू- बीजेपी की कमंडल समर्थक ‘विकास के साथ न्याय’ वाली सरकार में अनेकों बार शिक्षकों- छात्रों- दलितों के खिलाफ पुलिस की यही नीति थी और अब जेडीयू- आरजेडी की ‘सामाजिक न्याय’ की मंडलवादी सरकार में भी पुलिस की यही नीति है जो अफसोस की बात है. खास बात की धरना- प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन के द्वारा की गई इस प्रकार की बर्बर कार्रवाई हमेशा समाज के वंचित-शोषित और हाशिये के संघर्षरत लोगों के खिलाफ ही रही है.
बिहार की राजधानी पटना में 3 अगस्त, 2016 को अपने हक-हकूक के लिए सड़क पर आवाज बुलंद करने उतरे दलित छात्रों पर पुलिसिया दमन की बर्बर कार्रवाई दुखद है क्योंकि दलितों का वोट सभी लेना चाहते हैं लेकिन उनको बराबरी का हक कोई भी वाकई दिल से नहीं देना चाहता.जेडीयू- बीजेपी की कमंडल समर्थक ‘विकास के साथ न्याय’ वाली सरकार में अनेकों बार शिक्षकों- छात्रों- दलितों के खिलाफ पुलिस की यही नीति थी और अब जेडीयू- आरजेडी की ‘सामाजिक न्याय’ की मंडलवादी सरकार में भी पुलिस की यही नीति है जो अफसोस की बात है. खास बात की धरना- प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन के द्वारा की गई इस प्रकार की बर्बर कार्रवाई हमेशा समाज के वंचित-शोषित और हाशिये के संघर्षरत लोगों के खिलाफ ही रही है.
ऐसी घटनाओं से कई बातें साफ होती है. पहला, सरकार बदलने से पुलिस- प्रशासन का असंवेदनशील रवैया और कामकाज के तौर-तरीके नहीं बदलते है. दूसरा, सरकार में आने के बाद राजनीतिक दलों- नेताओं का रवैया असंवेदनशील हो जाता है. संख्या बल के आधार पर या फिर राजनीतिक दलों की मजबूरी में कई बार दलित-आदिवासी-ओबीसी समाज के हाथ नेतृत्व की कमान आ जाती है लेकिन सत्ता संचालन के केंद्रों व सहयोगी तंत्रों में समुचित बहुजन भागीदारी का न होना भी बदलाव की प्रतिगामी शक्तियों को आक्रमक बना देती है. इस कारण नीति बनाने, उसे लागू करने व जन-जन तक पहुँचाने में कहीं भी सरकार के नेतृत्वकर्ता की सोच काम नहीं करती है. यानि सरकार की कमान चाहे किसी बहुजन के हाथ में भले ही हो एक सवर्णवादी शासन व्यवस्था उसके समानांतर पुलिस-प्रशासन के माध्यम से चलने लगती है। इस कारण बहुजन नेता समय के अंतराल में मनोवैज्ञानिक तौर पर टूटकर- मजबूर होकर ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो उनके राजनीतिक सोच व विचारधारा से परे हो।
पुलिस की बर्बरता का यह ताजा मामला तो शिक्षा में भागीदारी के सवाल पर स्कॉलरशिप की माँग से जुड़ा था जिसपर दलित छात्र प्रदर्शन कर रहे थे. सरकार के लोगों को जबकि उसके शिक्षामंत्री अशोक चौधरी दलित ही हैं, उनकी बात सुनकर संज्ञान लेना चाहिये था क्योंकि यह प्रदर्शन आकस्मिक नहीं था बल्कि पूर्व घोषित- सूचित था. अगर एससी छात्रों के स्कॉलरशिप में गड़बड़ी, कोताही या कमी थी तो शिक्षामंत्री इसपर जन संवाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की स्थिति खुलकर स्पष्ट कर सकते थे. केन्द्र सरकार ने दलित- आदिवासी समाज के छात्रों के लिये दी जाने वाली राजीव गाँधी फेलोशिप इसलिये खत्म कर दी क्योंकि उसके पास महज 85 करोड़ रूपये सलाना का जुगाड़ नहीं था. उसी तर्ज पर बिहार में भी स्कॉलरशिप से समाज के वंचित समूह के छात्र वंचित है. अब सरकारें बहुजन छात्रों की शिक्षा के सवाल पर भी समय से राशि मुहैया नहीं करा पायें तो वाकई चिंता की बात है. दलितों को तो स्कॉलरशिप मिल भी नहीं रही है और उपर से पिटाई भी हो रही है. वहीं पिछड़ा- अति पिछड़ा को भी स्कॉलरशिप तो दूर उनकी बात- आवाज न कोई उठा रहा है, न ही ये लोग सड़क पर उतरने को तैयार है बल्कि मंडलवादी सरकार के मायाजाल में मंत्रमुग्ध होकर लालू-नीतीश के भजन गा रहे हैं. वैसे बिहार में स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों को भी हर महीने का रेगुलर वेतन नहीं मिल पाता है. बिहार में स्कूल-कॉलेज- विश्वविद्यालय स्तर के लगभग सभी शिक्षण संस्थान सवर्ण मठाधीशी के केन्द्र बने पड़े हैं जहां बहुजन छात्रों को न तो ज्ञान व बौद्धिकता का सहारा मिल रहा है न ही संगठन व संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिये कोई वैचारिक मार्गदर्शन या प्रेरणा. जाहिर है कि बहुजन अपनी सरकार में मार खाने को बाध्य हैं.
पुलिस- प्रशासन को इस तरह के विरोध प्रदर्शन में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था लेकिन कालांतर में अंग्रेज जमाने से लेकर अबतक विरोध प्रदर्शनों को पुलिस एक सेट पैटर्न अंदाज में निपटाती है. प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग, वाटर कैनन या अन्य ऐहतियातन तैयारी तो दूर लाठी मारकर सर फोड़ देना, पैर तोड़ देना और दम फुलने लगे तो गोली चला देने पर उतर जाना एक सामान्य सी बात हो गई है. जबकि खुफिया और अन्य तंत्रों के इस्तेमाल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रशासन-पुलिस चाहे तो मजबूत करने में मदद कर सकती हैं. इससे पुलिसिंग के तकनीकी ट्रेनिंग पर सवाल तो उठता ही है उनके सामाजिक- मनोवैज्ञानिक तौर पर वंचित समाज के प्रति असंवेदनशील रूख का अंदाजा लगता है. विभिन्न राज्य सरकारें और उनके मुखिया लोग भी विभिन्न छात्र-युवा, जाति-समुदाय के सामाजिक संगठनों से लगातार संवाद व सरोकार की परंपरा शुरू करें तो बेहतर हो कि सभी जाति-वर्ग- समाज के लोगों के सवाल गवर्नेंस का मुद्दा बने लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता दिखता है. यानि की मामला सरकार की बातों को जनता में कम्युनिकेट करने की अक्षमता और जनता से सीधे सरकार द्वारा फीडबैक प्राप्त न कर सत्ता परस्त प्रशासनिक बिचौलियों के माध्यम से जन-भावना को जानने से भी जुड़ा है.
भारत भर में दलितों के खिलाफ प्रताड़ना-दमन-हिंसा की घटनायें बढ़ी है. कई लोग इस तरह के दमन के मामले पर बिहार या अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी करने में लगे हैं. गुजरात में विपक्ष में कांग्रेस है वहीं बिहार में बीजेपी विपक्ष है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों आचार-व्यवहार में घोर सामंती मानसिकता वाली सामाजिक न्याय विरोधी पार्टियाँ है तो ताड़ से गिरे और खजूर पर अटके वाली बात से भी दलित समाज सतर्क दिख रहा है. गुजरात में दलितों के जनाक्रोश से भारत भर के दलित-आदिवासी समाज को सीख लेना चाहिये कि किसी पार्टी व नेता से नहीं गैर-राजनीतिक आंदोलन में भी दम है जिसके बूते आप एजेंडा सेटिंग कर सकते हैं. फिर सभी दलों के नेता आपकी ओर दौड़ेंगे जैसे कि राहुल गाँधी, केजरीवाल, मायावती भी उना गईं. अगर किसी समुदाय में वैचारिक-बौद्धिक बुनियाद पर एकजुट होकर आन्दोलन करने का जज्बा है तो किसी भी सरकार और नेताओं के आगे-पीछे घूमने की जरूरत नहीं है. इससे साफ है कि दलित-आदिवासी समाज को किसी भी राजनीतिक दल के दलदल में न फँस कर और किसी भी वर्तमान नेता (दलित-आदिवासी नेताओं सहित) का पिछलग्गू न बन कर अपने भविष्य के लिये नया नेतृत्व तैयार करना चाहिये.
भारत, खासतौर से उत्तर भारत में बहुजन समाज की दिक्कत है कि सारी गतिविधियाँ राजनीति घेरेबंदी और गिरोहबंदी की शिकार हो गयी हैं जिसके कारण जनता का हर सवाल राजनीतिक दलों के समर्थन की बाट जोहता है और लोग राजनेताओं के वरदहस्त होने के मोहताज दिखते हैं. यह भी है कि नॉन- पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट और इनिशियेटिव का सरकार, उसके सिपहसलार व मुलाजिम लोग बहुत नोटिस या तवज्जो नहीं देते हैं. इन कारणों से छात्र-युवा जो आंदोलन करते हैं वे भी संवाद-सेमिनार वगैरह रचनात्मक गतिविधियों की बजाय सड़क पर उतरने को मजबूर है और हंगामा खड़ा करने को उतावला भी दिखाई देते हैं. इन दिनों अक्सर आंदोलन को धरना-प्रदर्शन-भूख हड़ताल कर लम्बा खींचने की बजाय झड़प-विवाद-पत्थरबाजी में संलग्न होकर वन-डे वंडर की तर्ज पर अपनी माँगे मंगवाने की कोशिश में भी रहते हैं. छात्र-युवाओं के लिये चिंता की बात है कि राजनीति से वैचारिक-बौद्धिक संवाद एवं ट्रेनिंग-ग्रूमिंग का कल्चर अब खत्म हो गया है तो उनका आमतौर पर बिहेवियर पैटर्न संयम की बजाय आक्रमकता में जल्दी तब्दील होती दिखती है. नेता भी बहुत भरोसे के काबिल नहीं है क्योंकि वे दलाल- ठेकेदार व चाटुकार- चापलूस छोड़ दे तो छात्र- युवाओं से संवाद- विमर्श का रिश्ता नहीं बना पाते है और उनको महज भीड़ का हिस्सा समझते हैं. इन नेताओं में रोल-मॉडल की कमी है और धन अर्जित करना, सत्ता में किसी तरह बने रहना व परिवारवाद को बढ़ाना ही मुख्य मकसद दिखाई देता है. ऐसे में एक प्रकार का नैतिक-वैचारिक-बौद्धिक संकट भी है जिससे समाज गुजर रहा है जिसका भुक्तभोगी एससी- एसटी-ओबीसी समाज खासतौर से है.
बिहार की सरकार ने जिस तरीके से कोर्ट की आड़ में एससी-एसटी प्रोमोशन मुद्दे पर चुप्पी साधकर मुँह छुपा लिया है वह गजब है. जबकि होना तो यह चाहिये था कि एससी-एसटी प्रोमोशन के मुद्दे पर सरकार समर्थन में कोर्ट की मजबूरी के बावजूद खुलकर नैतिक तौर पर मुखर होती और साथ ही ओबीसी के प्रोमोशन में आरक्षण के सवाल पर भी आक्रमक होती. लेकिन नवम्बर, 2015 में बहुजन जातियों का बड़ा समर्थन लेने के बावजूद भी बिहार की नई सरकार चुप रहकर सवर्णों के प्रति स्ट्रैटेजिकली सॉफ्ट होने की नीति पर काम करती दिख रही है. दलित-आदिवासी समुदाय को समस्त सत्ता केंद्रों-संसाधनों और सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक क्षेत्रों के सभी स्तरों पर कमोबेश 25 फीसदी भागीदारी मुहैया कराना भारत के सभी राज्यों की सरकारों का मूल कर्तव्य होना चाहिये. इसी तरह समस्त बहुजन (एससी-एसटी- ओबीसी-पसमांदा) समुदाय के 85 फीसदी आवाम के लिये विशेष अवसर मुहैया कराना, उचित-त्वरित न्याय, सर्वांगीण विकास और समुचित भागीदारी का सवाल भी सरकारों के लिये भी बहुत जरूरी है.
निखिल आनंद एक सबल्टर्न पत्रकार और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. उनसे nikhil.anand20@gmail.com और 09939822007 पर संपर्क किया जा सकता है.
मेरे इस कुर्सी पर बैठने से अंतिम व्यक्ति का दर्द कम हो जाए तो यह बड़ी बात है- राकेश पटेल


असल में यह पहला मौका नहीं था जब राकेश पटेल ने अपने गांव घर के लोगों का नाम ऊंचा किया था. सन् 1998 में राकेश जब 10वीं में 82 प्रतिशत अंक लाकर कॉलेज टॉपर बने थे, तब भी पूरे क्षेत्र में खुशी मनी थी. हालांकि राकेश की पृष्ठभूमि वाले बहुत कम लोग अफसर बनने का सपना देख पाते हैं. परिवार के हालात बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन राकेश की जिद थी कि वह कुछ बनकर दिखाएंगे. गोरखपुर विश्वविद्यालय से एम.ए करने के बाद राकेश वहीं रहकर नौकरी की तैयारी करने लगे. 2005-06 में नेट क्वालीफाइ हो गए. उसी साल पहले ही प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विस और पीसीएस के प्रारंभिक (प्री) की परीक्षा पास कर ली और जेएनयू का इंट्रेंस भी पास कर लिया. 2006 में जुलाई में राकेश प्रो. विवेक कुमार के अंडर में समाजशास्त्र में एम.फिल करने जेएनयू आ गए. राकेश का टॉपिक था, ‘प्रवासी भारतीयों का सिनेमाई प्रस्तुतिकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन’. एक्सपर्ट ने इस अध्ययन को सोशियोलॉजी के लिए योगदान कहा. एम.फिल के बाद राकेश अपनी पी.एच डी जमा कर चुके हैं. विषय है, ‘ग्रामीण सामाजिक संरचना में निरंतरता एवं परिवर्तन’. इसके लिए उन्होंने लक्ष्मीपुर गांव को चुना है. राकेश का कहना है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, गांव के बारे में स्टडी करना चाहता था, इसलिए मैंने यह विषय चुना.

11 फऱवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला राजस्व दिवस मनाया. इस दौरान बेहतर काम करने के लिए पूरे प्रदेश से 18 डीएम, 18 एसडीएम और 18 तहसीलदार को सम्मानित किया गया. इस सूची में जौनपुर के एसडीएम सदर राकेश पटेल का भी नाम था. पटेल को जौनपुर में राजस्व से जुड़े मुकदमों के अधिकतम निस्तारण, राजस्व वसूली एवं उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. सरकार ने उन्हें प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया. महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर एकडंगा गांव के लोगों के लिए यह फख्र की बात थी. उन युवाओं में खुशी थी, जिन्हें उनके ‘राकेश भइया’ ने ‘अफसर’ बनने का सपना दिया है.
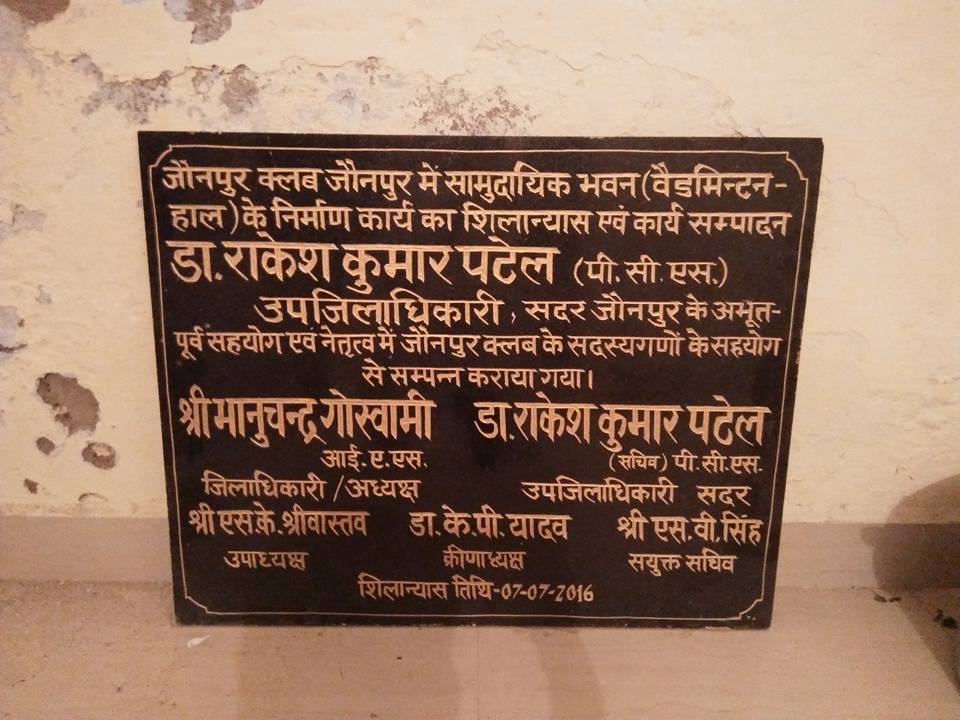 पीसीएस अधिकारी बनने के अपने सफर के बारे में राकेश कहते हैं, “हम जिस माहौल में पले पढ़े हैं, वहां अधिकारी बनने के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं. हमें बस नौकरी चाहिए होती है, जिससे हमें आर्थिक सुरक्षा मिल सके. लेकिन जेएनयू पहुंचने से काफी फर्क पड़ा. यहां आकर ज्ञानार्जन की भूख और समाज हित में उसका इस्तेमाल करने की सीख मिली. इसी का नतीजा था कि मैं ऐसे फिल्ड में जाना चाहता था जिसमें समाज को मदद कर सकूं. 2007-08 और 2010 में सिविल सर्विस का मेन्स दिया. दो बार इंटरव्यू में भी पहुंचा. पीसीएस में पहली बार में ही सेलेक्शन हो गया. 2007 की वेकेंसी थी. 2010 में इसका रिजल्ट आया. 2010 में ही संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मैंने मेरठ में प्रोबेशन पर डिप्टी कलक्टर के रूप में ज्वाइन किया. ” इसके बाद राकेश फर्रुखाबाद और लखीमपुर में रहे. फर्रुखाबाद में रहने के दौरान उन्होंने 26 गांवों में ग्राम पंचायत पुस्तकालय की शुरुआत की ताकि ग्रामीण बच्चों को अच्छी और उपयोगी किताबें मिल सके.
पीसीएस अधिकारी बनने के अपने सफर के बारे में राकेश कहते हैं, “हम जिस माहौल में पले पढ़े हैं, वहां अधिकारी बनने के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं. हमें बस नौकरी चाहिए होती है, जिससे हमें आर्थिक सुरक्षा मिल सके. लेकिन जेएनयू पहुंचने से काफी फर्क पड़ा. यहां आकर ज्ञानार्जन की भूख और समाज हित में उसका इस्तेमाल करने की सीख मिली. इसी का नतीजा था कि मैं ऐसे फिल्ड में जाना चाहता था जिसमें समाज को मदद कर सकूं. 2007-08 और 2010 में सिविल सर्विस का मेन्स दिया. दो बार इंटरव्यू में भी पहुंचा. पीसीएस में पहली बार में ही सेलेक्शन हो गया. 2007 की वेकेंसी थी. 2010 में इसका रिजल्ट आया. 2010 में ही संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मैंने मेरठ में प्रोबेशन पर डिप्टी कलक्टर के रूप में ज्वाइन किया. ” इसके बाद राकेश फर्रुखाबाद और लखीमपुर में रहे. फर्रुखाबाद में रहने के दौरान उन्होंने 26 गांवों में ग्राम पंचायत पुस्तकालय की शुरुआत की ताकि ग्रामीण बच्चों को अच्छी और उपयोगी किताबें मिल सके.
 अपने संघर्ष और समाजिक भेदभाव का जिक्र करते हुए राकेश कहते हैं, “मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं. वह बी.ए पास हैं. वह हमेशा अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते थे. आज मैं जो भी हूं उसमें मेरे माता-पिता का सहयोग और मेरे भाईयों के प्रोत्साहन की बड़ी भूमिका है.” रिजर्वेशन का लाभ कुछ खास जातियों को मिलने की बहस को पटेल अलग तरीके से देखते हैं. कहते हैं, “रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप से हजारों बच्चों की जिंदगी संवरती है. अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो आज मैं जो हूं, वह कैसे होता. ओबीसी जातियों में भी बहुत गरीबी है. अगर एक आदमी संपन्न है तो 1000 लोग जरुरतमंद हैं.” राकेश आगे जोड़ते हैं. कहते हैं कि किसी कमजोर पृष्ठभूमि से जब कोई आगे निकलता है तो पूरा गांव यहां तक की आस-पास के गांवों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके गार्जियन के बीच काफी साकारात्मक संदेश जाता है. जैसे मैं अपने गांव के और आस-पास के क्षेत्र में उदाहरण बना कि मेहनत से पढ़ाई करने और बिना पैसे दिए भी सरकारी नौकरी मिल सकती है. लोगों ने हमें काम करते देखा है. हमने खेतों में काम किया. साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहे.
अपने संघर्ष और समाजिक भेदभाव का जिक्र करते हुए राकेश कहते हैं, “मेरे पिताजी एक सामान्य किसान हैं. वह बी.ए पास हैं. वह हमेशा अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते थे. आज मैं जो भी हूं उसमें मेरे माता-पिता का सहयोग और मेरे भाईयों के प्रोत्साहन की बड़ी भूमिका है.” रिजर्वेशन का लाभ कुछ खास जातियों को मिलने की बहस को पटेल अलग तरीके से देखते हैं. कहते हैं, “रिजर्वेशन और स्कॉलरशिप से हजारों बच्चों की जिंदगी संवरती है. अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो आज मैं जो हूं, वह कैसे होता. ओबीसी जातियों में भी बहुत गरीबी है. अगर एक आदमी संपन्न है तो 1000 लोग जरुरतमंद हैं.” राकेश आगे जोड़ते हैं. कहते हैं कि किसी कमजोर पृष्ठभूमि से जब कोई आगे निकलता है तो पूरा गांव यहां तक की आस-पास के गांवों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके गार्जियन के बीच काफी साकारात्मक संदेश जाता है. जैसे मैं अपने गांव के और आस-पास के क्षेत्र में उदाहरण बना कि मेहनत से पढ़ाई करने और बिना पैसे दिए भी सरकारी नौकरी मिल सकती है. लोगों ने हमें काम करते देखा है. हमने खेतों में काम किया. साथ-साथ पढ़ाई भी करते रहे.
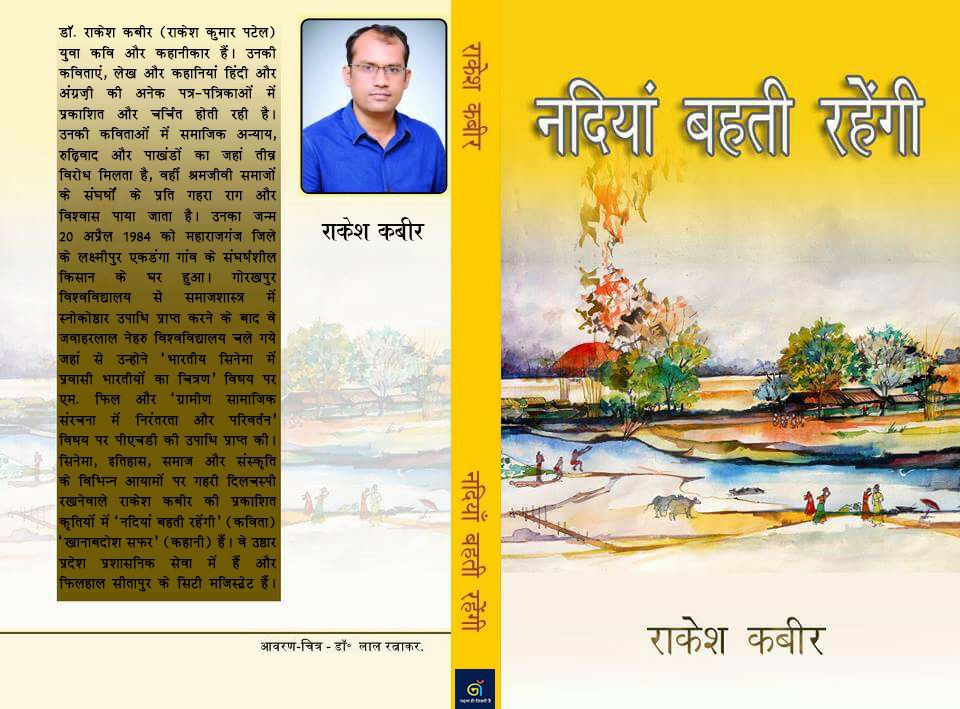
लेकिन राकेश सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है. वह वंचित तबकों से जुड़े मुद्दों पर लेखन के जरिए भी लगातार सक्रिय हैं. ‘नदियां बहती रहेंगी’ नाम से उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, जो इसमें उठाए गए मुद्दों के कारण काफी चर्चा में रहा. संघर्ष से निकलकर पहुंचे राकेश पटेल ‘पे बैक टू सोसायटी’ में विश्वास करते हैं. कहते हैं, “पढ़ाई को लेकर जो भी मदद मांगता है, मैं जितनी मदद कर सकता हूं जरूर करता हूं. मैं अपने तीन-तीन रिश्तेदारों को पढ़ाता हूं. कमजोर पृष्ठभूमि का जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी मेरे पास पहुंचता है उनकी मदद करता हूं.” राकेश कहते हैं कि मेरे आगे बढ़ने से मेरे गांव और आस-पास के गांव में लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है. उत्साहित राकेश कहते हैं, ‘मैंने भी उनकी मदद के लिए गांव में बुद्धा लाइब्रेरी खोली है.’ जौनपुर शहर के एसडीएम सदर के रूप में भी राकेश पटेल जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं. कहते हैं, ‘अगर मेरे इस कुर्सी पर बैठने से अंतिम व्यक्ति का दर्द कम हो जाए तो यह बड़ी बात है.’ इस युवा अधिकारी की यह सोच सलाम करने लायक है.
दलित अस्मिता यात्रा का दूसरा दिन, 15 अगस्त को पहुंचेगी उना
 अहमदाबाद। उना में दलित युवकों की पिटाई के बाद न्याय की मांग के लिए सैकड़ों दलितों और विभिन्न नागरिक अधिकार संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार को शहर से पैदल मार्च “दलित अस्मिता यात्रा” की शुरूआत की. गिर सोमनाथ जिले में उना शहर के वेजलपुर क्षेत्र से करीब 800 लोगों ने सुबह 380 किलोमीटर लंबी दस दिन की यात्रा की शुरूआत की. दलित अत्याचार संघर्ष समिति ने ऊना की घटना के विरोध में आंदोलन छेड़ रखा है. समिति के संयोजक जिगनेश मेवानी ने बताया कि दलितों के हित में कई मांगें रखी गई हैं. समिति की मांगों में गुजरात के भूमिहीन दलितों को पांच-पांच एकड़ जमीन, ऊना की घटना के पीड़ितों को न्याय, तय वेतन पर काम कर रहे राज्य के सफाईकर्मियों को स्थाई नियुक्ति करने आदि शामिल हैं.
जिग्नेश मेवानी ने कहा कि यह “अस्मिता यात्रा” देश भर के दलितों को पुरानी परंपराओं से आजादी की दिशा में पहला कदम है. हम अपनी यात्रा के दौरान दलितों से मृत जानवरों को उठाने के पारंपरिक काम को छोड़ने का आग्रह कर सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना है कि दलित अपने उपर किसी भी प्रकार अत्याचार नहीं सकेगा. अहमदाबाद वेजलपुर अंबेडकर चौक से शुरू हुई यात्रा धोलका, धंधूका, बोटाद, अमरेली, राजूला, सावरकुंडला होते हुए 14 अगस्त को उना पहुंचेगी. 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा.
अहमदाबाद। उना में दलित युवकों की पिटाई के बाद न्याय की मांग के लिए सैकड़ों दलितों और विभिन्न नागरिक अधिकार संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार को शहर से पैदल मार्च “दलित अस्मिता यात्रा” की शुरूआत की. गिर सोमनाथ जिले में उना शहर के वेजलपुर क्षेत्र से करीब 800 लोगों ने सुबह 380 किलोमीटर लंबी दस दिन की यात्रा की शुरूआत की. दलित अत्याचार संघर्ष समिति ने ऊना की घटना के विरोध में आंदोलन छेड़ रखा है. समिति के संयोजक जिगनेश मेवानी ने बताया कि दलितों के हित में कई मांगें रखी गई हैं. समिति की मांगों में गुजरात के भूमिहीन दलितों को पांच-पांच एकड़ जमीन, ऊना की घटना के पीड़ितों को न्याय, तय वेतन पर काम कर रहे राज्य के सफाईकर्मियों को स्थाई नियुक्ति करने आदि शामिल हैं.
जिग्नेश मेवानी ने कहा कि यह “अस्मिता यात्रा” देश भर के दलितों को पुरानी परंपराओं से आजादी की दिशा में पहला कदम है. हम अपनी यात्रा के दौरान दलितों से मृत जानवरों को उठाने के पारंपरिक काम को छोड़ने का आग्रह कर सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह संदेश देना है कि दलित अपने उपर किसी भी प्रकार अत्याचार नहीं सकेगा. अहमदाबाद वेजलपुर अंबेडकर चौक से शुरू हुई यात्रा धोलका, धंधूका, बोटाद, अमरेली, राजूला, सावरकुंडला होते हुए 14 अगस्त को उना पहुंचेगी. 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा. रियो ओलंपिक में दलित-आदिवासी भागेदारी
 ओलंपिक को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है. 2016 का ओलंपिक खेल ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हो रहा है. यह अब तक का 31वां ओलंपिक है. खेलों का यह महाकुंभ 5 अगस्त से शुरू हो गया है औऱ 21 अगस्त तक चलेगा. इसमें 206 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो इसमें 11 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. भारत से रियो ओलंपिक में 122 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो 14 खेलों में चुनौती पेश करेंगे. इसमें एथलेटिक्स में 38, हॉकी में 32, निशानेबाजी में 12, कुश्ती में 8, बैडमिंटन में 7, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और टेनिस में 4-4 खिलाड़ी अपनी चुनौती रखेंगे.
खास बात यह है कि इस ओलंपिक में दलित/आदिवासी समाज के खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिन्होंने लंबे संघर्ष और कठिन परिश्रम से ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है. दलित दस्तक के पास जो सूचना है उसके मुताबिक झारखंड से निक्की प्रधान हॉकी में और लक्ष्मी रानी मांझी और दीपीका कुमारी तीरंदाजी टीम में शामिल हैं. दीपीका जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं, जबकि निक्की और लक्ष्मी रानी मांझी ओलंपिक के लिए नया चेहरा है. भारत की ओर से रियो ओलंपिक जाने वालों में देविंदर वाल्मीकि भी शामिल हैं. देविंदर पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले देविंदर का पूरा परिवार मुंबई में रहता है. दलित दस्तक के पास ओलंपिक जाने वाले जिन दलित/ आदिवासी/ मूलनिवासी लोगों की जानकारी है, हम उसे साझा कर रहे हैं.
ओलंपिक को खेलों का महाकुंभ कहा जाता है. 2016 का ओलंपिक खेल ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हो रहा है. यह अब तक का 31वां ओलंपिक है. खेलों का यह महाकुंभ 5 अगस्त से शुरू हो गया है औऱ 21 अगस्त तक चलेगा. इसमें 206 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो इसमें 11 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. भारत से रियो ओलंपिक में 122 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जो 14 खेलों में चुनौती पेश करेंगे. इसमें एथलेटिक्स में 38, हॉकी में 32, निशानेबाजी में 12, कुश्ती में 8, बैडमिंटन में 7, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और टेनिस में 4-4 खिलाड़ी अपनी चुनौती रखेंगे.
खास बात यह है कि इस ओलंपिक में दलित/आदिवासी समाज के खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे, जिन्होंने लंबे संघर्ष और कठिन परिश्रम से ओलंपिक में अपनी जगह बनाई है. दलित दस्तक के पास जो सूचना है उसके मुताबिक झारखंड से निक्की प्रधान हॉकी में और लक्ष्मी रानी मांझी और दीपीका कुमारी तीरंदाजी टीम में शामिल हैं. दीपीका जाना-पहचाना नाम बन चुकी हैं, जबकि निक्की और लक्ष्मी रानी मांझी ओलंपिक के लिए नया चेहरा है. भारत की ओर से रियो ओलंपिक जाने वालों में देविंदर वाल्मीकि भी शामिल हैं. देविंदर पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा हैं. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले देविंदर का पूरा परिवार मुंबई में रहता है. दलित दस्तक के पास ओलंपिक जाने वाले जिन दलित/ आदिवासी/ मूलनिवासी लोगों की जानकारी है, हम उसे साझा कर रहे हैं.
रियो में झारखंड की बेटियां करेगी “चक दे इंडिया”
रियो ओलंपिक में झारखंड से तीन बेटियां जा रही हैं. इसमें निक्की प्रधान हॉकी में जबकि दीपीका कुमारी और लक्ष्मी रानी मांझी तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी. निक्की प्रधान- (हॉकी) झारखंड की राजधानी रांची से 30 किलोमीटर दूर हेसेल गांव के साधारण परिवार की असाधारण बेटी निक्की का चयन महिला ओलंपिक हॉकी टीम में हुआ है. निक्की प्रधान बचपन के दिनों में खेल के नाम से डरती थी. वहीं आज झारखंड राज्य की पहली महिला हॉकी ओलंपियन बनने जा रही है. निक्की के स्कूली जीवन के प्रारंभिक कोच और राजकीय मध्य विद्यालय पेलौल के शिक्षक दशरथ महतो बताते हैं कि प्रधान की बड़ी बहन शशि प्रधान हॉकी खेला करती थी, जबकि निक्की खेलने से बहुत डरती थी. उसे डर लगता था कि कही स्टिक से लगकर पैर न टूट जाए. लेकिन बाद में निक्की का मन हॉकी में ऐसा रमा कि वह ओलंपिक जा पहुंची है. निक्की का कहना है कि मुझसे देश के सवा सौ करोड़ लोगों की अपेक्षाएं होंगी. मैं बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी. हर खिलाड़ी का सपना होता है कि देश के लिए पदक जीते. मेरा भी एक सपना है कि मैं देश के लिए पदक हासिल करूं और देश का नाम रौशन करूं. निक्की झारखंड से ओलंपिक में पहुंचने वाली छठी हॉकी खिलाड़ी है, हालांकि यह कारनामा 24 साल बाद हो पाया है. लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो वह झारखंड से ओलंपिक पहुंचने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं. निक्की की इस सफलता से उसकी सहेली बिरसी मुंडू और शिक्षक सुजय मांझी सहित पूरा गांव खुश है. निक्की पिछले दो साल से भारतीय महिला हॉकी टीम की नियमित सदस्य है. निक्की हटिया स्थित रेलवे के डीआरएम कार्यालय में नौकरी करती है. जानकारी के मुताबिक निक्की जनजाति समाज से ताल्लुक रखती हैं. एक तथ्य यह भी है कि ओलंपिक में जाने वाली प्रधान के गांव में कोई खेल का मैदान भी नहीं है. वह स्कूली समय में सुबह शाम गांव के खेत में स्टीक लेकर अभ्यास किया करती थी. निक्की की सहेली बिरसी बताती है कि प्रधान में एक जुनून है. वह हमेशा अपने गांव और देश का नाम रोशन करने की बात किया करती थी. लक्ष्मी रानी मांझी- (तीरंदाजी) भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल जमशेदपुर की रहने वाली लक्ष्मीरानी मांझी का मानना है कि रियो ओलंपिक में बेहद कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. फिर भी वह यहां मेडल जीतना चाहती हैं. वह इससे पहले कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती. मांझी रियो ओलंपिक की तैयारी में दिन-रात जुटी रही. उसने दवाब से निपटने के लिए योग भी किया. मांझी पहली बार ओलिंपिक में शामिल होने जा रही हैं. उनका प्रदर्शन कंपीटिशन वाले दिन पर निर्भर करता है. वहां हर कोई मेडल जीतना चाहेगा. मांझी का मानना है कि ओलंपिक शुरू होने से 25 दिन पहले वहां जाने का फायदा मिलेगा. हमारा प्रदर्शन शानदार होगा. दीपिका कुमारी (तीरंदाजी) रियो ओलिंपिक में शामिल होने वाली झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी का मानना है कि साल 2012 लंदन ओलिंपिक में किया गया उनका प्रदर्शन अब बीते दिनों की बात हो चुकी है. दीपिका ने शूटिंग और स्कोरिंग में काफी सुधार किया है. दीपिका ने मानसिक दबाव से किस प्रकार निबटा जाता है इसका गुर भी सीख लिया है. दीपिका ओलंपिक से 25 दिन पहले ही रियो पहुंच चुकी हैं, जिससे की वहां के मौसम के अनुकूल वह खुद को ढाल सकें. देविंदर वाल्मीकि (हॉकी) अलीगढ़ में ब्लॉक धनीपुर के गांव अलहादपुर के देविंदर वाल्मीकि का चयन रियो ओलंपिक में खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम में हो गया है. टीम में मिड फिल्डर के तौर पर वे देश के लिए पसीना बहांएगें. देविंदर के पिता सुनील वाल्मीकि पेशे से ड्राइवर हैं. गरीब परिवार में जन्में देविंदर ने आर्थिक तंगी समेत कई समस्यओं से जूझते हुए रियो ओलंपिक तक का सफर तय किया है. देविंदर ने नौ साल की उम्र में हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने बड़े भाई युवराज से प्रेरित होकर स्टिक थामी थी. मुंबई के चर्च गेट में प्रैक्टिस करते हुए 24 साल की उम्र में ओलंपिक में स्थान पक्का कर अपना लोहा मनवाया है. देविंदर ने 2014, 2015 व 2016 में हुए हॉकी इंडिया लीग में मिड फिल्डर के तौर पर हिस्सा लिया. 2015 में बेल्जियम में हुई हॉकी वर्ल्ड लीग राउंड थ्री में दो गोल दागे. इसमें टीम इंडिया टॉप-4 में रही. 2016 में चैंपियन ट्रॉफी में एक गोल दागकर रजत पदक जीता, फिर 2016 के छठी नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में एक गोल किया.देविंदर के पिता सुनील वाल्मीकि काम की खोज में पांच दशक पहले मुंबई गए थे. वहां उन्होंने ड्राइविंग कर परिवार का पालन-पोषण किया. मां मीना ने मुंबई में ही 28 मई 1992 में देविंदर को जन्म दिया. खिलाड़ी के तीन भाई राकेश, रवि व युवराज यहां गांव अलहादपुर में ही पैदा हुए. देविंदर ने आर्थिक तंगी समेत तमाम समस्याओं से जूझते हुए रियो ओलंपिक तक का सफर तय किया है.बीबी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खत्म करेगी दलित छात्रों का आरक्षण, धरने पर बैठे छात्र
 लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्रशासन दलित छात्रों को मिला 50 प्रतिशत आरक्षण खत्म करना चाहती है, जिसका विरोध करने वाले 19 छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है. जिसके विरोध में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंटृ यूनियन (एयूडीएसयू) छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. दलित छात्रों की मांग है कि जिन 19 छात्रों के खिलाफ एफआईआर करने जा रहे है, उसे वापिस लिया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो याचिका कोर्ट दायर की है, उसे वापिस लिया जाए. दलित छात्रों को झूठे केस में फंसाने की निष्पक्ष जांच की जाए और बीएड विभाग में शिक्षक नियुक्ति पर हुई धांधली को लेकर उचित कार्रवाई की जाए.
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन यूनिवर्सिटी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिले 50 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करना चाहता है. इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय ने न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं. प्रशासन द्वारा छात्रों की मांग अनदेखी करने पर एयूडीएसयू के साथ छात्र धरने पर बैठ गए हैं.
इस मामले पर एयूडीएसयू ने अपने पेज पर 23 जुलाई को लिखा था कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर अशोका हॉस्टल के बाहर आरएसएस ने बैठक की. इस बैठक में गुजरात के आंदोलनरत दलितों को गालियां दी गई, तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की गई थी.
लखनऊ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी प्रशासन दलित छात्रों को मिला 50 प्रतिशत आरक्षण खत्म करना चाहती है, जिसका विरोध करने वाले 19 छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है. जिसके विरोध में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंटृ यूनियन (एयूडीएसयू) छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. दलित छात्रों की मांग है कि जिन 19 छात्रों के खिलाफ एफआईआर करने जा रहे है, उसे वापिस लिया जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो याचिका कोर्ट दायर की है, उसे वापिस लिया जाए. दलित छात्रों को झूठे केस में फंसाने की निष्पक्ष जांच की जाए और बीएड विभाग में शिक्षक नियुक्ति पर हुई धांधली को लेकर उचित कार्रवाई की जाए.
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन यूनिवर्सिटी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिले 50 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करना चाहता है. इस आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय ने न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं. प्रशासन द्वारा छात्रों की मांग अनदेखी करने पर एयूडीएसयू के साथ छात्र धरने पर बैठ गए हैं.
इस मामले पर एयूडीएसयू ने अपने पेज पर 23 जुलाई को लिखा था कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर अशोका हॉस्टल के बाहर आरएसएस ने बैठक की. इस बैठक में गुजरात के आंदोलनरत दलितों को गालियां दी गई, तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ भी की गई थी. 

